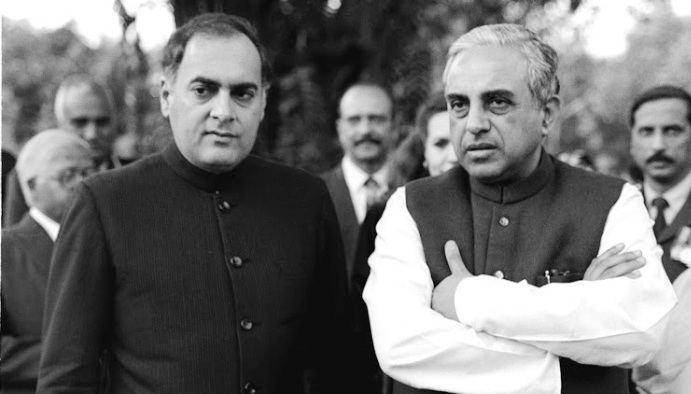Meraj Ahmad for BeyondHeadlines
लोकतान्त्रिक देश में सबसे महत्त्वपूर्ण है चुनाव के आधार पर आम लोगों की सत्ता में भागीदारी… राजनीति सदैव समाजिकता को परिभाषित करती रही है, यहाँ तक कि राजनीति ने समाज की दशा और दिशा के निर्देशन का भी काम किया है. भारतीय समाज एकांगी समाज नहीं है. लगभग हर धार्मिक समुदाय में सामाजिक स्तरीकरण है. इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे तथा चुनाव में इसके सम्बन्ध पर चर्चा की जाये.
26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया. मौलिक अधिकार के रूप में ऐसे प्रावधान रखे गए जिससे देश के सामाजिक धरातल को समतल बनाने का काम संभव हो सके. इन अधिकारों की परिधि को समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने बढ़ाया है. 1951 में संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग या SC और ST के लिए विशेष प्रावधन करने का अधिकार राज्य को दिया. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 भारत के सामाजिक इतिहास में युगांतरकारी रहा है. अब राज्य ‘समानता के अधिकार’ को लागू करने के लिए कानून बना सकता था, और ऐसे क़ानून बने भी. इसके बाद मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू हुईं, जिसने समाजिक न्याय के लिए किये गए संघर्ष को और एक कदम आगे बढाया. लेकिन क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए था कि सामाजिक न्याय के पहिये ने अपनी परिधि पूरी कर ली है? और क्या इस परिधि में सारे धार्मिक साम्प्रदायों के पिछड़े और शोषित वर्गों का समावेश हो चुका है?
पिछली सदी में नब्बे का दशक राजनीतिक दृष्टि से काफी उथल पुथल का रहा. एक तरफ मंडल-कमंडल का जोर था तो दूसरी तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए विश्व बैंक के दबाव में भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी पूँजी के लिए खोला जाना था. जनता पार्टी से जन्मी भाजापा सत्ता में आई और इसके दुष्परिणाम देखे गये.
हिन्दुत्त्व की राजनीति ने न सिर्फ गुथे हुए भारतीय समाज को कमज़ोर किया बल्कि कई वर्गों को हाशिये पर भी धकेल दिया. इस प्रकार की राजनीति ने अब तक चलने वाले विमर्श- साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता- के वाद को राजनीति के मुख्य मंच पर न सिर्फ खड़ा किया बल्कि इसकी आड़ में निरंतर हो रही ‘सेक्युलर’ राजनीतिक असफलताओं को छिपाया भी जाने लगा. धीरे-धीरे आम आदमी से जुड़े मुद्दे किनारे होते गए और पूंजीवाद को गहराई से स्थापित किया जाने लगा. जिसका असर ये हुआ कि हर धार्मिक संप्रदाय का मेहनतकश तबक़ा और पिछड़ गया. और इसकी दोहरी मार धार्मिक अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों पर पड़ी.
सवाल यह है कि हिंदुत्तव की राजनीति पर आधारित पार्टी इतनी गहरी पैठ कैसे बना पायी, इसे अब तक क्यों नहीं रोका गया? विपक्षी पार्टियों ने इसे रोकने का कितना प्रयास किया? और इसमें सबसे ज्यादा नुक्सान समाज के किस वर्ग का हुआ? आजादी के बाद साम्प्रदायिकता की राजनीति निश्चित रूप से भगवा बिग्रेड ने शुरू किया और यह यकायक नहीं हो गया. संघ की स्थापना ने आज़ाद भारत के भविष्य को जिस तरह से देखा, और मुस्लिम लीग जिस तरह एक नया मुल्क बनाने में कामयाब हुआ, इससे यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिकता को किसी एक राजनीतिक विचारधारा से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा. भगवा बिग्रेड का उफान अन्य सेक्युलर कही जाने वाली पार्टियों की असफलता का ही परिणाम रहा है, और यदि भगवा रंग धीमा पड़ा है तो इसका श्रेय आम जनता को ही दिया जा सकता है; यह सामाजिक-राजनीतिक घटना ये भी सिद्ध करती है कि आम भारतीय मूलतः साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं रखता है.
साम्प्रदायिकता की आग को हवा देने के अन्य कारण भी हैं. भगवा बिग्रेड के एक शीर्ष नेता ने ही कहा था कि रथ यात्रा सामाजिक आन्दोलन की धार को कुंद करने के लिए भी आयोजित की गयी थी. इस प्रकार की राजनीति को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया. यह भी प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक पार्टियों ने विकास के साथ-साथ साम्प्रदायिकता को रोकने का कितना प्रयास किया है, विशेषकर हिंदी क्षेत्रों में? क्या सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों ने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर भी पर भी उतना ही पॉलिटिकल कैपिटल लगाया है? क्या यह दोनों बातें अलग हैं या इनके साथ कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? इसका उत्तर सबसे बड़े हिंदी भाषी क्षेत्र- उत्तर प्रदेश के पिछले दस सालों की राजनीति में छिपा हुआ है.
अब अहम सवाल है आम आदमी से जुड़े मुद्दों का, जिससे देश के हर नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म, ज़ात, भाषा या भौगोलिक क्षेत्र का हो, को जूझना ही पड़ता है. आम आदमी से जुड़े सवालों में मुख्य हैं भ्रष्टाचार से मुक्ति और शासन प्रशासन में पारदर्शिता, सबके लिए शिक्षा और सामान अवसर, कृषि, महिलाओं का उत्थान, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि. पिछले दशक में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासों के कारण बनी परिस्थितियों ने फिर से वही साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का पुराना अलाप छेड़ने को मजबूर किया. पिछले दो सालों में सड़-गल गयी भ्रष्ट, साम्प्रदायिक और भाई-भतीजावाद पर आधारित राजनीति के खिलाफ हुए जन संघर्ष को जनता ने बहुत ही करीब से देखा.
निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में हुए आम चुनाव के परिणाम ने राजनीति की भाषा को बदल दिया. वो कहते है न कि रूल्स ऑफ़ द गेम को ही चेंज कर दिया. राजनीतिक पार्टियों को अब लगने लगा है कि आम आदमी से जुड़े मुद्दों के आधार पर भी मज़बूत जनमत संग्रह किया जा सकता है, इसलिए अब परम्परागत राजनीति को बदलना होगा. इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि इस प्रकार की राजनीति ने साम्प्रदायिकता पर भी लगाम लगाने का काम किया है.
अब इस पूरे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में मुस्लिम समाज कहां खड़ा होता है? दंगे सिर्फ नब्बे के दशक के बाद ही सच्चाई नहीं हैं. आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर 1990 तक देश में कई भयानक दंगे हुए जिनमें हैदराबाद जनसंहार (1948), गुजरात (1969), मुरादाबाद (1980), नेल्ली (1983), सिख जनसंहार (1984), हाशिमपुरा (1987) और भागलपुर (1989) उल्लेखनीय हैं. नब्बे के बाद कई और बड़े दंगे हुए जिसमे गुजरात का नरसंहार (2002) सबसे अधिक चर्चा में रहा. निरंतर होते रहे दंगे ने धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की कमर को तोड़ कर रख दिया है. बदलती अर्थव्यवस्था के कारण लघु-उद्योगों का भी काफी नुक्सान हुआ. दंगे की मार, बदलती अर्थव्यवस्था, और अशिक्षा के कारण मुस्लिम समाज का पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से हाशिये पर आ गया. सच्चर समिति के अनुसार आंकड़े साबित करते हैं कि मुस्लिम समाज में शिक्षा की दर रास्ट्रीय औसत से काफी कम है. सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्तव न के बराबर है. लेकिन इन स्थितियों को बदलने के लिए क्या राजनीतिक प्रयास किये गए? इन प्रयासों की प्रकृति क्या रही है, और वास्तव में कितना अंतर हुआ है?
प्रतिक्रिया स्वरूप राजनीतिक जवाबदेही तय करके, धार्मिक अल्पसंख्यकों का सामाजिक उत्थान कैसे किया जाये, इस पर अधिकाधिक बहस होती रही है. प्रतीकों की परम्परागत राजनीति में विशेष भाषा, परिधान और संस्कृति का दिखावी पोषण राजनीति शोषण का आधार बना. इसी के साथ ‘सेक्युलर’ बनने की होड़ में ‘माइनॉरिटी पॉलिटिक्स’ का स्वरुप तैयार किया गया. लेकिन तथ्यात्मक सामाजिक सत्य साबित करते हैं कि अब तक की जा रही राजनीति में कहीं न कहीं बड़ी भारी चूक हुई है.
ऐसी स्थिति में प्रश्न यही कि इस बदलते परिदृश्य में मुस्लिम समाज का वोट किस आधार पर बटोरा जाए ताकि सेक्युलर राजनीति के साथ साथ सामूहिक विकास संभव हो सके? शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास, सीधे तौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए की जा रही राजनीति का मुख्य हिस्सा नहीं बना. आरक्षण का फ़ायदा, जिसे देश के आज़ाद होने के बाद तीनों स्तरों पर मिलना चाहिए था, नहीं मिला. मुस्लिम ओबीसी को मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने बाद शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना तो संभव तो हुआ लेकिन प्रतिनिध्तिव कुछ विशेष नहीं रहा (सच्चर समिति के अनुसार) जिसका मुख्य कारण है आरक्षण के अधिकार को प्राप्त करने की योग्यता ही न होना.
अब इस तथ्य का स्पष्ट रूप से कई सरकारी दस्तावेजों में उल्लेख हो चुका है कि भारतीय मुस्लिम समाज एक एकांगी समाज नहीं है. सच्चर समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि मुस्लिम समाज तीन स्तरों में विभाजित है: अशराफ (सामान्य), अज्लाफ़ (ओबीसी के बराबर) और अर्जाल (अनुसूचित जाति के बराबर). संभवतः पहली बार किसी सरकारी रिपोर्ट में अब तक एकांगी समझे जाने वाले समाज के विषय में इस प्रकार का उल्लेख किया गया.
साफ़ है कि इस आधार पर ही राजनीतिक दिशा में क़दम बढ़ाया जाना चाहिए. साथ ही साथ Presidential Order, 1950 में दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन को अब तक जगह नहीं मिली है, और इससे सम्बंधित याचिका अभी कोर्ट में लंबित है. इसके लिए निरंतर राजनीतिक प्रयास भी किये जा रहे हैं लेकिन मुख्य राजनीति में आज भी यह बात खुलकर सामने नहीं रखी गयी है.
उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के नाम पर की जा रही है “माइनॉरिटी पॉलिटिक्स” प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है. अब तक जिस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियाँ देश में उत्पन्न की गयीं उसमे साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का बोलबाला रहा है. जिसका अर्थ ये भी है कि वोट डरा कर लिए गए. माइनॉरिटी पॉलिटिक्स मुख्यतः चूँकि प्रतीकात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द- यानि उर्दू, अलीगढ़, मदरसा इत्यादि के ही आस-पास घूमती रही, जिसके कारण धर्मनिरपेक्ष मुद्दों जैसे शिक्षा, समाजिक न्याय और रोज़गार जैसे मुद्दे कभी मुख्य रूप से आगे नहीं आ पाए. यहाँ यह समझना होगा कि सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दे भी आवश्यक हैं लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्राथमिकतायें अब तय करनी होंगी.
चूँकि अब राजनीतिक नियम बदल रहे हैं, इसलिए नयी राजनीतिकता से अपेक्षित है कि वह इन तथ्यों की गहराई में जाए और समझे कि आम मुस्लिम समाज को राज्य के नीतिगत मामलो में धर्म के आधार पर न पहचान कर साम्प्रदायिकता के खतरे न उठाये जाएँ. उचित यही होगा कि एक सामान्य भारतीय नागरिक की तरह ही सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उसके आस्तित्व को स्वीकार कर सामूहिक विकास और पारदर्शी सरकार की परिकल्पना की जाये.
(लेखक जे.एन.यू. में शोध छात्र हैं. इनसे merajahmad1984@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.)