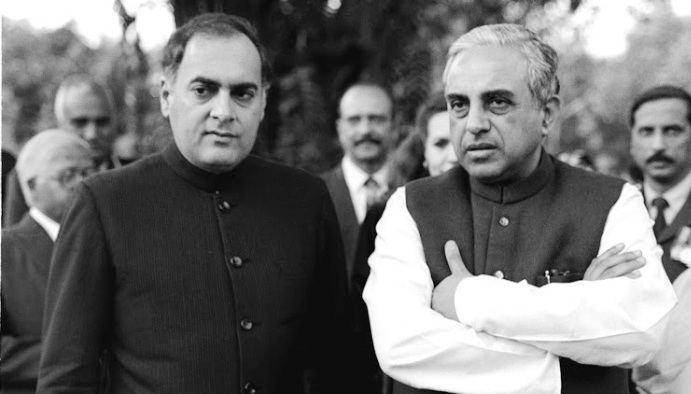Afaque Haider for BeyondHeadlines
मुम्बई बम बलास्ट में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये याकूब मेमन को हाल ही में दिये गये मृत्युदंड ने न्याय की अवधारणा पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं. एक बार फिर मृत्युदंड और न्याय आम लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गया है.
मेमन की फांसी से पहले आखिरी लम्हों में हुए न्यायालय की कार्रवाई ने न्यायतंत्र की न्याय प्रणाली पर भी कई प्रश्न चिन्ह लगाएं हैं. इस कार्रवाई पर न केवल जनता बल्कि बु़द्धिजीवी वर्ग भी बंटे दिखाई पड़ रहे हैं. जहां एक वर्ग इसे जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन मान रहा है और मृत्युदंड को इस अधिकार का विरोधाभास मान रहा है. वहीं दूसरा वर्ग इसे पीडि़तों को मिलने वाले न्याय के रूप में देख रहा है. लेकिन सवाल अब भी बरक़रार है कि क्या मानव निर्मित कोई संस्था न्याय करने के लिए सक्षम है?
मशहूर फिलॉस्फर जॉन रॉल्स ने अपनी किताब ‘A Theory of Justice’ में कहा है कि ‘न्याय का सिद्धांत’ निष्पक्षता पर टिका होता है. जिसके लिए न्यायिक संस्थाओं की ज़रूरत है. इन संस्थाओं के सामने हर कोई समान होगा. एक बेख़बरी का पर्दा होगा, जो रॉल्स के अवधारण में Veil of ignorance है. न्याय की पूरी कल्पना इसी इग्नोरेंस पर टिकी होती है. राजा हो या रंक कानून के सामने सभी बराबर होंगे. इस पर्दे के पीछे कौन होगा कानून इससे बेख़बर होगा.
लेकिन रॉल्स का यह सिद्धांत और न्याय की यह प्रणाली व्यवहारिक जीवन और यथार्थ के धरातल पर कहीं बैठती हुई दिखाई नहीं देती है. कानून के राज्य में सभी समान होतें हैं और सभी कानून से नीचे होते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब कानून का एक रूप हो, न्याय का एक रंग हो. न्याय की देवी के आंखों में भले ही पट्टी बंधी होती है. परन्तु न्याय के मंदिरों के पुजारियों के आंख, कान और नाक सभी खुले होते हैं.
आंकडे़ बतातें हैं कि 85 प्रतिशत मृत्युदंड पाने वाले अधिकतर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं, जिनका संबंध समाज के शोषित तबके से होता है. हाल ही में दैनिक इंडियन एक्सप्रेस के एक सर्वे में पाया गया कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम अल्पसंख्यक अपनी आबादी से डेढ़ गुनाह हिन्दुस्तान के जेलों में बंद है, जबकि काबिले गौर बात यह है कि दूसरे तबके के अनुपात में ये कम दोषी पाये जाते हैं.
न्यायतंत्र से जुड़े आंकडें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या न्याय सबके लिए समान है या इसके कई रंग हैं. सलमान खान को जहां अदालत ने केवल मिनटों में बेल दे दिया, वहीं इसी देश में कई ऐसे भी केस हैं जहां केवल बेल के कागज़ात नहीं पहुंचने के कारण बिना किसी जुर्म के लोग दश्कों तक बंद रहे हैं.
याकूब मेमन को बॉम्बे बम बलास्ट की साजि़श में अदालत ने दोषी पाया, जिसके लिए उसे मौत की सज़ा दी गयी. लेकिन क्या 235 लोगों की मौत के लिए किसी एक को फांसी देना न्याय है. आखिर न्याय का दायरा इतना तंग क्यों है? बॉम्बे बम बलास्ट से ठीक पहले बॉम्बे में भीषण दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गये. सरकार ने इन दंगों की जांच के लिए जस्टिस श्रीकृष्ण कमीशन का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में साफ़ तौर पर दंगों के लिए शिवसेना और बालठाकरे को दोषी माना और बम बलास्ट का कारण बॉम्बे में हुए सांप्रदायिक दंगों को क़रार दिया.
श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट को सरकार और अवाम दोनों भूल गई. सरकार ने खुद कमीशन बनाई और रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाल दिया. जिन नेताओं की श्रीकृष्ण कमीशन ने निशानदेही की वह सत्ता की मलाई खाते रहें और जिन अफ़सरों को दंगों के लिए जिम्मेदार माना उन्हें सरकार प्रमोशन देती रही. सरकार के लिए दंगों में मारे गये निर्दोष लोगों के लिए न्याय के अलग अर्थ थें.
बाल ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में खुलेआम खून ख़राबे की बात कही जिसके नतीजे में बॉम्बे की ज़मीन लालाज़ार हो गयी. सामना में बाल ठाकरे के छपे लेख आज भी बतौर कनूनी दस्तावेज़ मौजूद हैं. लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई. दो साल PUCL ने बाल ठाकरे के खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन वह कानून से भी बड़ा हो गया, कानून के हाथ लंबे होते हुए भी कभी बॉम्बे के असली गुनाहगारों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाएं. जो पहली नज़र में कानूनन अपराधी था, उसके खिलाफ़ एक मुक़दमा तक ना चल पाया. ठीक 20 साल बाद बाल ठाकरे की मौत पर एक बच्ची द्वारा मुम्बई बंद पर किये गये सवाल पर हुकूमते वक़्त ने उसे उसी धारा के तहत बंद कर दिया जिस धारा के तहत कभी बाल ठाकरे को जेल जाना था.
ये सारे तथ्य इस बात की पुष्ठी करते हैं कि न्यायतंत्र की बुनियाद कितनी खोखली है और इसके केवल एक रंग नहीं हैं बल्कि कई रंग हैं.
मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्याय में कहा था कि जहां पक्षपात होगा वहां न्याय कैसा? कोई भी मानव निर्मित कृत्रिम न्यायतंत्र पक्षपातहीन हो मुमकिन नहीं है. क्योंकि न्यायतंत्र के ये अगवा भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज का हिस्सा हम सब हैं. उनकी भी अपनी कमजोरियां और झुकाव होता है. अतः यह तंत्र पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं हो सकता. हम न्याय के लिए न्याययिक संस्था तो बना सकते हैं, लेकिन इसे चलाने वाले फरिश्ते नहीं होते बल्कि इंसान ही होते हैं.
जहां तक सवाल न्याय और मृत्युदंड का है, तो मृत्युदंड पूरी तरह से जजों के विवेकाधिकार पर निर्भर होता है. वह किस अपराध को मृत्युदंड के लायक माने और किसे नहीं. इसकी सबसे बेहतर मिसाल गुजरात के दंगों में माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और जयदीप पटेल को मिलने वाली सजा है. जयोसना यगनिक ने ये कहकर मृत्युदंड की सजा नहीं दी, क्योंकि वह खुद मुत्युदंड की सजा पर विश्वास नहीं करती हैं. जबकि ये मामल दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का था. जहां दोषियों ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी थीं.
ठीक इसी तरह ग्राहम स्टेंस और उसके दो बच्चों के नृशंष हत्या के लिए अदालत ने दारा सिंह को फांसी की सजा नहीं दी, जबकि इसके बरक्स अफ़ज़ल गुरू के मुक़दमे में जज ने राष्ट्र की सामूहिक चेतना को संतुष्ट करने का हवाला देकर मृत्युदंड को दुरूस्त ठहराया. अदालत का ये फैसला अपने आपमें न्याययिक से ज्यादा राजनीतिक मालूम होता है.
राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी अपराधी की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है. लेकिन राष्ट्रपति इस मामले में भी कैबिनेट से सलाह लेता है और उसके अनुसार ही फैसला करता है. कैबिनेट की तरफ़ से ये फैसला गृह मंत्रालय ही मुख्य रूप से लेता है. जब बात कैबिनेट और गृह मंत्रालय की आ जाती है तब मामला स्वयं राजनीतिक हो जाता है.
सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर ही फैसले लेतें हैं. नहीं तो जो सरकार अफ़ज़ल गुरू और याकूब मेमन को तख्तेदार पर लटकता देखने को बेचैन थी, वह राजीव गांधी और बेअंत सिंह के हत्यारों में इतनी उदासीनता क्यों दिखाती. मालूम होता है कि न्याय अपने चरित्र में न्याययिक कम राजनीतिक ज्यादा है. सजा-ए-मौत सियासत के हाथ में एक आला सियासी हथियार है. एक ही अपराध और धाराओं में बंद अलग अलग अपराधियों के लिए सरकार और न्यायतंत्र का रवैया बिल्कुल अलग है. ये इस सत्य की पुष्टि करता है कि न्याय के सचमुच कई रंग हैं.
न्याययिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी अपराधी की दया याचिका उसके फांसी से कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति ने खारिज की हो. सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके कुछ दिन और जिंदा रहने की दया याचिका भी उसके मरने से महज़ दो घंटे पहले ही खारिज की. काबिले दिलचस्प बात ये है कि जिस न्यायतंत्र में याकूब मेमन को 22 साल तक सलाखों के पीछे जिन्दा रखा चंद दिन और रखने से डर गयी.
आखिर सरकार को कुछ अपराधियों में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है. दूसरी तरफ़ खुद सरकार द्वारा बम्बई दंगों पर गठित श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट कचरे के डब्बे में डाल दी गयी. जिन लोगों को जस्टिस श्रीकृष्ण ने दोषी बनाया उन्हें सरकार ने नायक बना दिया. ये इस सच्चाई कि तस्दीक करता है कि इंसाफ़ के कई रंग है. मानव द्वारा निर्मित इन न्याययिक संस्थाओं की बुनियाद बेहद खोखली है. ऐसे में याकूब मेमन की फांसी पर एक प्रश्न तो स्वाभाविक है कि क्या मानव निर्मित कृत्रिम व्यवस्था को ये अधिकार देना चाहिए कि वह ईश्वर द्वारा निर्मित प्राकृतिक जीवन को समाप्त कर दे?
(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हैं. ये लेखक के अपने विचार हैं.)