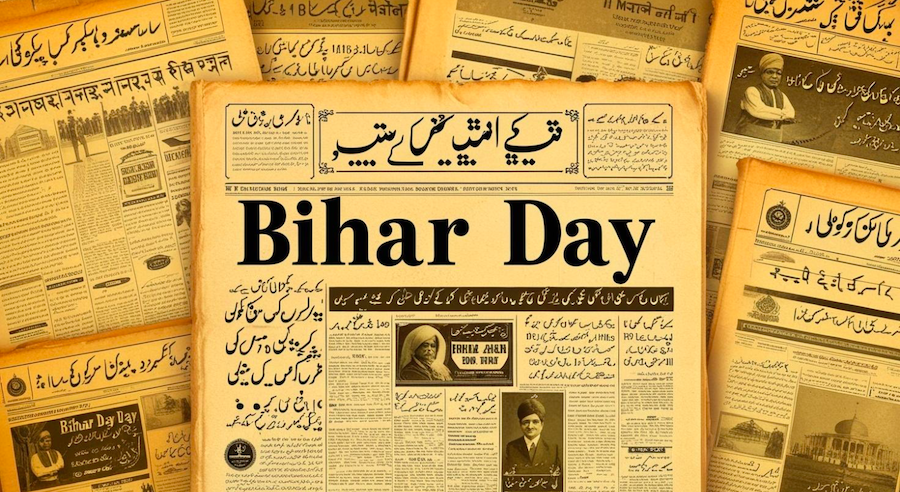Nandini Sundar
मैं टेलीविजन पर होने वाले चर्चाओं से तंग आ गयी हूँ जिसमें अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या माओवादियों के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का रवैया नरम है? कोई ये क्यों नहीं पूछता कि हमारे सम्मानीय राजनेताओं और रक्षा विशेषज्ञों का, पुलिस हिरासत में होने वाले प्रताड़ना और गैर कानूनी हत्याओं पर नरम रुख क्यों रहता है?
टेलीविजन पर लोग गंभीर चर्चाओं में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं रखते, वो मात्र यहीं चाहते हैं कि माओवादियों की करनी के लिए हम प्रताड़ना से गुजरें. अर्नब गोस्वामी का प्रोफ़ेसर हरगोपाल का “सैधांतिक विश्लेषण” देने पर मजाक बनाना बहुत ही बुरा अनुभव था. अगर भयभीत मुद्रा में उतेजना के साथ माओवादियों के खात्मे के लिए सेना भेजने की बात करना ही “विश्लेषण” है और बाकी सभी का नज़रिया पूर्वाग्रह है तो फिर ऐसे किसी पैनल की ज़रूरत ही क्या है?
 मीडिया की शब्दावली बहुत ही सीमित है. मुझे याद है बिनायक सेन का एक साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने माओवादी हिंसा की ‘निंदा” की और प्रस्तुतकर्ता लगातार पूछे जा रहा था कि क्या उन्होंने “भर्त्सना” की. जहाँ तक मुझे पता है दोनों शब्दों का लगभग एक ही मतलब होता है. आज कल इससे पहले कि मीडिया मुझसे पूछे मैं ही चिल्लाने लगती हूँ ” हाँ! मैं निंदा करती हूँ, हाँ! मैं निंदा करती हूँ” मैं नींद से उठ कर चिल्लाने लगती हूँ “मैं निंदा करती हूँ”. मुझे दुसरे किसी शब्द के इस्तेमाल पर डर लगता है क्योंकि मीडिया को इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आता.
मीडिया की शब्दावली बहुत ही सीमित है. मुझे याद है बिनायक सेन का एक साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने माओवादी हिंसा की ‘निंदा” की और प्रस्तुतकर्ता लगातार पूछे जा रहा था कि क्या उन्होंने “भर्त्सना” की. जहाँ तक मुझे पता है दोनों शब्दों का लगभग एक ही मतलब होता है. आज कल इससे पहले कि मीडिया मुझसे पूछे मैं ही चिल्लाने लगती हूँ ” हाँ! मैं निंदा करती हूँ, हाँ! मैं निंदा करती हूँ” मैं नींद से उठ कर चिल्लाने लगती हूँ “मैं निंदा करती हूँ”. मुझे दुसरे किसी शब्द के इस्तेमाल पर डर लगता है क्योंकि मीडिया को इसके अलावा कुछ और समझ में नहीं आता.
टेलीविजन पर होने वाले चर्चाओं में मेरे शामिल होने का मात्र एक कारण यह है कि मेरे पास मेरे विचारों को जाहिर करने के लिए बहुत ही सीमित जगह है. वैसे तो मीडिया इस बात से बेपरवाह रहती है कि वास्तव में बस्तर जैसे जगहों में क्या हो रहा है पर जब कभी नागरिकों की बड़े तादाद में मौत होती है, तो कोई भी चर्चा और ख़बरें नहीं दिखाई जाती हैं. मजबूरन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी ऐसे प्रतिकूल माहौल में बोलना पड़ता है, क्योंकि यही मात्र ऐसा समय होता है जब मीडिया हमारे विचारों में दिलचस्पी दिखाती है, इसलिए नहीं कि वो हमें सुनना चाहते हैं इसलिये क्योंकि उन्हें अपने “मुकाबला” की रेटिंग बढानी होती है. इसे कहते हैं “संतुलन”. प्रस्तुतकर्ता (एंकर) की निराशा तब दिखती है जब चर्चा में शामिल लोग असहमति के बजाय कई मुद्दों पर सहमत हो जाते हैं.
25 मई की घटना के बाद तो मेरे मत को जानने के लिए पत्रकारों के कॉल्स की बाढ़ सी आ गयी है. पर जब मैं लिखना चाहती हूँ तो बहुत ही सीमित जगह मिलती हैं. एक बड़े समाचार पत्र ने महेंद्र करमा की ह्त्या पर मेरे विचारों को प्रकाशित करने से मना कर दिया, तब तक उनके पास ऐसे कई लेख थें जो सैनिक बलों के इस्तेमाल की वकालत कर रहे थें. और जब मेरे विचारों को प्रकाशित किया गया तो वो भी एक शब्द सीमा के अंतर्गत थें. मैंने राष्ट्रीय मीडिया में सलवा जुडूम पर लिखा गया अब तक का पहला लेख 2006 में लिखा था, जिसमें मात्र 800 शब्दों को जगह मिली थे. सलवा जुडूम के पहले वर्ष में, सलवा जुडूम पर प्रकाशित निबंधों को मैं आसानी से गिनती कर बता सकती हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से कई संपादको से मिली और उन्हें तस्वीरों के साथ प्रमाण भी दिखाएँ और टेलीविजन संपादको से आग्रह भी किया की इस पर एक चर्चा कराई जाए पर किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई. अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई होती तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती.
मैं 2005 से ही लिखना चाह रही हूँ, क्योंकि आखिरकार मैं एक एंथ्रोपोलोजिस्त हूँ. मेरा दिमाग मीडिया के शोर और उन लेखों से जो लगातार एक ही बात दुहराते हैं, से इस तरह जकड़ गया है कि मैं यहीं सोचती हूँ चूँकि कोइ नहीं सुन रहा है मैं नहीं लिखूंगी.
मैं यहाँ अपने लेख “भावनात्मक युद्ध” का एक टुकडा प्रस्तुत करना चाहूंगी जो मैंने अप्रैल 2010 में केंद्रीय सुरक्षा बल के 76 जवानों की मौत पर लोगों की प्रतिक्रया पर लिखा था. यह निबन्ध “Third World Quarterly” में प्रकाशित किया गया था.
“सरकार का गुस्सा मात्र माओवादियों के खिलाफ नहीं था बल्कि कथित रूप से “माओवादियों के लिए सहानुभूति रखने वालों” (जैसा कि सरकार अक्सर कहती है) के लिए भी था, जिनके द्वारा संविधान और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, सरकार की मौखिक और लिखित आलोचना को नैतिक रूप से माओवादियों द्वारा उन नीतियों के खिलाफ बदले में की गयी कार्यवाही के बराबर माना जा रहा था. कुछ ही मिनटों के अन्दर, चूँकि सरकार ही प्राथमिक रूप से ख़बरों को परिभाषित करती है, चाहें कथित सहानुभूति रखने वालों ने हमले की पर्याप्त आलोचना की हो या नहीं, इसे हमले की ख़बरों की तरह ही दिखाया जाने लगा.
सरकार और मीडिया का एकतरफा क्रोध शायद ही आम आदिवासियों को चुन चुन कर मारने या बलात्कार के खिलाफ गृह मंत्री द्वारा भर्त्सना की मांग करता है. इससे हर्मन और चोम्स्की द्वारा बताये गए “अयोग्य और योग्य पीड़ित” के बीच का अंतर ख़याल में आता है जिसे उन्होंने मीडिया के “प्रोपेगेंडा मॉडल” का हिस्सा बताया है, जबकि मीडिया द्वारा “योग्य पीड़ितों” की ख़बरें विस्तृत तथा गुस्से और सदमों से भरी रहती है, “अयोग्य पीड़ितों” को बहुत ही सीमित जगह मिलती है और उनकी ख़बरों को बहुत ही सामान्य तरीके से दिखाया जाता है, और इस बात का बहुत ही कम प्रयास किया जाता है कि किसी को जिम्मेदार बताया जाए या फिर सत्ता में ऊँचे ओहदे पर बैठे लोगों के भी दोष का भी पता किया जाए.
(यह लेख नंदिनी सुन्दर द्वारा अंग्रेज़ी में लिखे गए लेख On the Media’s Need for Whipping Boys का हिन्दी अनुवाद है, जिसे धीरज द्वारा किया गया है. अंग्रेज़ी में इस लेख को http://nandinisundar.blogspot.in/2013/06/on-medias-need-for-whipping-boys.html पर देख सकते हैं.)