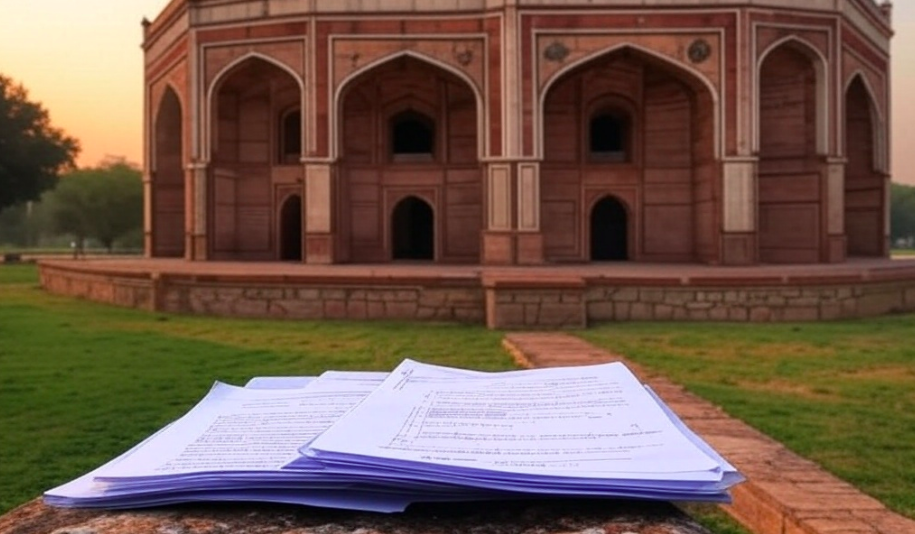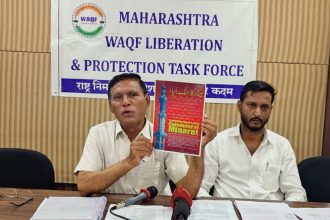1947 के पहले मुल्क में जो बड़े मीडिया घराने थे, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में निकालने वाले अख़बारों के मालिक थे, उनका वही चरित्र था, जो आज है. सत्ता के साथ गठजोड़. और दूसरी तरफ़ बहुत तरह के वैसे लोग थे, जो किसी न किसी स्तर पर आज़ादी की बात करते थे. लोकतंत्र की बात करते थे.
ऐसा नहीं है कि जो छोटे-छोटे अख़बार निकले, उनका अपना इंट्रेस्ट नहीं था. कई धार्मिक कारणों से पत्रकारिता कर रहे थे, कुछ जातिगत वर्चस्व को लेकर पत्रकारिता में सक्रिय थे. महिलाओं ने बहुत सारी पत्र-पत्रिकाएं निकालीं. अपनी आज़ादी के लिए निकाला. इस तरह से आप पाएंगे कि उस दौर में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उन तमाम भाषाओं में लोगों ने अपनी राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और लोकतंत्र की चाहत में पत्रकारिता की. समाज, राजनीति में नए मूल्यों को स्थापित करने की बेचैनी दिखती है.
मुझे लगता है कि आज़ादी के पहले की पत्रकारिता के दो शब्द महत्वपूर्ण हैं. वो दो शब्द हैं — लोकतंत्र और समानता. समाज में समानता होनी चाहिए. और समानता के साथ लोकतंत्र होना चाहिए. ये पत्रकारिता की चाहत थी. इसीलिए लोगों ने यह कहा कि पत्रकारिता जो हमारे यहां है, वो एक सामाजिक ज़िम्मेवारी का काम है. इसलिए उस समय ये पत्र-पत्रिकाएं समाज सुधार की बात करती थीं. दहेज नहीं लेना है. महिलाओं पर उत्पीड़न नहीं करना है. छूआछूत नहीं मानना है. ये तमाम तरह की बातें, आज़ादी के पहले पत्रकारिता का हिस्सा थीं.
लेकिन जो लोग बाज़ार में अपना वर्चस्व रखते थे. यानी जो मीडिया घराने थे. उन मीडिया घरानों ने, ये जितनी जगह हम लोगों ने बनाई थी. वो सब ख़त्म कर दिया. यहां हम लोगों का मतलब भारत के विभिन्न तरह के लोग. महिलाओं ने. पुरूषों ने. दलितों ने. आदिवासियों ने. सवर्णों ने. जो भी जगह अपने-अपने स्तर से बनाई थी. जो जगह समाज के विभिन्न हिस्सों में इन लोगों ने तैयार किया था. उन सारी जगहों को बड़े मीडिया घरानों ने अपना क़ब्ज़ा जमा लिया.
आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा संकट यह है कि विभिन्न स्तरों पर जो अख़बार निकला करते थे. वो 1947 के बाद धीरे-धीरे बड़ी कंपनियों के भीतर समा गए. ये सबसे ज़्यादा ख़तरा लोकतंत्र और समानता की जो चेतना है, उसके लिए दिखाई दे रहा है. विविधता से भरे समाज में विकेन्द्रीकरण की चेतना बहुत महत्वपूर्ण होती है. यह विकेन्द्रीकरण राजनीतिक सत्ता का ही नहीं. यह हर स्तर पर कारगर हो इसकी ज़रूरत को सक्रिय रखती है. मीडिया में भी केन्द्रीकरण उतनी ही ख़तरनाक है जितनी राजनीतिक तौर पर केन्द्रीकरण को लोकतंत्र के लिए ख़तरा माना जाता है.
आप सोचिए! आज़ादी के पहले महिलाओं के लिए कितनी पत्रिकाएं निकलती थी, मालूम है. सैकड़ों की संख्या में. आज आप बताईए कितनी महिलाओं के पत्रिकाओं के नाम जानते हैं? एक, दो, तीन, चार. इससे ज़्यादा नहीं. और जो तीन-चार पत्रिकाएं हैं वो क्या खेतों में काम करने वाली महिलाओं की बात करती है. घरों में काम करने वाली जो साधारण महिलाएं हैं, उनकी बात करती है. नहीं, बिल्कुल नहीं. यानी आज़ादी के बाद की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें देश की अधिकत्तर महिलाओं की आज़ादी को समेटने के लिए इस्तेमाल होते हम देख रहे हैं.
आज टीवी चैनल किसकी बात करता है. क्या वो साधारण महिलाओं की बात करते हैं. नहीं. वो गहने से लदी हुई, बहुत ही क़ीमती साड़ियां पहनी हुई, छल-प्रपंच करने वाली महिलाओं की बात करता है. सारी की सारी महिलाओं की एक ग़लत तस्वीर इसने बना रखी है. यानी आर्थिक सत्ता और उसकी भव्यता का प्रदर्शन और उसके पतनशील मूल्यों को स्थापित करते हम देख रहे हैं.
जब आप इन चीज़ों पर ग़ौर करेंगे तो पाएंगे कि पूरी की पूरी पत्रकारिता और मीडिया का जो कारोबार है, वो उल्टी दिशा में चला गया है. अब लोग कहते हैं कि मीडिया एक व्यवसाय है. मीडिया के ज़रिए चीज़ें बेची जाती हैं. पहले लोगों के लिए मीडिया थी. आज लोगों के लिए मीडिया नहीं है. मीडिया के लिए लोग हैं. आज़ादी के बाद आज की पत्रकारिता में ये एक सबसे बड़ा फ़र्क़ आ गया है.
देश का सबसे बड़ा मीडिया घराना जो हैं उसके मालिक कहते हैं कि वे न्यूज़ के कारोबार में नहीं हैं बल्कि वे तो विज्ञापन के कारोबार के लिए न्यूज़ पेपर निकालते हैं. इस तरह आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के कारोबार के लिए संविधान में नागरिकों को दिए गए अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है. यह पूंजीवाद द्वारा उस संविधान का इस्तेमाल है जो कि समानता की बात करता है.
मीडिया अब जैसा चाहती है, उस तरह से लोगों को अपनी धुन पर नचा सकती है. कितना हंसना है. क्या पहनना है. क्या खाना है. कैसे रहना है. कितना आपको हिन्दू बन जाना है. कितना मुसलमान रहना है. कितना सिक्ख बनना है. कितना धर्म-निरपेक्ष बनना है. आज सबकुछ मीडिया तय करती है. 24 घंटे हम उसकी निगरानी में रहते हैं. हमारे 24 घंटे का उसके पास पूरा एक रूटिन रहता है. और हम उसके साथ-साथ, उसके पीछे-पीछे चलते हैं.
आज़ादी के बाद आज के दौर में आपको एक भी टीवी चैनल या अख़बार ऐसा नहीं मिलेगा जो नागरिकों के लिए निकलता हो. यानी भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए. आज जो भी चैनल या अख़बार निकलते हैं वो अपने अपने पाठकों व दर्शकों के लिए चलते हैं.
मान लीजिए कि अगर हमारे पाठक ठेकेदार हों, तो हम ठेकेदार के मन-मिज़ाज का अख़बार निकालेंगे. हमारा न्यूज़ चैनल अगर कम्यूनल यानी साम्प्रदायिक लोग देखते हों तो फिर हम उनके मन मुताबिक़ ही बात करेंगे. महिलाओं की आज़ादी के ख़िलाफ़ सोचने वालों के लिए वैसा ही मीडिया हाउस चलाएंगे. वे मीडिया हाउस तो कहेंगे कि हमारे लोग यही पसंद करते हैं. इसलिए हम यही दिखाएंगे.
भारतीय नागरिकता का सवाल यानी भारतीय नागरिकों के लिए हम अख़बार निकाल रहे हैं, ये बात तो बहुत पीछे चली गई है. अधिकार का इस्तेमाल आप कर रहे हैं संविधान का. और संविधान बात करता है नागरिकों की. लेकिन आप उस संविधान के अधिकार का इस्तेमाल अपने घर के लोगों के लिए कर रहे हैं. अपने पाठकों के लिए कर रहे हैं. आख़िर ये पाठक या दर्शक आप के घर के लोग ही तो हैं.
मुझे लगता है कि मीडिया में आज एक बुनियादी तब्दीली आ गई है. और इस बदलाव को लोग अगर चाहे तो दुरूस्त कर सकते हैं. लोगों को दुरूस्त करना ही चाहिए. और दुरूस्त करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीक़ा यही है कि जैसे ही आपके मन में ख़्याल आता है कि हमको दस लोगों के बीच लगातार संवाद करने के लिए कोई वेबसाईट या अख़बार शुरू करना है, चैनल शुरू करना है. तो हम उतने के लिए ही काम शुरू कर देंगे. हम इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि 100-500 लोग जुटेंगे तब हम बात शुरू करेंगे.
संवाद महत्वपूर्ण है. संवाद के लिए माध्यमों की ज़रूरत यह होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. संवाद की बुनावट करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है. एक तरह का संवाद कबीर से तैयार किया, आज तक लोगों के लिए वह ज़रूरी लगता है. अब तो संवाद को तैयार करने का काम पीछे छूट गया है और माध्यम की ज़रूरत पर ज़ोर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है. यह उल्टी वाणी है.
आप बस शुरू कर दीजिए. नहीं तो हर वक़्त आप कहेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है और हमारे इतने छोटे से प्रयास से क्या होगा. तो आप सोचिए कि आप जितनी देर कीजिएगा, वो साम्राज्य उतना ही फैलता जाएगा. आप अपने प्रयास से जो स्पेस बनाएंगे, वो स्पेस अब तक वो साम्राज्य ही ले रहा था, कम से कम अब उसके पास नहीं जाएगा. आपको जब भी ऐसा मौक़ा मिलता है, आप लोकतंत्र और संविधान के नागरिकों के लिए अख़बार, चैनल या वेबसाइट शुरू करें. याद रहे अपने पाठकों-दर्शकों के लिए नहीं. संविधान के लिए और देश के नागरिकों के लिए अपना ये काम पहले करें. और यही सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है.
(अफ़रोज़ आलम साहिल से बातचीत पर आधारित)