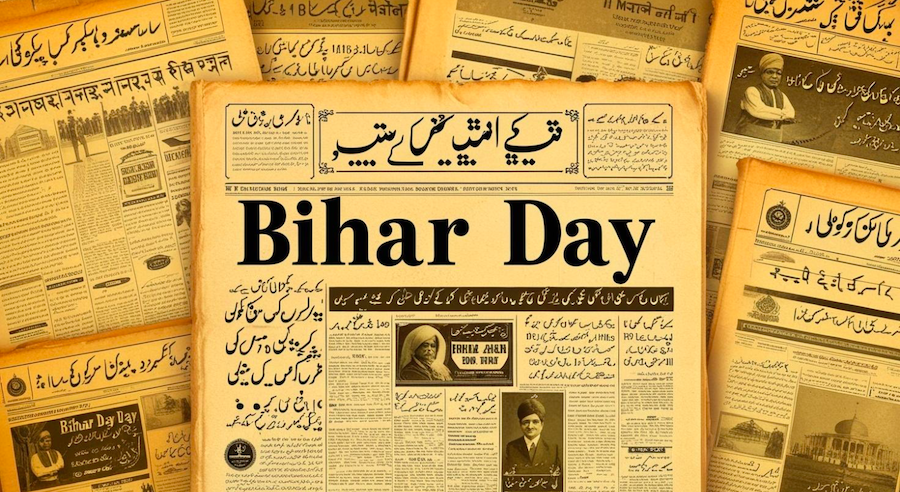Afroz Alam Sahil for BeyondHeadlines
आज़ादी की लड़ाई केवल चुने हुए नेताओं ने ही नहीं लड़ी थी, बल्कि देश का हर नागरिक इसमें सम्मिलित हुआ था. अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्र भारत के शासन में देश के हर नागरिक का भी हाथ हो. इस दृष्टि से तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग तथा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग ले चुके महापुरूषों ने देश की शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नई नीतियां बनायीं और संविधान का निर्माण किया. हमने भी 26 जनवरी 1950 में लोकतंत्र को भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्वीकार किया और देश को गणतंत्र का दर्जा दिया.
लेकिन यदि आज देखें तो क्या संविधान निर्माताओं की मेहनत सफल हो पायी है? क्या उनके सपने पूरे हो गए? शायद नहीं! क्योंकि बंगाल से आए रिक्शाचालक लाल बाबू के लिए गणतंत्र दिवस का परेड देखना आज भी एक सपना है. वो कहते हैं कि “ गांव में थे तो वहां टीवी पर झंडा फहराते हुए लोगों को देखता था. मेरे हाथ खुद बखुद उठकर झंडे को सलामी देती थी, सोचा कि दिल्ली जाकर क़रीब से देखुंगा. पर दिल्ली में आकर ऐसा मुमकिन न हो सका. पिछले 3 सालों से अपनी मेहनत की कमाई से टिकट के लिए जाता हूं, पर टिकट देने वालों के ज़रिया भगा दिया जाता है.” रिक्शाचालक रोहित को तो यह तक नहीं पता कि यह गणतंत्र दिवस क्या होता है और क्यों होता है? उसे बस इतना पता है कि इस रात उसे रोड पर सोने नहीं दिया जाएगा. वो कहता है कि शायद हम गरीबों के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है. लोग हम पर ज़ुल्म करते हैं, मारते-पीटते हैं और जब थाने में जाओ तो पुलिस वाले भी यही करके भगा देते हैं. वो बोलते-बोलते रो पड़ता है.
यह सिर्फ लाल बाबू और रोहित की ही कहानी नहीं है, बल्कि देश के हर गरीब की है. यही नहीं, हमारा समाज जितना विभाजित आज है, उतना पहले कभी नहीं रहा. आज हम जुड़ने के बजाय बिखरे पड़े हैं. धर्म, राष्ट्रीयता और एकता की बातें पुरानी पड़ गई हैं और जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रीयता के आधार पर नई पहचानें सर्वोपरि हो गई हैं. एक समय था जब हम अपनी सारी कमज़ोरियों, कमियों, ग़रीबी और गुलामी के बावजूद एक थे, परन्तु आज कोई यहां कहने का साहस नहीं करता कि जो भी हमें हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई , अगड़ी-पिछड़ी जातियां, उत्तर-दक्षिण, ग्रामीण-शहरी अथवा हिन्दी-अहिन्दी भाषियों में बांटने की कोशिश करता है अर्थात जो भी देश की एकता के विरूद्ध काम करता है, वह हमारे देश भारत का दुश्मन है. आज हमारे देश के नेता ही धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना वोट बैंक बनाते हैं. जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं. चुनाव जीतने के बाद इन्हे संसद और विधान सभाओं में जगह मिलती है, सरकार बनती है और संसदीय लोकतंत्र चलता है. यही कारण है कि लोकतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्रीय भावना के निर्माण का एक संगठित भारतीय समाज की पहचान बनाने का हमारा उद्देश्य पूरा न हो सका. अब प्रश्न यह उठता है कि आखि़र हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था क्यों चुनी?
मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि दास को अपने स्वामी की हर बात आदर्श लगती है. वह वैसा ही बनना चाहता है. पश्चिम देशों की गुलामी में सदियों तड़पने के बाद यह स्वाभाविक था कि हम अपने मालिकों के देश शासन शैली और संस्थाओं की ओर आकृष्ट होते तथा इन्हें ही सर्वोत्तम और अनुकरणीय मानते। आज़ादी के संघर्ष के दिनों में भी राष्ट्रीय आन्दोलन के नायकों की मांग रही थी कि भारतीयों को भारत में भी वे सभी अधिकार व अवसर मिले जो अंग्रेज़ों को अपने देश में प्राप्त थे और वैसा ही संसदीय व्यवस्था स्थापित हो जैसा ब्रिटेन में था, पर ऐसा हो न सका.
दरअसल, आज़ादी का अर्थ होना चाहिए भारत के प्रत्येक गांव में पीने योग्य पानी, भूख से मुक्ति और बीमार पड़ने पर चिकित्सा की व्यवस्था किन्तु गणतंत्र के 63 वर्ष पूरे होने के बाद भी देश में एक लाख से अधिक गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. आज भी लगभग 30 प्रतिशत भारतीय निर्धनता की रेखा तले जीते हैं. लाखों को दो जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है. करोड़ों लोग रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं. आज भी स्कूल, चिकित्सा, मकान और अन्य बुनियादी सुविधाओं से करोड़ों लोग वंचित हैं.
आखि़र यह कैसी विडंबना है. लोकतंत्र का आधार मानव जीवन का मूल्य और व्यक्तियों के बीच समानता को माना जाता है, किन्तु हमारा सामाजिक जीवन और चिंतन आज भी सामंतवादी हैं. आज भी मनुष्य के जीवन की अलग-अलग कीमतें लगती हैं. कहीं एक बच्चे का प्रतिदिन का खर्च 5000 रूपये है तो कहीं मात्र 200-300 रूपये में आदिवासी माताएं अपने बच्चे को बेच डालती हैं. आखिर क्यों हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो वायदा किया गया था वो आज 59 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ? लगभग 9 फीसदी वार्षिक आर्थिक प्रगति दर का लाभ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही क़ैद है. गरीब किसान की उपजाऊ भूमि बिना उसकी मर्जी के छीन कर सेज को दी जा रही है. सूचना क्रांति और उदारीकरण से शहरों में बढ़ते रोज़गार के अवसर भी ग्रामीण नौजवानों की बेरोजगारी कम नहीं कर पा रहे हैं. हरित क्रांति और अनाज के भरे भंड