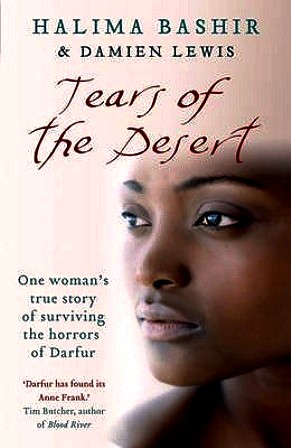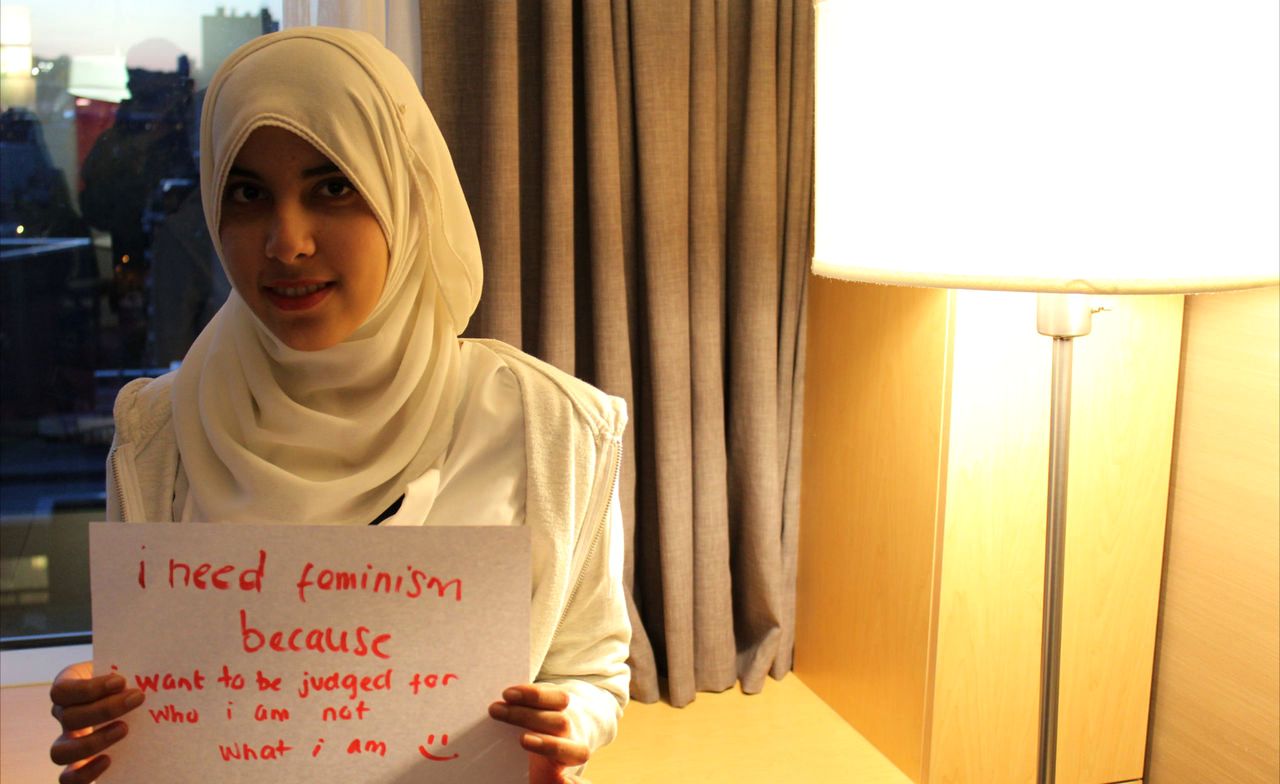Faiyaz Ahmad Wajeeh & Meraj Ahmad for BeyondHeadlines
तहलका की परम्परा से उसका पाठक वर्ग वाकिफ़ है. लेकिन परंपरा के इतिहास में उसके नए अध्याय को जिस तरह से सुर्खी मिली है उसने कई सवाल खड़े किये हैं.
हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं की तर्ज़ पर सबको कुछ न कुछ कहने का मौका मिल गया, और हद तो तब हो गयी जब बंगारू लक्ष्मण ने अपना बचाव पक्ष रखकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का हास्यापद प्रयास किया. तेजपाल मीडिया बिरादरी से आते हैं इसलिए कई न्यूज़ चैनलों और समाचार संपादकों के समक्ष ये बड़ा भावुक प्रश्न रहा कि इस पूरे प्रसंग को “कवर” कैसे किया जाये. मामला “हाई-प्रोफाइल केस” का ही नहीं, वर्किंग-प्लेस पर महिला अधिकार के हनन का भी है. तेजपाल के बदलते बयान और उनके सहयोगियों द्वारा बचाव पक्ष में दी गयी दलीलें साबित करने लगीं कि केस ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल भी नहीं है.
मीडिया ने इस मामले में तत्परता और सूझ-बूझ का परिचय दिया, और लगभग फुल ‘कवरेज’ दिया. प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में “nation wants to know” के स्टाइल में जमकर परिचर्चा हुई. कारण स्पष्ट है कि इस बार मीडियाकर्मी और मीडिया की अपनी साख कटघरे में है. इसलिए कवरेज के फुल लेंथ के पीछे की कहानी में मीडिया की मंशा भी ज़ाहिर थी कि इस पूरे प्रसंग की अवधि और स्पेस संकुचित होने के कारण कहीं मीडिया के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह न लग जाये. इतने बड़े कवरेज से महिला अधिकारों के प्रति सजगता ज़रुर आएगी और विशाखा जजमेंट (1997) को लैटर-एंड-स्पिरिट में लागू करने की कवायद को तेज़ करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक माहौल भी बनेगा. ये स्पष्ट हो चला है कि मीडिया में महिला अधिकार सम्बंधित परिचर्चाएं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा राजनीतिक दबाव के लिए आवश्यक हैं.
क्या महिला अधिकारों से सम्बंधित मुद्दे मीडिया के माध्यम से राजनीतिक बनाये जाने चाहिए यह एक बड़ा सवाल है. अगर ऐसा नहीं भी है तो निरंतर परिचर्चा स्वतः एक प्रकार से सामाजिक चेतना के साथ-साथ राजनीतिक केन्द्रों पर दबाव बनाने का काम करती ही हैं. लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे हाई-प्रोफाइल केस ही क्यों महिला अधिकारों के लिए उदहारण स्वरुप मीडिया को लुभाती हैं? क्या नारी का व्यवसाय, जाति और उसके धर्म को भी देखना आवश्यक है? मीडिया, विशेषकर दिसम्बर 16 की घटना के बाद, महिला अधिकारों के प्रति ‘सजग’ दिखती है. यहाँ हमें मीडिया की अपनी परिकल्पना में उस महिला को देखना होगा जिसको वो विशेष कारणों से विक्टिम बना कर पेश ही नहीं करती बल्कि उसको स्पेस भी देती है. इसके उलट बिना किसी ‘विशेष कारणों’ के मीडिया की परिकल्पना में दलित, आदिवासी और ऐसी कोई भी महिला अपने न्याय की लड़ाई में कितना स्थान पा सकी है?
क्या मीडिया दलित, आदिवासी, पिछड़ी और धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं की अस्मिताओं के लिए भी उतनी ही सजग है? क्या कवरेज और सामाजिक न्याय के असाधारण मामले में मीडिया को किसी भी महिला की जातिगत, धर्मिक, भाषाई या इलाकाई पहचान पर विशेष टिप्पणी और सजगता दिखानी चाहिए?
इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क के सर्वे (सितम्बर-अक्टूबर 2012) में दलित महिलाओं के रेप की कई घटनाएँ सामने आयीं जिनमें से कुछ बड़ी भयावह हैं. इस सर्वे के अनुसार लगभग 90% केसेस दर्ज ही नहीं हुए. हिसार के बहु-प्रचारित और चर्चित केस मे एक सोलह वर्षीया दलित महिला के साथ सात पुरुषों ने बलात्कार किया. ये सभी अपराधी उच्च जाति के हैं. यह मामला अभी भी लंबित है और पीड़िता इस सदमे से अब तक उबर नहीं पायी है. इस मामले में यह भी देखना चाहिए कि मीडिया ने इसको किस तरह कवर किया है.
इस तरह के घटनाक्रम को दैनिक समाचार पत्रों में ही देखा जाये तो हमारे समाज का एक और चरित्र निकल कर सामने आता है. कुछ बानगियाँ इस प्रकार हैं:
· द हिन्दू (अक्टूबर 19) की रिपोर्ट के अनुसार एक 56 वर्षीया दलित महिला ने पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. यहाँ यह कहने की ज़रूरत नहीं कि पीड़िता उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित और धमकायी गयी थी. बाद में महिला ने SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989 के तहत भी केस दर्ज करवाया.
· द हिन्दू (29 नवम्बर) की खबर के अनुसार एक और दलित महिला ने जान-माल के डर के कारण बन्दूक के लाइसेंस के लिए National Commission for Scheduled Castes में मदद की गुहार लगायी. इस घटना के पीछे भी जातीय संघर्ष की बात कही गयी है.
· तहलका की रिपोर्ट (अगस्त 30) के अनुसार जिंद शहर (हरियाणा) में एक दलित महिला के साथ न सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसकी हत्या भी कर दी गयी. पीड़िता के वकील का कथन है कि शुरुआत में पुलिस ने धारा 302 और 376, I.P.C., के तहत मुक़दमा दर्ज करने का प्रयास तो किया लेकिन SC/ST Act के तहत कोई धारा नहीं लगायी जा सकी. 25 अगस्त को जिंद के ही एक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में रेप और हत्या की बात सामने नहीं आयी- जिसके विरोध में परिवार वालों ने अन्तिम संस्कार करने से मना कर दिया. तत्पश्चात दलित समाज की कुछ संस्थाओं ने इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया.
· द हिन्दू (अक्टूबर 20) में प्रकाशित खबर के अनुसार हरियाणा के सिरसी जिले में एक दलित महिला के रेप की घटना फिर सामने आयी जिसमे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया.
· टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित हुई खबर (नवम्बर 8) के अनुसार एक दलित रेप सर्वाइवर ने हिसार जिला प्रशासन पर पीडिता की पीड़ा पर ध्यान न देने का आरोप लगाया. अपने पत्र में महिला ने National Commission for the Scheduled Castes (NCSC) को कहा कि उच्च जाति के कुछ लड़कों के लैंगिक आक्षेप के कारण उसका घर से निकलना बंद हो गया है.
· द हिन्दू की एक ख़बर (नवम्बर 30) के अनुसार दिन्दुगल जिला में दलित-वन्नियार ‘संघर्ष’ के पांच दिन बाद दलित टोला के सारे पुरुष (लगभग 300 परिवार) का कोई अता पता नहीं है. National SC/ST Welfare Commission, चेन्नई के डायरेक्टर डी. वेंकटेसन की माने तो, ‘एक छोटी व्यक्तिगत घटना (ईव-टीसिंग) ने उपद्रव का रूप ले लिया’. क्या इस घटना की तकनीकी और मुज़फ्फरनगर की उपद्रवी घटना में कोई समानता है, इस पर विचार करना चाहिए. मुज़फ्फरनगर उपद्रव ने जीवन की ही आहुति नहीं ली बल्कि महिला अस्मिताओं का भी चीर-हरण किया. इन अस्मिताओं पर कुछ इक्का-दुक्का अख़बारों, खासतौर से उर्दू मीडिया, को छोड़कर इन ख़बरों पर कोई चर्चा नहीं हुई. हाँ, कुछ समाजसेवी संगठनों ने जांच-पड़ताल की क़वायद में तत्परता ज़रूर दिखाई.
घटना के इन क्रमों को यहाँ दोहराने के पीछे सूचीकरण की कोई मंशा नहीं है. BeyondHeadlines ने ‘दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या, यौन शोषण, उत्पीडन की 101 गंभीर घटनाओं’ की पूरी लिस्ट पहले ही प्रकाशित कर दी है (1सितम्बर, 13).
क्या ऐसे किसी भी मामले में, यदि पीड़ित दलित या धार्मिक अल्पसंख्यक है तो विशेष क़ानून या विशेष कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए? क्या इन्हीं मामलों में मीडिया को अपने रोल का निर्धारण नहीं करना चाहिए?
प्रजातन्त्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र संस्थाएं हैं. इस का अर्थ यह भी है कि सरकारी संस्थाएं धार्मिक, जातिगत, भाषाई और इलाकाई ‘पहचान’ से ऊपर हों. निश्चित रूप से सरकारी संस्थाओं पर किसी भी पहचान के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाना उचित नहीं है. यह वास्तव में एक आदर्श स्थिति है- महिला अधिकार की लड़ाई यदि मीडिया में बिना ‘हाई प्रोफाइल केस’ बने स्वतः न्याय की प्रसांगिकता को सामने लाती है, और भविष्य में किसी भी भारतीय महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होता है तो यह एक आदर्श न्याय प्रक्रिया का उदाहरण है. इस आदर्श स्वरुप का हनन तब होता है जब हरियाणा जैसे राज्य में निरंतर दलित अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ की ख़बरें आती हैं और क़ानून व्यवस्था द्वारा शुरूआती चरण से ही न्याय न मिलने की शिकायतें कुंठा का रूप धर लेती हैं. सरकारी संस्थाओं पर सवाल तब उठ खड़ा होता है जब हारकर पीड़िता की ही जाति/धर्म/भाषा के लोग अन्याय के खिलाफ लामबंद होने के लिए बाध्य होते हैं, और ऐसे में मीडिया का दोहरा चरित्र खुल कर सामने आने लगता है.
आदर्श स्थति में महिला तो महिला ही है- उसकी ज़ात या धर्म क्योंकर देखी जाये? मामला तब उलझता है जब न्याय की गुहार का अनुत्तरित रहना और पीड़िता का एक वर्ग विशेष से होना बारम्बार संयोग बन जाता है. दलित तथा धार्मिक अल्संख्यक महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएँ निरंतर प्रकाश में आती रही हैं, लेकिन ऐसी घटनाएँ मुख्य रूप से मीडिया में शायद ही चर्चा के विषय की सामग्री बन पायी हों. यहाँ सवाल ये है कि मीडिया की इस आँख-मिचोली में ‘हाई-प्रोफाइल केस’ और ‘सामान्य केस’ की परिभाषा और मापदण्ड कौन तय करेगा? इस पर विचार करना होगा.
अंत में यह भी विचार करना होगा कि आखिर क्यों दलित, पिछड़े तथा धार्मिक अल्पसंख्यक की अस्मिताओं के प्रश्न पहचान-विशेष स्वयंसेवी संगठन उठाने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि यह सामान्य न्याय प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए. और यदि यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पा रहा हो तो मीडिया अपने उत्तरदायित्व से कैसे मुंह मोड़ सकती है. इस प्रकार की बाध्यताएं ऐसी पिछड़े वर्गों की उर्जा का निरर्थक व्यय नहीं तो और क्या है? हरिशंकर परसाई की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं- ‘भूमिपति ठाकुर मांग करने वाले हैं कि हरिजनों को मारने की सजा उन्हें न मिले. उनकी भी पवित्र परम्परा है. डाकू भी दंड सहित में संशोधन कराना चाहते हैं. उनकी भी सदियों की परम्परा है. इधर कायस्थ और कान्यकुब्ज भी अपने को कुछ धाराओं से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं. सुना है कि बहु को जला देने के अपराध को दंड-संहिता से निकाल देने की मांग होने वाली है, क्योंकि सती को जलाना प्राचीन पवित्र परंपरा है.’ कहीं हमारा देश जाने-अनजाने कुछ ‘प्राचीन और पवित्र’ परम्पराओं का निर्वाह तो नहीं किये जा रहा है?
(लेखक जे.एन.यू. में शोध छात्र हैं. इनसे faiyazwajeeh@gmail.com और merajahmad1984@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.)