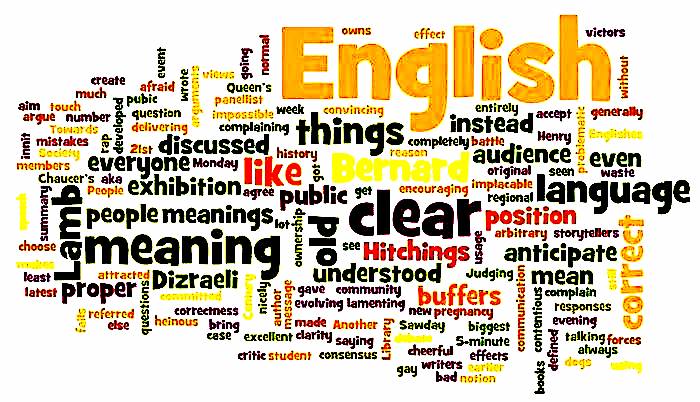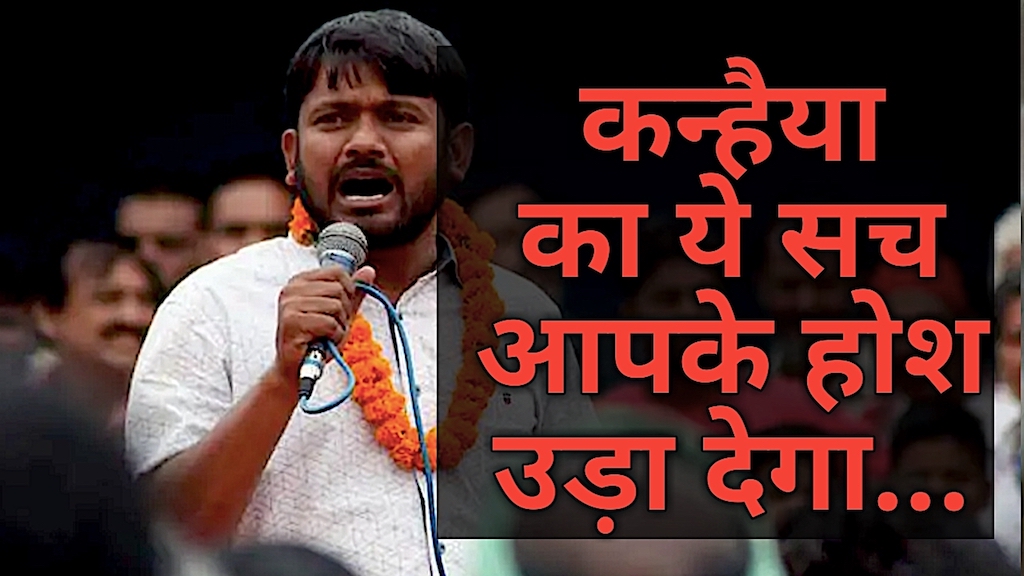By Kalim Azeem
मई 2017 में इरफ़ान खान स्टारर फ़िल्म ‘हिंदी मीडियम’ काफ़ी चर्चा में रही थी. सही मायनों में इस फ़िल्म का नाम ‘इंग्लिश मीडियम’ होना चाहिए था, क्योंकि ये फ़िल्म बच्चों के अभिभावकों की अंग्रेज़ी मानसिकता को दर्शाती है.
बीते कुछ सालों से अंग्रेज़ी माध्यम के पढ़ाई को लेकर अभिभावक परेशान नज़र आ रहे हैं. इंग्लिश मीडियम के इस टैबू को उपरोक्त फ़िल्म के माध्यम से तोड़ने का काम किया गया था.
फ़िल्म में ‘राईट टू एजूकेशन’ के साथ अमीरों का खिलवाड़ दर्शाया गया है. ये एक संजीदा फ़िल्म थी. जिसकी विषयवस्तु को काफ़ी सराहा गया. सरकार की राईट टू एजूकेशन पॉलिसी गरीब तथा आर्थिक कमज़ोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं. पर इस कोटे में अमीरों ने पैसे के दम पर सेंध लगाई है. जो गरीबी का चोला पहनकर गरीबों के शिक्षा के अधिकार को खा जाती है. दूसरी ओर गरीब तथा जहां अंग्रेज़ी शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, वहां के इंग्लिश मीडियम के टैबू को लेकर उस फ़िल्म में चर्चा की गई है.
फ़िल्म में एक पात्र ऐसा है, जो दिहाड़ी मज़दूरी करता है. वो अपने बच्चों का दाख़िला अंग्रेज़ी स्कूल में कराना चाहता है. बच्चे के माता-पिता दिन भर मज़दूरी करते हैं. यह परिवार एक ऐसे बस्ती में रहता है, जहां के सारे बच्चे सरकारी हिन्दी मीडियम स्कूल में जाते हैं. पर उस आदमी को लगता है कि उसका बच्चा अमीरों के साथ अच्छे और बढ़िया स्कूल में हो. वहां अच्छी शिक्षा हासिल करे.
यक़ीनन अच्छी शिक्षा का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है. अच्छी शिक्षा उसका अधिकार भी है. सरकार की इस पर पॉलिसी भी है, जो यह चाहती है कि ऐसे परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान हो.
अंग्रेज़ी को लेकर ग़लत धारणा
हमारे समाज में यह धारणा बनी है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा मिली तो उनका आर्थिक विकास होगा. उन्हें अच्छी और फ़र्राटेदार अंग्रेज़ी बोलनी आ जाएगी, जिससे उसे बड़ी नौकरी मिलेगी. कुछ लोगों को यह बहुत आसान नज़र आता है. इसलिए अंग्रेज़ी मीडियम और महंगे स्कूलों की होड़ में माता-पिता बिना सोचे-समझे शामिल हो जाते हैं. मानो इन स्कूलों में दाख़िला होते ही उनके बच्चे बड़े आदमी बन जाएंगे. माता-पिता इसके लिए किसी भी हद तक जाने को राज़ी हो जाते हैं.
पर हालात इसके बिल्कुल विपरित हैं. यह बात सही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए. पर उसके लिए शैक्षिक हैसियत से ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है. लोगों को ये विचार विवादित लग सकता है, पर असल मायने में अच्छी शिक्षा के बारे में उस घर में मौजूद शैक्षिक माहौल और उसकी दशा के बारे में सोचते नहीं हैं.
मेरा यह विचार एक अलग दायरे में आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है. जिस घर में उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं, वहां बच्चों के लिए अंग्रेज़ी स्कूल तथा प्री-एजूकेशन स्कूल फ़ायदेमंद साबित होते हैं. बच्चा स्कूल से घर आते ही वह लोग बच्चे का होमवर्क सही से ले सकते हैं. उसके नोट्स पढ़कर स्कूल से दी गई सूचनाओं को फॉलो कर सकते हैं. उसके स्टडी को आगे ले जाने वाले संवाद उसके साथ कर सकते हैं. इंटरनेट की मदद से उस स्कूली शिक्षा को गति देने वाला सिलेबस बच्चे को लेकर सिखा सकते हैं. मुलत: घर के अंग्रेज़ी वातावरण का बहुत बड़ा फ़ायदा उस बच्चे की शिक्षा को होगा.
इसके उलट एक सामान्य मध्य वर्ग घर का वातावरण अलग होता हैं. जहां बच्चे स्कूल से टूटी-फूटी अंग्रेज़ी के वर्ण सीखकर या रटकर घर आते हैं. रोज़ाना स्कूल के कुछ घंटों के भीतर वह बच्चा ठीक से अंग्रेज़ी सीख नहीं पाता. उसे घर पर और ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता होती है. पर घर के बड़े किसी हिन्दी मीडियम तथा सामान्य स्कूल में पढ़े होते हैं. उस बच्चे की शिक्षा को बेहतर ढंग से बढ़ाने के लिए उनका सहयोग कम मिलता है. अभिभावक सुबह-सुबह उठकर काम पर या दिहाड़ी मज़दूरी के लिए चले जाते हैं और शाम को लौटकर सो जाते हैं. बच्चे के होमवर्क लेने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं होता. घर की कामकाजी महिला हो या उस बच्चे की मां बच्चे को समय नहीं दे पाती. उसी तरह बच्चे के किताबों में गढ़े सिलेबस अभिभावक तथा बड़ों के समझ से परे होते हैं. फिर सवाल यह पैदा होता है कि वहां उस महंगी वाली अंग्रेज़ी शिक्षा का क्या फ़ायदा? क्योंकि न तो उस घर में कोई अंग्रेज़ी जानता हैं, न बोलता है. तो फिर बच्चे किसे देखकर, सुनकर अंग्रेज़ी शिक्षा को आगे लेकर जाएंगे. जिस घर में दो वक़्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है. वहां पर भी बच्चों के अच्छी शिक्षा को लेकर सजगता पाई जाती हैं.
इंग्लिश मीडियम का टैबू
दूसरी और मध्यवर्ग में अंग्रेज़ी शिक्षा का टैबू अपने चरम पर होता है. आर्थिक स्थिती ना होने के बावजूद माता-पिता मॉन्टेसरी तथा प्री-स्कूल एजूकेशन की महंगी फ़ीस भरते हैं. जब तक फीस भरना मुमकिन होता है, बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है. पर जब प्री-स्कूल का एजूकेशन ख़त्म हो जाता है, तो अभिभावक के पास प्रथम कक्षा के लिए अच्छा स्कूल तथा उस स्कूल की महंगी फ़ीस भरना नामुमकीन हो जाता है.
एक तो ऐसे अंग्रेज़ी स्कूल शहर से बाहर होते हैं, या फिर घर से बहुत दूर, जहां पहुंचने के लिए बच्चों को स्कूल बस का सहारा लेना पड़ता है. उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है. पर्यायस्वरुप अगर ऑटो या किसी निजी बस का सहारा लिया तो उस खर्चे का निर्वाहन करना अभिभावकों के लिए मुश्किल बन जाता है. ऐसे में एक तो बच्चे की पढ़ाई लटक जाती है, या फिर उसे सामान्य स्कूल में भेज दिया जाता है.
मानसिकता बदलने की ज़रूरत
नन्हें बच्चों की मानसिकता को बग़ैर सोचे-समझे हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं. इसी तरह एक और बड़ी समस्या को हम अनदेखा करते हैं. हर अंग्रेज़ी मीडियम के प्री-स्कूल एजूकेशन का सिलेबस अलग-अलग है. उनकी किताबें, नोटबुक सभी एक दूसरे से भिन्न हैं. हर स्कूल का अपना सिलेबस होता है. कहीं ए फॉर एप्पल तो कहीं ए फॉर एअरोप्लेन होता है. कहीं बी फॉर बॉल तो कहीं बैट होता है. ऐसे में एक घर के दो बच्चे जब साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वहां उन दोनों बच्चों का तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है.
मेरा भतीजा अदीब और भांजा सुफ़ियान दो अलग-अगल स्कूल में पढ़ते हैं. उन दोनों में मैंने कई बार ऊपर उल्लेखित शब्दों को लेकर असामंजस्य की स्थिती बनते देखा है. वही हमारे बिटिया सबीन के लिए हमने मार्केट के कुछ अल्फाबेट चार्ट खरीदे हैं. जहां ए फॉर अँण्ट तो बी फॉर बैलून, सी फॉर कप, डी फॉर डायनोसॉर. इस तरह के अल्फाबेट हैं. सबीन इन शब्दों को रटती है. पर जब अदीब और सुफ़ियान मिलते हैं तो सबीन चकरा जाती है. क्योंकि दोनों के शब्दों और उसके मिनिंग में बड़ा अंतर है. यह स्थिती बच्चों में बेहतर तालमेल नहीं बैठाती. जिससे उनका नन्हा सा दिमाग़ बी फॉर बॉल मानने को इनकार करता है.
बेहतर होता कि प्री-स्कूल एजूकेशन का हर सिलेबस एक जैसा हो. सरकार ने उन्हें स्कूल स्थापित करने की मान्यता दे दी. साथ ही अपना-अपना सिलेबस रखने की सुविधा प्रदान की, पर कहीं पर भी एक जैसा सिलेबस नहीं है. जहां नन्हें बच्चों के मानसिक अवस्था को लेकर संसोधन कर सिलेबस डिज़ाइन किया गया हो. उसे हर स्कूल में मान्यता मिले, ऐसा नहीं होता. सिलेबस की निर्माण प्रक्रिया में मोनोपॉली पाई जाती है. जिसका विपरित असर बच्चों के मानसिकता पर होता हैं.
तो फिर क्या किया जाए?
सरकार को चाहिए कि हर सिलेबस को एक जैसा बनाए. जिससे सभी बच्चे एक जैसी शिक्षा ग्रहण कर सकें. उनका आपस में तालमेल बैठ सके. अंकों में जिस तरह की समानता है, उसी तरह अन्य सिलेबस में भी होनी चाहिए.
सबसे बड़ी बात कहूं तो अंग्रेज़ी मीडियम के टैबू से बाहर आने की ज़रूरत है. माना कि अंग्रेज़ी व्यावसायिक भाषा है. पर उसका इतना अतिरेक सही नहीं है. हमारे माता-पिता ने हिन्दी तथा सामान्य स्कूलों से शिक्षा अर्जित कर नौकरी पाई है. उन्हें उसी शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान हुए हैं. तो अंग्रेज़ी शिक्षा की डिमांड सही नहीं है. रही बात अच्छी नौकरी की तो वह अब ना तो हिन्दी मीडियम में है ना तो अंग्रेज़ी मीडियम में. हाँ, यह बात है कि अंग्रेज़ी की डिमांड ज़्यादा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषा को कम महत्व दें.
हिन्दी मीडियम में भी अच्छा रोज़गार देने वाली पढ़ाई हो सकती है. साथ ही अंग्रेज़ी को प्रथम दर्जा देना उचित नहीं है. चीन जैसे राष्ट्र ने अपनी भाषा को बढ़ावा दिया है. अंग्रेज़ी भाषा का टैबू वहां नहीं है. चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने दुनिया को अपने पैरों पर ला खड़ा किया है. यही वजह है कि दुनिया के हर हिस्से में चीनी भाषा सीखने की होड़ लगी रहती है. क्योंकि वहां लोग जहां कहीं भी जाएं चायनीज़ में ही बात करते हैं.
(लेखक पुणे में ‘सत्याग्रही विचारधारा’ पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं.)