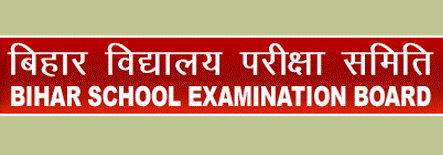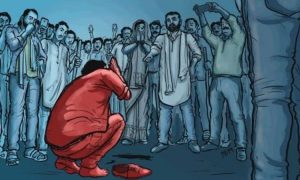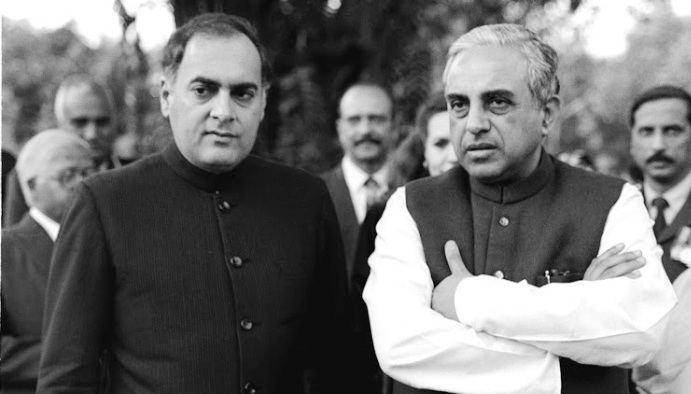Yogesh Garg for BeyondHeadlines
2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अरविन्द केजरीवाल की अगुवाई में एक नये राजनैतिक दल का खाका पेश किया गया. पार्टी के नाम की घोषणा बाद में होगी. संभवत इसका नाम भी ‘स्वराज’ शब्द से जुड़ा हो. लेकिन स्वराज पार्टी का नाम इतिहास से आता है. और इतिहास में भी व्यवस्था परिवर्तन के लिये लगभग इसी तरह के राजनैतिक विकल्प का प्रयोग हुआ था. लेकिन वो स्थायी न रह सका. कुछ वर्षो में स्वराज दल की क्रान्ति की मशाल ठण्डी पड़ गई.
आइये इतिहास में डुबकी लगाकर देखते हैं कि राजनैतिक विकल्प (स्वराज पार्टी) का परीक्षण क्यों असफल रहा.
वर्तमान में अरविन्द केजरीवाल और उनके साथियों द्वारा बनाये जा रहे राजनैतिक दल में क्या-क्या समानताएं हो सकती हैं. और क्या अरविन्द केजरीवाल इतिहास से कुछ सीखना चाहेंगे?
अगर आप इतिहास देखें तो पायेंगे कि राजनैतिक विकल्प(पार्टी) के द्वारा व्यवस्था में सुधार का प्रयोग सर्वप्रथम 1923 में स्वराज पार्टी के गठन से हुआ था. इस पार्टी के मुख्य नेता मोतीलाल नेहरू और चिरंजन दास थे. अन्य नेताओं में चितामन केलकर, सुभाष बाबू और विट्ठल भाई पटेल थे.
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ़ एक लंबा संघर्ष था. आजादी की यह लड़ाई अलग-अलग समय में अपने ढंग से लड़ी गई थी. इस लंबी लड़ाई में ‘स्वराजवाद’ का उदय राजनीतिक परीक्षण के तौर पर हुआ था.
‘स्वराजवाद’ से मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ऐसे रूझान से है जिसने कौंसिल प्रवेश की राष्ट्रीय आन्दोलन के एक हिस्से के रूप में वकालत की. इनका मानना था कि कांग्रेस को चुनाव लड़कर कौंसिल में जाना चाहिये और शासन की गलत नीतियों का राजनैतिक तरीके से विरोध करना चाहिये. जबकि महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस लेने के साथ ही कांग्रेस को कौंसिल में जाने से रोक दिया. वो सिर्फ कांग्रेस को जनजागरण और सामाजिक आन्दोलनों से राष्ट्रवाद के उदय का साधन मानते थे. स्वराज पार्टी का उदय का कारण कांग्रेस में फूट थी. असहयोग आन्दोलन वापस लेने से गुस्साये नेताओं की प्रतिक्रिया थी. इनका मानना था कि जब तक सत्ता का हिस्सा नहीं बनते तब तक सुधार संभव नहीं है. जिसके सम्बन्ध में महात्मा गांधी का ये मानना था कि राष्ट्रवादी नेताओं के मतभेद और फूट से निश्चित ही ब्रिटिश शासन को लाभ होगा.
1920 कांग्रेस के कलकता अधिवेशन में ये कांग्रेस द्वारा किये गये चुनावो के बहिष्कार का निर्णय असफल रहा था. कांग्रेस द्वारा छोड़ी गई सीटों पर अवांछनीय तत्वों का अधिकार हो गया था.
स्वराज पार्टी के गठन के हिमायती राष्ट्रवादी नेताओं को कहने का मौका मिला कि सत्ता प्रतिनिधित्व छोड़ देने से लाभ बाहरी शत्रु को ही ज्यादा होगा. गलत लोग चुने जायेंगे उससे नुक़सान तो राष्ट्र का ही होगा.
इसके बाद गया अधिवेशन मे स्वराजवादियों के राजनैतिक सुधार पक्ष मे 890 मत थे और विरोध मे रुढिवादी कांग्रेसियों के 1740 मत थे. तब से रुढिवादी कांग्रेसियो को ‘परिवर्तन विरोधी’ और स्वराज पार्टी वालो को ‘परिवर्तन समर्थक’ की पहचान मिली. लेकिन गांधीजी ने भी माना कि एक सशक्त मत की अवहेलना करना राजनीति में प्रवेश के पक्षधर स्वराज-वादियो ने कौंसिलो में प्रवेश कर अंग्रेजी द्वैध शासन का विरोध किया. कुशासन को बेनकाब किया. मध्य प्रान्त और बंगाल में चुनावों में सफलता प्राप्त की. वहीं कांग्रेस खादी आन्दोलन और स्वदेशी आन्दोलन से जुड़ी रही. हालांकि गांधीजी ने व्यक्तिगत रुप से कांग्रेस के नेताओ को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी, लेकिन सत्ता का हिस्सा बनना उन्हें मंजूर नहीं था. उन्हें इस बात पर भी आपत्ति थी कि स्वराज पार्टी वाले खादी और चरखे को चुनाव प्रचार का हिस्सा ना बनाये.
1924 के बेलगाम अधिवेशन मे गांधीजी (कांग्रेस) और स्वराज पार्टी वाले मोतीलाल नेहरू और चिरंजन दास के बीच समझौता हो गया. यह तय हुआ कि गांधीजी और उनके अनुयायी रचनात्मक एवं सामाजिक आन्दोलन, खादी आन्दोलन चलायेंगे और स्वराज पार्टी वाले राजनैतिक पार्टी का जिम्मा लेंगे.
इस पार्टी का जीवन काल संक्षिप्त रहा. क्योंकि ये कांग्रेस से फूट और अंसतोष से जन्मी थी. इनका मुख्य लक्ष्य कौंसिल में ब्रिटिश सरकार की जन विरोध की नीतियों का विरोध करना था. इनके पास शासन की कोई स्पष्ट नीति लक्ष्य उद्देश्य व कार्ययोजना व संविधान नहीं था. राष्ट्रीय मुद्दो पर इनकी समझ न के बराबर थी. और ना ही ये रचनात्मक कार्यो के द्वारा जनता को उद्देलित कर पाये. इनके पास केन्द्रीय सत्ता शक्ति को प्रभावित करने लायक सामर्थ्य नहीं था. और न ही अधिकार थे. सरकार इनकी सुनती नहीं थी तो इनके पास इस्तीफे देकर दबाव का ही विकल्प था. जिससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था. केवल असंतोष और विरोध के दम पर पार्टी का अस्तित्व बचाये रखना कठिन होता जा रहा था.
इस पार्टी के खत्म होने का कारण दूसरा यह भी था कि इस खेमे में उदारवादी लोग भी थे, जो ब्रिटिश शासन का विरोध करना उचित नहीं मानते थे. उन्हें लगता था कि अंग्रेजी सरकार का तीक्ष्ण विरोध करने के बजाय अपने मांगे मनवाने के लिये सहयोगी रवैया अपनाया जाये. इस मुद्दे पर स्वराज पार्टी भी दो खेमे मे बंट गई. खुलेआम मतभेद तब नज़र आये, जब वीएस तांबे जो मध्य प्रान्त विधायिका के स्वराजी अध्यक्ष थे. उन्होने ब्रिटिश शासन की कार्यकारी परिषद की सदस्यता ग्रहण कर ली. स्वराज पार्टी विभाजन और फूट से पथभ्रष्ट होती जा रही थी.
एक अन्य कारण यह भी था कि कुछ स्वराज पार्टी वादी राष्ट्रीय नेता चुनाव लड़कर मिलने वाले पद और सुविधाओ के लोभ में फंस गये. अनुक्रियावादी हो गये थे. सरकार के साथ अनुक्रिया वादी सहयोग के सिद्धान्त का इन्होंने प्रतिपादन किया.
इस पार्टी के पतन का एक अन्य कारण ये भी था कि पार्टी शुरु से ही मोतीलाल नेहरु और चिंतरजन दास पर ही केन्द्रित रही. स्वराज पार्टी के पर्याय एक चेहरा बना रहा और एक मात्र ‘ थिक टैंक’ चिंतरजन दास ही थे. उनकी जून 1925 में मृत्यु के बाद पार्टी का कोई “धणी धोरी” नहीं रहा.
जिन राष्ट्रवादी नेताओं को चिंतरजन दास ने स्वराज पार्टी के लिये संगठित किया था वे अब बेलगाम हो गये थे. नेतृत्व का अभाव हो गया था क्यों पार्टी सिर्फ एक दिमाग से चल रही थी. पार्टी के लिये कोई स्पष्ट संविधान नहीं बनाया गया था. जिससे मुख्य नेता की अनुपस्थिति में पार्टी की नीतियां और कार्य-योजना तय की जा सके.
व्यक्तिवादी पार्टी छवि के चले जाने के बाद लोगों का स्वराज पार्टी से मोहभंग हो गया. अन्य नेताओं व मोतीलाल नेहरु में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो पार्टी चला पाते.
8 मार्च 1926 को स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरु केन्द्रीय असेम्बली से बाहर ले आये. वे दिखाना चाहते थे स्वराज पार्टी वाले साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार से कोई संबध नहीं रखते हैं, जो जन समान्य की स्वराज की इच्छा के प्रति कोई सम्मान नहीं रखती है.
इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन एक संक्षिप्त किन्तु महत्वपूर्ण अध्याय स्वराज पार्टी के केन्द्रीय असेम्बली छोड़ने के साथ ही समाप्त हो गया. ये ऐसा अध्याय था जिसमें पहली बार व्यवस्था परिवर्तन के लिये राजनैतिक विकल्प आजमाया गया. उपर्युक्त कारणों से यह स्थायी नहीं रह सका.
हालांकि पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ था. परन्तु इस विचार (पार्टी) की शक्ति क्षीण होकर मृतप्राय हो चुकी थी. 1930 मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समर्थन करते हुये स्वराज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़े. और 1934 मे मद्रास असेम्बली में बहुमत ना आने पर इस विकल्प (पार्टी) का अस्तित्व नगण्य हो गया.
इतिहास खुद को दोहराता है. और सीखने के दो तरीके होते हैं. या तो हम खुद गलती करके सीखें या इतिहास में जो गलतियां और लोगों ने की है उन्हें ना दोहराये.
राजनैतिक विकल्प द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के प्रयोग अब तक 3 बार हुये हैं. जिनमें दो बार असफलता मिली है. एक महाप्रयोग 1951 का लोकसभा चुनाव था जब अधिकतर राष्ट्रवादी राजनीति में आये, लेकिन उसके लिये उनके पास पर्याप्त अनुभव था और स्पष्ट नीति थी. कार्ययोजना और संविधान था. तीसरा प्रयोग 1977 में जेपी आन्दोलन के बाद हुआ. ये असफल रहा…
हमें इतिहास से सीखना चाहिये. नहीं तो हम भी वही गलती करेंगे जो पहले दो बार हो चुकी है.