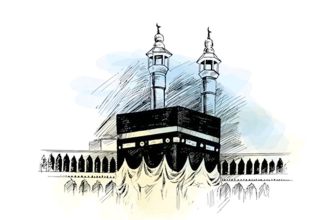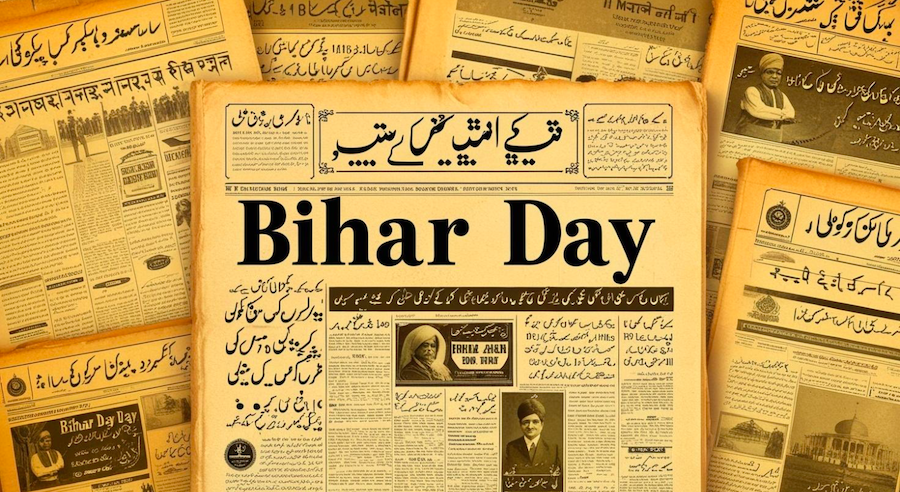Amit Tyagi for BeyondHeadlines
मेरा मानना है कि मानवाधिकार चर्चा का नहीं आचरण का विषय है. सारी चर्चाएँ और बहस सिर्फ मानवाधिकार को समझने का प्रयास तो हो सकती हैं किन्तु जरूरतमंदों को फ़ायदा पहुँचाती हुई नहीं दिखती है. पूंजीवादी व्यवस्था मे सामंतवादी सोच मानवाधिकार का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होती है. स्वयं के पास आवश्यकता से कुछ भी अधिक होना किसी अन्य के मानवाधिकार का हनन ही माना जाएगा. मानवाधिकार का सबसे ज़्यादा ढ़ोल पीटने वाले विकसित देश ही गरीब देशों की प्राकृतिक सम्पदा पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं. महात्मा गांधी का भी कहना है… “ पूंजी अपने–आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है. किसी ना किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता तो हमेशा रहेगी…” वास्तव मे मानव अधिकार एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता, निवास, लिंग, या जातीय मूल, रंग, धर्म या अन्य स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकार हैं.
आज दुनिया में सिर्फ स्वयं को बेहतर दिखने और वर्चस्व की जंग मची हुई है. धन बल के द्वारा एक इंसान दुसरे इंसान पर विजय पाने को अमादा है. कभी-कभी तो हालात इतने ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं कि यदि इंसान पर कोई कानूनी नियंत्रण ना हो तो वह स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति को मारने को तैयार है. छोटी छोटी बात पर लोगों का आक्रामक हो जाना और जगह जगह हो रही हिंसा इस बात का सबूत है कि शायद मानवता ही आज खतरे में है. अगर आज दुनिया में अमीरों और ताकतवरों के बीच आम जनता सुरक्षित ढंग से रह पाती है तो उसकी वजह है सबको मिलने वाला “तथाकथित मानवाधिकार”.
यूं तो मानवाधिकार सबके लिए समान होता है लेकिन वास्तव मे इसका फायदा उसे ही मिल पाता है जिसे या तो इसकी जानकारी हो या कोई संसाधन.
विश्व में मानवाधिकार के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस की शुरुआत की थी. 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा स्वीकार की थी. 1950 से महासभा ने सभी देशों को इसकी शुरुआत के लिए आमंत्रित किया था. संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए तय किया. लेकिन हमारे देश में मानवाधिकार कानून को अमल में लाने के लिए काफी लंबा समय लग गया. भारत में 26 सिंतबर, 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में लाया गया है. अगर भारत में मानवाधिकारों की बात की जाए तो यह साफ है कि मानवाधिकार व्यक्ति की हैसियत देखकर ही मिलता है. यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जहां साक्षरता का स्तर अपेक्षाकृत थोड़ा कम है वहां मानवाधिकारों का हनन आम बात है. कुछ स्थानों पर कई बार बेकसूरों को पुलिस और प्रशासन के लोग सिर्फ अपना गुस्सा शांत करने के लिए बेरहमी से मार देते हैं और फिर झूठा केस लगा उन्हें फंसा देते हैं. लेकिन इसके विपरीत शहरों में जहां लोग साक्षर हैं वहां पढे लिखे लोग मानव के अधिकारों का गलत प्रयोग अपनि गलतियों के बचाव के लिए भी करते हैं. स्वयं को प्रगतिशीलता का ठेकेदार मानने वाले और अङ्ग्रेज़ी मानसिकता का चोला ओढ़े एक खास किस्म का युवा वर्ग मानवाधिकार के नाम पर जब पार्क, गार्डन और गलियों आदि में अश्लीलता फैलाते दिखते हैं तब मानवअधिकारों कि परिभाषा ही बदलती दिखने लगती है. इसी क्रम में जब मानवाधिकार के जानकार लोग जब अपराधियों के मानवाधिकार हनन कि बातें करते हैं तो बहुत कष्ट होता है. जहां तक अपराधियों की बात है एक बलात्कारी, आतंकवादी या हत्यारे को सिर्फ मानवाधिकार के नाम पर सुविधाएं दिलवाना और तंत्र को सुधारने के लिए काम कर रहे लोगों का मनोबल तोड़ने का कृत्य गलत है. अब अगर अपने अंजाम तक पहुंचे कसाब जैसे किसी आतंकवादी के मानवाधिकार के लिए पैरवी कोई भी करेगा तो उन लोगों को कितना कष्ट होगा जिनके स्वजन उस आतंकवादी के साथियों के द्वारा शहीद हुए हैं. अबु सलेम, अफजल गुरू जैसे हत्यारे और आतंकियों के मानवाधिकार की बात की जाती है तो यह निरर्थक लगती है. यहां विरोधाभास तो है पर मानव का हित साधना ही परम उद्देश्य लगता है. लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि इन्हीं अपराधियों के साये में जब कोई निर्दोष हत्थे चढ़ जाता है और प्रशासन सच उगलवाने के लिए गैरकानूनी रूप से किसी को शारीरिक या मानसिक यातना देता है तब समझ में आता है मानवाधिकार कितना जरूरी है. इसलिए मैंने प्रारम्भ मे ही अपनी बात काही थी कि मानवाधिकार चर्चा का नहीं आचरण का विषय है.
भारत कि न्यायपालिका ने भी लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए समय समय पर दिशा निर्देश दिये हैं उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बंधुआ श्रम का उन्मूलन , रांची, आगरा एवं ग्वालियर के मानसिक अस्पतालों का कामकाज , शासकीय महिला सुरक्षा गृह, आगरा का कामकाज , भोजन का अधिकार जैसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. सामाजिक कुरीतियों और लोगों को उनके मानव अधिकारों को दिलवाने मे मानवाधिकार आयोग के प्रयास भी सरहनीय तो हैं किन्तु ऊंट के मुंह मे ज़ीरा के समान हैं. आयोग के प्रमुख प्रयासों मे बाल विवाह निषेध अधिनियम की समीक्षा, 1929 ,बाल अधिकार प्रोटोकॉल के लिए कन्वेंशन ,सरकारी कर्मचारियों द्वारा करवाए जाने वाले बालश्रम की रोकथाम, ,बाल श्रम उन्मूलन ,बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए गाइडबुक, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार: लिंग संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका मैनुअल , सेक्स पर्यटन और तस्करी की रोकथाम पर संवेदनशील कार्यक्रम, मातृ रक्ताल्पता और मानव अधिकार, वृन्दावन में बेसहारा औरतों का पुनर्वास, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकना, रेल में महिला यात्रियों का उत्पीड़न रोकना, सफाई उन्मूलन पुस्तिका, दलित मुद्दों विशेषकार उन पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम, डिनोटिफाइड और खानाबदोश जनजातियों की समस्याएं, विकलांगों के लिए अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, एचआईवी/एड्स, 1999 के उड़ीसा चक्रवात पीड़ितों के लिए राहत कार्य , 2001 के गुजरात भूकंप के बाद राहत उपायों की निगरानी, जिला शिकायत प्राधिकरण, प्रमुख रूप से सरहनीय हैं. मानवाधिकार आयोग के ये कार्य तो सराहनीय है किन्तु जनता की अपेक्षाएँ इससे बहुत ज़्यादा है. और शायद जितना हम और मानवाधिकार से जुड़े संघठन इस बात को आत्मसात करते चले जाएंगे कि मानवाधिकार चर्चा का नहीं आचरण का विषय है लोगों तक इसके फायदे पहुंचने शुरू हो जाएंगे.