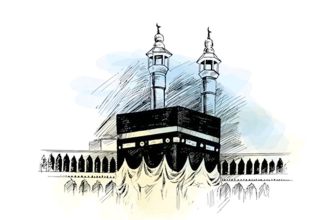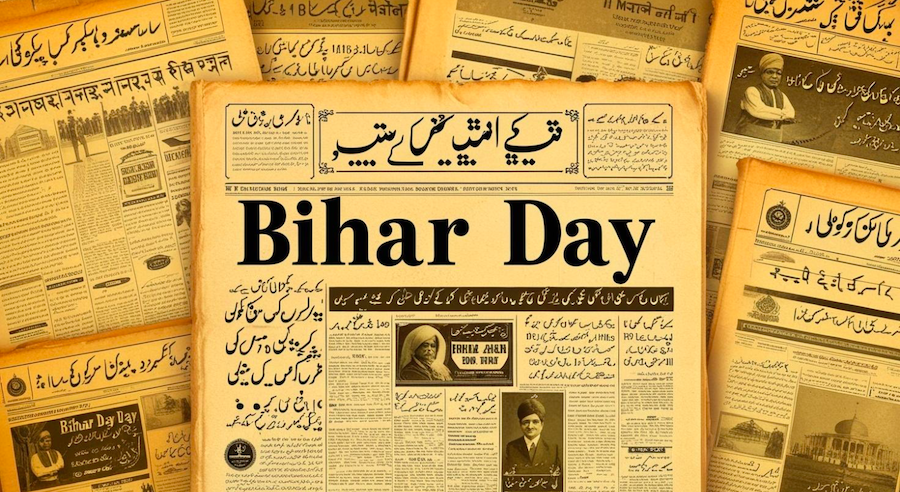Anurag Bakshi for BeyondHeadlines
13 मई, 2013 को भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के 61 वर्ष पूरे हो गए हैं. संसदीय व्यवस्था के इन छह दशकों में निस्संदेह ढेरों उपलब्धियां रही हैं. जनसरोकार से जुड़े काफी विधेयकों ने गंभीर चर्चा के बाद कानून की शक्ल ली है.
सत्ता का हस्तांतरण हमेशा वोट से हुआ है. यहां एक वोट से भले सरकार गिर जाए, लेकिन पड़ोसी मुल्कों की तरह हिंसक संघर्ष नहीं दिखा. देर रात तक चली सदन की बैठकें, बाहरी संकटों पर संसद की एकजुटता, हर तबके की हिस्सेदारी और दोषी पाए जाने पर स्वयं सांसदों के खिलाफ कार्रवाई ने संसद का मान बढ़ाया है. जाहिर है यही सब हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती रही हैं.
लेकिन आपातकाल हो या फिर सांसदों की खरीद-फरोख्त, सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का मामला या फिर संसदीय समितियों पर उठते सवाल, ऐसे कई प्रश्न भी सफर के इस पड़ाव पर गंभीर चिंतन के लिए मजबूर करते हैं.
1962 तक देश में एकल सदस्यीय एवं बहुसदस्यीय दोनों तरह के निर्वाचन क्षेत्र होते थे लिहाजा 401 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 489 सीटों के लिए करीब चार महीने तक चले चुनाव में कुल 17 करोड़ 32 लाख मतदाताओं में से करीब 46 फीसदी ने अपनी चुनावी ताकत का इस्तेमाल किया तबसे लेकर अब तक लोकसभा की तस्वीर काफी बदल चुकी है. उद्धाहरण के तौर पर अब कुल निर्वाचित सीटें बढ़कर 543 हो चुकी हैं. देश में अब 71 करोड़ से अधिक मतदाता हैं. जाहिर है बढ़ती आबादी के बीच चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अपेक्षाओं का दबाव बढ़ा है. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पिछले कुछ दशकों से हमारे माननीय जनअपेक्षाओं पर खरा उतर पा रहे हैं? क्या संसद अपनी सार्थकता सिद्ध कर पा रही है? बीते 61 वर्ष में लोकसभा की बैठकों में आती साल दर साल की कमी निराश करती है.
पहली लोक सभा में कुल 677 दिन तक सत्र चला था, जबकि मौजूदा 15वीं लोकसभा के चार सालों में अब तक कुल 314 बैठकें ही हो सकी हैं. 15वीं लोकसभा, अपने बजट सत्र, यानी 13वें सत्र तक, कुल 1252 घंटे बैठी है, जो पहली लोकसभा की कुल बैठकों के मुकाबले आधी से भी कम हैं.
दुर्भाग्य से संसद बाधित करने में कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता. आज निचले सदन में नुमाइंदगी करने वाले 38 राजनीतिक दल हैं. लेकिन फिर भी लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में चलती बड़े दलों की ही है. तीन-चार बड़े राजनीतिक दल ही ज्यादातर व्यवधान के दोषी हैं.
समय-समय पर विधायिका की तस्वीर सुधारने पर होने वाले सम्मेलनों में हर दल चिंता जाहिर करता रहा. हर बार लगता मानो संसदीय मोर्चे पर अब सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका. शायद यही वजह रही कि राजनीति से युवाओं का मोहभंग होता गया.
पहली लोकसभा में 35 वर्ष से कम उम्र के सांसदों की संख्या 82 थी जबकि मौजूदा 15वीं लोकसभा में केवल 37 ही युवा सांसद हैं. पिछले 61 सालों में 25-30 वर्ष के केवल 192 सांसद ही चुने गए हैं. यानी मात्र 2.5 फीसदी!
जिस देश की करीब 65 फीसदी आबादी 35 साल से कम हैं. वहां लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या लगातार घट रही है. देश की आधी आबादी महिलाओं की संसद में हिस्सेदारी भी 11 फीसदी तक ही सीमित है. वैसे राजनीतिक आपराधिकरण और चुनाव सुधारों की भारी कमी भी इस राजनीतिक उदासीनता की बड़ी वजह है.
आंकड़े बता रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग धनबल और बाहुबल के दम पर सांसद बनने की दौड़ में आगे हैं. संसद में जिस तरह विचार-विमर्श की बजाय हंगामा ज्यादा होने लगा है. इसके लिए कुछ प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं:
पहला: कार्यपालिका द्वारा संसद के उपेक्षा की बढ़ती प्रवृत्ति
नेहरू युग में जहां प्रधानमंत्री संसद में होने वाली बहसों को पूरी गंभीरता से लेते थे. वहीं इंदिरा गांधी का दौर आते-आते कार्यपालिका विधायिका पर हावी होने लगी. अभी भी संसद में होने वाले हंगामे का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार संसद को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है.
दूसरा : विपक्ष में भी बहस द्वारा सरकार को घेरने की प्रवृत्ति कम हुई है
मसलन, विपक्ष में अब ऐसे बहुत कम नेता हैं, जो डॉ राममनोहर लोहिया या मधु दंडवते की तरह अपनी बहस और आंकड़ों द्वारा सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें. इसकी जगह संसद की कार्रवाई रोककर सरकार को झुकाने की कोशिश की जाती है.
तीसरा : यह भी सच है कि राजनीति के अपराधीकरण ने भी संसद के काम के स्तर को प्रभावित किया है. संसद में बहुत से अपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद भी हैं. ये लोकतंत्रीकरण और हाशिए के समूहों के उभार की बजाय राजनीति में पैसे और बंदूक के बढ़ते जोर के कारण संसद में पहुंचे हैं. संसद की कार्यवाही की गरिमा के अनुसार काम करने की बजाय ऐसे सांसद कई मर्तबा छोटी बातों पर भी जबर्दस्त हंगामा करते हैं.
संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि कार्यपालिका अहंकार से भरा व्यवहार करने की बजाय विपक्ष और संसद को पूरी गंभीरता से लें. विपक्ष के लिए भी यह आवश्यक है कि वे हर मुद्दे पर संसद ठप्प न करें. संसद में बहस द्वारा सरकार को घेरकर ज्यादा अच्छी तरह से उसका पर्दाफाश किया जा सकता है.
हमारे माननीयों की कथनी और करनी में अंतर साफ दिखता है. अलग-अलग मंचों पर राजनीतिक शुचिता, आचरण, नैतिकता और मर्यादा, जवाबदेही जैसी बातों की वकालत करने वाले राजनेता जब खुद इन पर अमल करते नहीं दिखते हैं तो आम जन का हृदय कचोटता है.
2012 में 13 मई को संसद के साठ साल पूरे होने के मौके पर आयोजित संसद के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके सांसदों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की गई थी, जिससे सदन की गरिमा को बनाए रखा जा सके. सत्र के दौरान हमारे प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने संसदीय परंपरा, मर्यादा और इसके गौरवशाली इतिहास पर काफी लंबे चौड़े बयान दिए थे.
चुनिंदा लोगों के बयानों पर एक नजर:
(1) संसद की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान उत्पन्न करने, स्थगन और शोर-शराबा से इस संस्थान को लेकर बाहर संदेह उत्पन्न होने लगा है. –मनमोहन सिंह.
(2) संसद की गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा हर की कीमत पर होनी चाहिए. इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है. लेकिन हमारा व्यवहार भी उच्च नैतिक मानदंडों से निर्धारित होना चाहिए. –सोनिया गांधी.
(3) संसद में गतिरोध खत्म करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. कुछ सदस्यों की वजह से पूरी कार्यवाही स्थगित होती है, विधेयक लटक जाते हैं. –प्रणब मुखर्जी.
(4) विभिन्न मतों को आदर देने से भारतीय लोकतंत्र सफलता का एक मुकाम हासिल कर सका है. अगर संसद सदस्य एक दूसरे के विचारों का आदर करें तो हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है. –लालकृष्ण आडवाणी.
(5) लोकतंत्र को और बेहतर करने के लिए हमें और ज्यादा लोकतांत्रिक होना पड़ेगा. संसद में महिलाओं को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए. –सुषमा स्वराज
(6) लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संसद की है. लेकिन संसदीय प्रणाली के ऊपर कोई नहीं हो सकता. लोकपाल के नाम पर हमारे ऊपर किसी को नहीं बिठाया जा सकता. –लालू प्रसाद यादव.
(7)अगर देश में 80 फीसद लोग गरीब और पिछड़े बने रहेंगे तो न लोकतंत्र और न ही संसद का विकास हो सकता है. –शरद यादव
(8) संसदीय प्रणाली को लेकर लोगों में बढ़ती निराशा गंभीर चिंता का कारण है. संसद को जनता की अपेक्षा पर खरा उतरना होगा. –अरुण जेटली
(9) यह ऐसा पड़ाव है जहां से पीछे मुड़कर भी देखा जाता है और आगे की ओर भी. यह हमारे आत्मावलोकन का समय है. आने वाली चुनौतियों के आकलन का समय है. –मीरा कुमार
(10) महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लेने का समय है यह. अभी भी किसानों में आत्महत्या और भुखमरी को दूर करना एक बड़ी समस्या है. –मुलायम सिंह यादव
यही नहीं, 1997 में संसद की 50वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर सदन में ‘भारत के लिए एजेंडा’ संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था. उसमें भी यही प्रतिबद्धता दिखाई गई थी कि ‘संसद की प्रतिष्ठा को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा. संसदीय प्रक्रियाओं का गौरवशाली तरीके से निर्वहन किया जाएगा. प्रश्नकाल में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी. सदन की कार्यवाही को बाधा पहुंचाने वाले नारों और अप्रिय क्रियाकलापों से बचा जाएगा.’
मुझे लगता है कि यह एजेंडा आर्काइव में ही सुरक्षित है. वर्तमान क्रियाकलापों से उसका कोई लेना देना नहीं है.