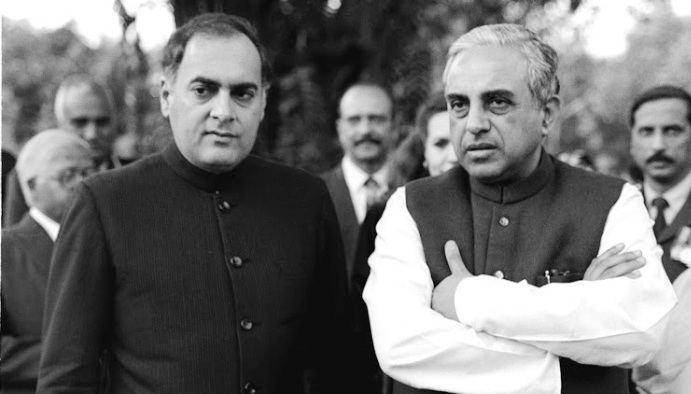Abubakr Sabbaq Subhani for BeyondHeadlines
देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध व वरिष्ठ न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा अय्यर ने पुलिस हिरासत में टॉर्चर को आतंकवाद से भी भयानक अपराध क़रार दिया था, क्योंकि टॉर्चर में हमेशा सरकार व पुलिस प्रशासन का अपना हित छिपा होता है. (द हिंदू, 27.07.2003).
हिरासत के दौरान टॉर्चर की शुरुआत कब हुई? इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं, लेकिन किसी भी राज्य की स्थापना के साथ ही ज़ुल्म व ज़्यादती का इतिहास शुरू हो जाता है. भारतीय इतिहास में ऐसे साक्ष्य विलुप्त हैं जो कभी भी किसी भी स्तर पर टार्चर का सरकारी स्तर पर विरोध करते नज़र आएं, बल्कि तथ्य यह है कि सरकार के नेतृत्व में ही यह आक्रामक रस्म परवान चढ़ती नज़र आती है.
 अंतरराष्ट्रीय नियम व क़ानून इस अमानवीय शोषण प्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध करते हैं और इसके उन्मूलन के लिए जहां तक मुमकिन हो, कोशिश करते नज़र आते हैं. 1948 में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार पर जारी घोषणा-पत्र (UDHR) का अनुच्छेद-5 एवं ICCPR के धारा-7 भी साफ शब्दों में घोषणा करती है कि “किसी भी व्यक्ति को टार्चर, दर्दनाक यातना, गैर इंसानी या अपमान भरा सलूक या सज़ा का शिकार नहीं बनाया जाएगा”, इसी भावना और बुनियादी स्वतंत्रता के दर्शन को फिर हमारे देश के लोकतांत्रिक संविधान में महत्व देते हुए संविधान की भूमिका तथा मूलभूत अधिकारों के अध्याय में शामिल किया गया. संविधान के अनुच्छेद-21 में प्रत्येक नागरिक के लिए मानव सम्मान यानी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने और शोषण से सुरक्षा का अधिकार स्वीकार किया गया. इस मूलभूत अधिकार की सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए इसके संरक्षण के लिए न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्रदान किए गए.
अंतरराष्ट्रीय नियम व क़ानून इस अमानवीय शोषण प्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध करते हैं और इसके उन्मूलन के लिए जहां तक मुमकिन हो, कोशिश करते नज़र आते हैं. 1948 में संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार पर जारी घोषणा-पत्र (UDHR) का अनुच्छेद-5 एवं ICCPR के धारा-7 भी साफ शब्दों में घोषणा करती है कि “किसी भी व्यक्ति को टार्चर, दर्दनाक यातना, गैर इंसानी या अपमान भरा सलूक या सज़ा का शिकार नहीं बनाया जाएगा”, इसी भावना और बुनियादी स्वतंत्रता के दर्शन को फिर हमारे देश के लोकतांत्रिक संविधान में महत्व देते हुए संविधान की भूमिका तथा मूलभूत अधिकारों के अध्याय में शामिल किया गया. संविधान के अनुच्छेद-21 में प्रत्येक नागरिक के लिए मानव सम्मान यानी स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने और शोषण से सुरक्षा का अधिकार स्वीकार किया गया. इस मूलभूत अधिकार की सुरक्षा को विशेष महत्व देते हुए इसके संरक्षण के लिए न्यायिक व्यवस्था बनाई गई, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्रदान किए गए.
इन सभी तथ्यों के बावजूद भारतीय संविधान या अन्य क़ानूनों में कहीं भी टॉर्चर की परिभाषा या इसकी मनाही का उल्लेख “टॉर्चर” शब्द के साथ नहीं है, बल्कि सामान्य प्रावधानों में हिरासत के दौरान मौत के मामले में इंडियन पिनल कोड की धारा-302 का ही संदर्भ लिया जाएगा.
संयुक्त राष्ट्र की जेनरल असम्बली ने 10 दिसम्बर, 1948 में टॉर्चर के परिपेक्ष्य में एक विश्वस्तरीय संधि UNCAT पास किया, जिसका मक़सद टॉर्चर को कानूनी ऐतबार से गैर-क़ानूनी बनाया जा सके. इस संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र से संबंधित देश अपने देश में टॉर्चर के समाप्ती हेतु ऐसे कानून लागू करें, जिनके ज़रिए टॉर्चर को ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया जा सके. यही नहीं, इस पर नज़र रखने के लिए एक “कमिटी अगैंस्ट टॉर्चर” का भी गठन किया गया. संधि की धारा-22 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत शिकायत भी इस कमिटी में कर सकता है.
हमारे देश भारत ने भी टॉर्चर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की इस संधि पर अक्टूबर 1997 में हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अपने देश में जो स्थिति है, इन सब से आप बखूबी वाकिफ हैं. यही नहीं, इसके अलावा अनुबंध की धारा-20 और 22 के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करके उससे क्षमा भी मांगी ली, यानी हमारी सरकार न तो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि इस देश में टॉर्चर के खिलाफ कोई कानून लागू करे और न ही यहां के किसी नागरिक को यह हैसियत हासिल है कि वह राज्य के ज़ुल्म व ज़्यादती के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की “कमिटी अगैंस्ट टॉर्चर” में शिकायत दर्ज कर सके.
इस संदिग्ध नियत व इरादे के साथ भारत सरकार ने 2008 में “काउंटर टॉर्चर बिल” संसद में पेश की, इस बिल के तहत अगर कोई सरकारी व्यक्ति या पुलिस अगर किसी को गंभीर चोट, जीवन के लिए खतरा, लिंग या स्वास्थ्य को नुक़सान, या किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक पीड़ा के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं तो वो सज़ा के हक़दार होंगे. बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि किसी जानकारी या इकबालिया बयान के लिए भी अगर टॉर्चर का इस्तेमाल होता है तो भी वह सजा के हक़दार होंगे.
यह बिल लोकसभा में बिना किसी बहस के पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में कुछ आपत्तियों के बाद फिर 2010 में संशोधित विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया, लेकिन आज तक न तो टॉर्चर को गैर कानूनी घोषित किया गया है और न ही इसे रोकने हेतु कोई गंभीर कोशिश की गई.
सन् 1993 में भारतीय संसद ने “मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम” लागू किया, उक्त अधिनियम की धारा-3 के तहत एक “राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग” का गठन अस्तित्व में आया. इस आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वो नागरिकों के मानव व नागरिक अधिकार की रक्षा करे. किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में मामले की जांच करे. जांच पूरी होने के बाद संबंधित अदालत या राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करे और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्रवाई करे. लेकिन अफसोस! भारत सरकार की दूसरे संस्थाओं की तरह इस आयोग का प्रदर्शन और ईमानदारी भी सवालों के कठगरे में है.
भारत में हिरासत के दौरान, चाहे वह हिरासत पुलिस की हो या अदालत की, टॉर्चर विशेषकर कमजोर लोगों के लिए एक गंभीर समस्या का रुख अख्तियार करता जा रहा है. यही टॉर्चर यानी ज़ुल्म व ज़्यादती जब अपनी सीमा पार कर जाती है तो और उस इंसान की जान तक ले लेती है, जिसे हम कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस हिरासत में मौत का नाम दे देते हैं.
हिरासत में मौतों की मौजूदा स्थिति और उसकी गंभीरता का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इन आंकड़ों को देखा जा सकता है, जिसके अनुसार पिछले दशक यानी 2001 से 2010 के दौरान हमारे देश में कुल 14231 मौत पुलिस हिरासत में हुई हैं, यानी प्रतिदिन हिरासत में होने वाली मौतों की दर 4.33 फीसदी है. इन तमाम मौतों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण हिरासत के दौरान होने वाला टॉर्चर और ज़ुल्म व शोषण है जिसको मानव शरीर सहन करने में नाकाम हो जाता है.
जबकि पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या 417 और न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या 4285 दर्ज की है, जो हमारे देश की न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है.
इन मौतों के आंकड़े को सामने रखकर हमारे दिमाग़ में सिर्फ और सिर्फ उसी पुलिस की तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसकी बुनियाद 1860 में अंग्रेजों ने रखी थी. जिसके नज़दिक हर वो व्यक्ति जो सरकारी जुल्म व ज़्यादतियों के खिलाफ इंसाफ और हक़ की आवाज़ उठाता था, वह देश का दुश्मन होता था.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ये आंकड़े वास्तविक घटना से किस हद तक करीब हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर के संबंध में सामने आए तथ्य ही हक़ीक़त से पर्दा उठाने के लिए पर्याप्त हैं.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस दशक में जम्मू कश्मीर में हिरासत में मौतों की संख्या महज़ 6 दर्ज की है, हालांकि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 13 मार्च 2011 में राज्य के विधान परिषद की बैठक में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए 1990 के बाद केवल पुलिस हिरासत के दौरान मौतों की संख्या 341 स्वीकार की है, हालांकि मुख्यमंत्री के ये आँकड़े भी ख़ुद सरकारी रिकॉर्ड से लिए गए हैं. सरकारी रिकॉर्ड सरकारी अत्याचार और आक्रामकता के बारे में किस हद तक न्याय पर आधारित होता है, यह भी एक अहम सवाल है.
हाल ही में खालिद मुजाहिद की हत्या ने एक बार फिर लोगों को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, जैसा कि पिछले साल पुणे की यरवदा जेल में क़तील सिद्दीकी की हत्या ने या उससे पहले ख्वाजा यूनुस की हत्या के बाद हमने देखा था. यह सवाल अगर खालिद मुजाहिद या अन्य दुर्घटनाओं में से किसी एक दुर्घटना तक सीमित कर दिया जाए तो यह मानवता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी.
खैर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थिति पर अगर गौर किया जाए तो हिरासत में होने वाली मौतों में तेजी के साथ वृद्धि होती जा रही है. 1993-94 के दौरान हिरासत में मौतों की संख्या 34 थी, 1998-99 में यह संख्या बढ़कर 1297 हुई, लेकिन 2004-05 में हिरासत के दौरान मौतों की संख्या 1493 तक पहुंच गई. हिरासत के दौरान मौत का शिकार होने वालो को इंसाफ दिलाने का मामला अदालत तक पहुंचता रहा है, अदालत मुआवजा देती रही हैं. जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नीलाबती बहरा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में दिया.
और वैसे भी यह मुआवजा सरकार के सिर जाता है. जैसा कि महिला मूरन बनाम स्टेट ऑफ असम या फिर फूलवती बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली जैसे कई फैसलों में कहा गया. यही नहीं, इस घटना की आपराधिक दायित्व ऑफिसर इंचार्ज के सिर बांधी गई.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हमेशा मुआवजा पर जोर दिया. पिछले 20 वर्षों में आयोग ने कभी भी अपराधियों के खिलाफ अदालत में मुक़दमा या सजा की वकालत नहीं की, यानी अगर किसी नागरिक को ज़ुल्म व सितम का शिकार बनाया जाता है, उसकी क्रूर हत्या कर दी जाती है. लेकिन उसके रिश्तेदार सालों-साल की लंबी कानूनी और न्यायिक पेचीदगियों का सामना करने के बाद सिर्फ कुछ मुआवजे के हक़दार स्वीकार किए जाएंगे. और वो मुआवज़ा उन्हीं जैसे नागरिकों से वसूले गए टैक्स से अदा की जाती है. वाह रे हमारी न्यायिक व्यवस्था… शायद ऐसी व्यवस्था हिरासत के दौरान मौतों के आंकड़ों में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि का कारण ही बन सकता है.
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार संरक्षण के पक्ष में बहुत सी बातें अपने फैसलों में दर्ज की हैं, जैसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा “अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सभ्य समाज का गला घुट जाएगा… पुलिस अगर आपराधिक कार्रवाईयों में शामिल पाया जाए तो उस अपराध के मामले में आम लोगों को दी जाने वाली सज़ाओं से ज्यादा कठोर सज़ा के हक़दार यह पुलिस वाले होने चाहिए, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है न कि स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाना…”
इसके अलावा अनगिनत फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस व्यवस्था में प्रचलित ज़ुल्म व टॉर्चर को स्वीकार किया है, लेकिन कभी कोई सकारात्मक पहल इस दिशा में सरकार की ओर से नहीं की गई.
हमारे पास ऐसे अनगिनत मिसालें हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में दर्ज किया गया है कि किसी नागरिक की पुलिस गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत उस नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करके नहीं कर सकते. यही नहीं, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह संविधान की धारा-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में संपर्क कर सकता है. हिरासत उसकी आज़ादी को पाबंद तो कर सकती है, लेकिन यह उसे इसके मानव अधिकार से वंचित नहीं कर सकती.
संविधान की धारा-20 साफ शब्दों में कहती है कि किसी भी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, और न ही उसके साथ किसी प्रकार का गैरइंसानी व्यवहार किया जाएगा, जो अपराध हो, उसी के अनुसार कानून के मुताबिक ही सजा दी जा सकती है.
संविधान की धारा-21 टॉर्चर के एवं तमाम संबंधित ज़ुल्म व ज़्यादती से सुरक्षा प्रदान करती है. इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार रखता है, उसे किसी तरह के अत्याचार और ज़्यादती का शिकार नहीं बनाया जाएगा.
संविधान की धारा-22 के तहत प्रत्येक नागरिक को हिरासत व गिरफ्तारी के दौरान बहुत से अधिकार दिए गए हैं. जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले उसके गिरफ्तारी के कारणों, वकील से कानूनी सहायता, किसी करीबी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेशी आवश्यक क़रार दिया गया है.
इंडियन एवीडेन्स एक्ट-1872 की धारा-25 के तहत पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी का पुलिस को दिया गया इक़बालिया बयान का कोई कानूनी महत्व नहीं होगा, और न ही उसे किसी अदालत में बतौर सबूत पेश किया जा सकता है. हालांकि पिछले तीन दशकों के दौरान आतंकवाद से मुकाबले के नाम पर तीन ऐसे काले कानून (पोटा, टाडा और मकोका) भी लागू गए जिनमें पुलिस को दिया गया इक़बालिया बयान सबूत का महत्व रखता है. मकोका के अलावा शेष 2 कानून तो अपने बेजा इस्तेमाल के कारण एक सीमा तक पहुँचने के बाद प्रतिबंधित दिए जा चुके हैं, लेकिन मकोका आज भी ज़ुल्म व ज़्यादती का एक विशेष हथियार बना हुआ है. इसी कानून की धारा-24 के तहत धमकी, दबाव या वादे के ज़रिए लिया गया इक़बालिया बयान किसी भी अदालत में इस्तेमाल योग्य नहीं होगा.
भारतीय दंड संहिता-1860 के कई प्रावधान हर नागरिक को पुलिस अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करती है, यदि उनका सही उपयोग किया जाए. संहिता की धाराओं जैसे धारा-330, हिरासत के दौरान इक़बालिया बयान लेने के लिए टॉर्चर किया गया हो, और कुछ मामूली ज़ख्म ही बने हो, धारा-331, जब हिरासत के दौरान गंभीर ज़ख्म हुए हो. धारा-342 में उसके सज़ा का उल्लेख है जो एक वर्ष के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना और धारा-348 के तहत जबरन अपराध स्वीकार करने की खातिर या माल की वापसी के लिए बेजा कैद, इन प्रावधानों के तहत अगर गिरफ्तार या हिरासत में रखने वाला पुलिस ऑफिसर दौरान थर्ड डिग्री टार्चर का उपयोग करता है तो वह टार्चर का दोषी क़रार दिया जाएगा. इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले “स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम श्याम सुन्दर द्विवेदी (1995 ई.) में दर्ज किया है.
हिरासत के दौरान टार्चर के मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अगर हिरासत में मौत हो गई हो तो धारा 302, 304,304ए और जब आपको महसूस हो कि मृतक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है तो धारा-306 के तहत जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुक़दमा अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है.
क्रिमिनल प्रोसिज़र कोड (सीआरपीसी) की कई ऐसी धाराएं हैं जो आम नागरिकों को पुलिस के बेजा शोषण से सुरक्षा प्रदान करती हैं. जैसे धारा-46 और 49 उन सभी लोगों को हिरासत के दौरान टॉर्चर से रक्षा करती है, जो ऐसे अपराधों में आरोपी न हों जिनकी सज़ा आजीवन कारावास या मौत न हो. यानी किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार न किए गए हों.
धारा-50 से 56 तक जिसकी संविधान की धारा-22 में भी चर्चा की गई है. विशेष तौर पर धारा-54 के तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पहले अपनी मेडिकल जांच करवा सकता है. इस सिद्धांत का उल्लेख मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले ए.के. सहदेव बनाम रमेश ननजी शाह में भी किया है, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के टॉर्चर या ज़्यादती के मामले में मेडिकल जांच जिसका सर्टिफिकेट प्रभावित व्यक्ति को प्रदान करना आवश्यक है. अगर प्रभावित व्यक्ति के आवेदन पर मजिस्ट्रेट / जिला न्यायाधीश उक्त कार्रवाई का निर्देश नहीं देता है तो सीआरपीसी की धारा-482 के तहत हाईकोर्ट में हस्तक्षेप के लिए आवेदन किया जा सकता है, जैसा कि मुकेश कुमार बनाम स्टेट के मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया.
हिरासत के दौरान मौत के मामले में बुनियादी महत्व सीआरपीसी की धारा-176 पर निर्भर है. इस धारा के अनुसार हिरासत के दौरान मौत होने पर मौत के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट के ज़रिए जांच ज़रूरी क़रार दिया गया है.
इंडियन पुलिस एक्ट की धारा 7 और 29 के तहत अगर पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी और दायित्वों की अदायगी में कोताही या असफल साबित होता है, या ईमानदारी बरतने में नाकाम होता है तो उक्त धाराओं में बरखास्तगी, जुर्माना और निलंबन का प्रावधान हैं.
इसी तरह आपराधिक मामलों की कार्रवाईयों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के डी.के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और भाई जसबिर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब और शीला बरसे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के फैसले में देख सकते हैं. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले और बाद की कार्रवाईयों के संदर्भ में अहम निर्देश जारी किए हैं, इस निर्देश का बोर्ड सभी ही पुलिस स्टेशनों में दिवारों की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी हिरासत के दौरान मौत के सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि पुलिस या न्यायिक हिरासत में होने वाली मौत के सिलसिले में संबंधित राज्य या केंद्र सरकार 24 घंटे के अंदर आयोग को सूचना देगी, साथ ही पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ आयोग को भेजी जाएगी. इसके अलावा पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ज़रिए कराए जाने के भी आदेश हैं.
हमारे देश के संविधान और अन्य क़ानून में हालांकि शब्द टॉर्चर का उपयोग मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे दिशा-निर्देश हैं जो हिरासत में मौतों पर कानूनी लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. आज ज़रूरत है कि व्यक्तिगत घटनाओं को सामाजिक अहमियत दी जाए, अगर सामाजिक समस्या को समाज ईमानदारी से महसूस करे, संगठित तरीके से जिला स्तर पर प्रेशर ग्रुप तैयार किए जाएं जो समाज के जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर सड़क से लेकर अदालत तक इन मुद्दों पर संघर्ष करे तो यह समस्या आसानी से काबू में आ सकती है, लेकिन सच तो यह है कि आज तक इस मुद्दे को लेकर सामाजिक स्तर पर मात्र वक़्ती व जज़्बाती विरोध प्रदर्शनों के अलावा कोई भी संघर्ष नहीं किया गया. समय की मांग है कि एक संगठित कानूनी संघर्ष किया जाए, जिसके बुनियादी स्तंभ ईमानदारी, कड़ा संघर्ष, सामाजिक कोशिश व सरपरस्ती , मानव सोच और धैर्य है, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ न्याय के रास्ते ही जीत संभव है और न्याय का रास्ता हमेशा अदालत से होकर गुजरता है.
(लेखक एसोशियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राईट्स से जुड़े हैं.)