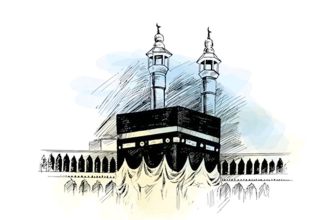Anurag Bakshi for BeyondHeadlines
राज्यसभा में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कोलेजियम प्रणाली की वजह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बिगड़ गया है और यह व्यवस्था बनाकर न्यायपालिका ने 1993 में संविधान को एक तरह से दोबारा लिख दिया.
क्या न्यायपालिका के दोष गिन रहे कानून मंत्री यह दावा करने की स्थिति में हैं कि कार्यपालिका यानी सरकार ने अपना काम सही तरह किया है? सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि अगर बदली हुई व्यवस्था में आम जनता यह महसूस करती है कि सरकार के दखल के कारण न्यायाधीश अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं रख पा रहे तो यह देश के लिए अत्यंत घातक होगा.
 यह स्पष्ट है कि अब सभी राजनीतिक दल इस पर एकमत हैं कि कोलेजियम व्यवस्था को बदला जाना चाहिए. पिछले दिनों राज्यसभा में न्यायपालिका की आलोचना में दलीय दीवारें टूटती दिखाई दीं. इस व्यवस्था को बदले जाने की आवश्यकता जिन कारणों से महसूस हो रही है, उनमें एक कारण यह बताया जा रहा है कि कुछ काबिल समझे जाने वाले न्यायाधीश शीर्ष पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात हो रहा है.
यह स्पष्ट है कि अब सभी राजनीतिक दल इस पर एकमत हैं कि कोलेजियम व्यवस्था को बदला जाना चाहिए. पिछले दिनों राज्यसभा में न्यायपालिका की आलोचना में दलीय दीवारें टूटती दिखाई दीं. इस व्यवस्था को बदले जाने की आवश्यकता जिन कारणों से महसूस हो रही है, उनमें एक कारण यह बताया जा रहा है कि कुछ काबिल समझे जाने वाले न्यायाधीश शीर्ष पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्षपात हो रहा है.
पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने सक्रियता का परिचय दिया है. पर्यावरण से लेकर जनता के अधिकारों और राजनीतिक दलों के कामकाज से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिनमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है. न्यायपालिका के इस हस्तक्षेप को राजनीतिक दलों ने उसकी अति सक्रियता माना है. यह भी स्पष्ट है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में कुछ अदालती आदेशों के चलते योजनाओं-परियोजनाओं पर बाधाएं भी खड़ी हुईं, जिसके चलते देश की आर्थिक हानि भी हुई और सरकार की फजीहत भी.
एक तथ्य यह भी है कि कुछ मामलों में अदालती हस्तक्षेप के बाद सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार की पोल खुली और जांच का आधार तैयार हो सका. आश्चर्य नहीं कि इस सबके चलते ही राजनीतिक दलों ने यह महसूस किया हो कि न्यायिक तंत्र के कामकाज पर नए सिरे से निगाह डालने की आवश्यकता है.
केवल राम जेठमलानी ही ऐसे थे जो प्रस्तावित कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बता रहे थे. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस संविधान संशोधन विधेयक पर खामोश है. क्योंकि मामला संसद का है. सुप्रीम कोर्ट को इंतजार रहेगा कि कब इस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और यह कानून का रूप लेता है. हो सकता है कि कोई इस प्रस्तावित कानून को सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दे. यदि ऐसा होता है तो शीर्ष अदालत को इस पर नए सिरे से निगाह डालने का मौका मिलेगा. इसकी संभावना कम ही है कि सुप्रीम कोर्ट इस बड़े बदलाव को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेगा कि राजनेताओं को न्यायपालिका की सक्रियता से परेशानी हो रही है.
देश अभी तक यह नहीं जान सका है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का एकाधिकार अपने पास रखने के पीछे न्यायपालिका का क्या उद्देश्य था और अब इस एकाधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आम जनता इस सवाल का जवाब इसलिए जानना चाहेगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में वह न्यायपालिका को ही उम्मीद की अंतिम किरण के रूप में देख रही है.
इसमें संदेह नहीं कि न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार के आरोपों से पूरी तरह अछूती नहीं हैं. लेकिन राजनेताओं और प्रशासनिक तंत्र के मुकाबले न्यायपालिका को आम तौर पर साफ-सुथरा ही माना जाता है. पिछले कुछ समय में अनेक मामलों में फैसला देते हुए न्यायपालिका ने शासन और प्रशासन के कामकाज पर जैसी टिप्पणियां की, उससे आम जनता के बीच यही धारणा कायम हुई कि उसके हितों की परवाह केवल अदालतें ही कर रही हैं. इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि मौजूदा समय अनेक नामी-गिरामी वकील राजनीति में सक्रिय हैं. इसलिए यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में हेरफेर के पीछे कहीं न्यायपालिका के प्रति उनकी व्यक्तिगत राय तो नहीं?