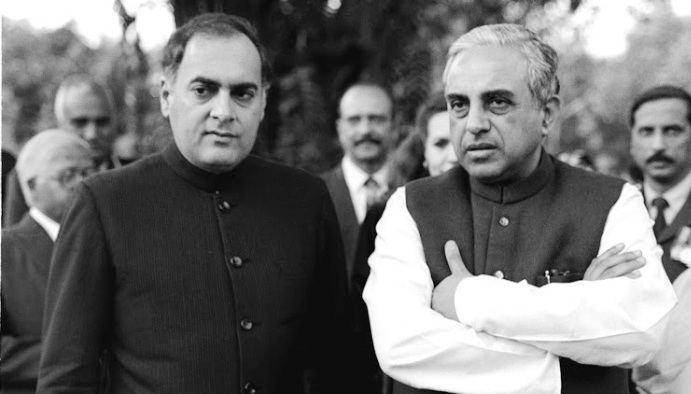Shahnawaz Alam for BeyondHeadlines
उत्तर प्रदेश के मुज़फरनगर-शामली में पिछले दिनों हुई मुस्लिम विरोधी साम्प्रदायिक हिंसा का विश्लेषण इस बात को समझने के लिए तो किया ही जाना चाहिए कि हिंदुत्व जब चाहे और जहां चाहे, बिना अपनी सरकार के भी ‘गुजरात’ दुहराने में सक्षम हो चुका है तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में गैर-सियासी दिखने वाले मुस्लिम धार्मिक संगठनों के सियासी कार्यप्रणाली जो अंततः सत्तापक्ष को तमाम लानतों के बाद भी क्लीन-चिट देता है, को भी समझने के लिए इसका विश्लेषण ज़रूरी है. जो अपने मूल में मुसलमानों के बीच पनपे सियासी खालीपन को भरने की कोशिश करती ताक़त होने के चलते अपने व्यवहार (जो कहीं और से संचालित और नियंत्रित होता है) से बार बार साबित करते हैं कि सपा या दूसरी मध्यमार्गी कथित सेक्यूलर पार्टियों को किस तरह की और किस हद तक की मुस्लिम आकांक्षाएं स्वीकार्य हैं.
इस परिघटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें मुज़फ्फनगर-शामली जैसी घटनाओं के बाद मुसलमानों की तरफ से जांच आयोगों के गठन की मांग जिसे सरकारें मान भी लेती हैं, जैसा कि इस मामले में भी सपा सरकार ने जस्टिस विष्णु सहाय जांच आयोग का गठन कर के किया है, की राजनीति का विश्लेषण करना होगा.
क्योंकि हर ऐसी घटना के बाद जांच आयोगों का गठन राजनीतिक दलों के सेक्यूलर होने की कसौटी मानी जाने लगी है. जबकि यह कसौटी अपने आप में अंतरविरोधी है. मसलन, जांच आयोग गठित करने की घोषणा तो आप को सेक्यूलर बना सकती है लेकिन उसकी सिफारिशों पर अमल आपके मुस्लिम परस्त और हिंदुविरोधी घोषित हो जाने का खतरा भी रखती है, जिसे उठाने का साहस अधिकतर राजनीतिक दल नहीं रखते. क्योंकि हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रचलित मनोविज्ञान सहिष्णुता (हिंदु धर्म की) पर टिका है (सम्प्रति मोहनदास करमचंद गांधी)
स्वभावतः जिसकी एक सीमा है जिसके परे जाने पर वह धर्मनिरपेक्षता को बर्दाश्त नहीं कर पाता. यानी हमारी राजनीति उतनी ही सेक्यूलर हो सकती है जितनी हमारी हिंदुत्ववादी जेहनियत उसे छूट देती है. इसीलिए हम मलियाना, बाबरी मस्जिद विध्वंस या बम्बई के सवाल पर अपनी सारी धर्मनिरपेक्षता को जांच आयोगों के गठन तक जाते-जाते दम तोड़ देते हुए देखते हैं. या अगर वह इन आयोगों की रपटों को जन-दबाव में जारी करने का साहस दिखा भी दे तो साम्प्रदायिक ताकतों के यह कह भर देने से कि रिपोर्ट हिंदु विरोधी है (जैसा कि कांग्रेस सरकारों द्वारा श्री कृष्ण आयोग या लिबराहन आयोग की रपटों के सार्वजनिक किये जाने पर भाजपा और शिवसेना ने कहा था) हमारी कथित सेक्यूलर पार्टियां बैकफुट पर आ जाती हैं.
इस तरह जांच आयोग हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बैरियर बन जाता है जिसे ‘पार नहीं करना है.’ सपा-कांग्रेस जैसी पार्टियां मानती हैं तो वहीं इसे ‘पार नहीं किया जा सकता’ यह धारणा मुसलमानों में मज़बूत होते जाता है जो अंततः ऐसी पाटिर्यों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.
परिणामतः हर मुस्लिम विरोधी हिंसा के बाद मुसलमानों में नागरिक होने की राजनीतिक चेतना का क्षरण होता है. जिसके चलते वह विक्टिमहुड (दमित होने के चलते निराशा में पैदा हुई आत्मदया की भावना जो आपस में भी एक दूसरे को जोड़ती है) के गहरे मानसिक और वैचारिक दलदल में धंसता जाता है.
मुज़फ्फरनगर-शामली के विभिन्न राहत शिविरों के कुछ दृश्यों से मुसलमानों के नागरिकीय चेतना के क्षरण (अनागरीकीकरण) की इस प्रक्रिया को समझा जा सकता है.
दृश्य -1. शामली के कैराना कैम्प जहां 10 हजार मुसलमान पनाह लिए हैं, में तब्लीगी जमात (जो धर्मप्रचार का काम करता है, जिसका मुख्य जोर मुसलमानों को दुनियावी चीजों के बजाए दीन/धर्म की ओर लौटाना है) का एक दल अपनी उपस्थिति की वजह बताते हुये समझाता है कि ऐसे बुरे वक्त में ही लोगों में भटकने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. लिहाजा उन्हें नमाज़ से जोड़े रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो वह कैम्पों में नमाज़ की अहमियत सम्बंधी बुकलेट बांटकर कर रहे हैं. इस त्रासदी की वजह मुसलमानों का दीन से दूर होना मानने वाला तब्लीगी कार्यकर्ता जो मानता है कि ‘इंसाफ सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है और मुसलमानों को सिर्फ उसी से इसे मांगना चाहिए’ ने इस जनसंहार के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को दुनियावी काम बताते हुये ‘हमारा काम सिर्फ दीनी है’ कह कर संवाद को खत्म कर देता है.
दृश्य -2. लगभग 5 हजार मुसलमानों की पनाहगाह बने जोगिया खेड़ा कैम्प में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में जिनका एजेंडा सरकार की किरकिरी का सबब बने इन कैम्पों को किसी भी कीमत पर बंद कराना है, में एक बड़े उलेमा संगठन के स्थानीय नेता लोगों को अपने गांव लौट जाने (जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं) को प्रेरित करने के लिए अरबी में एक आयत पढ़ते हैं, जिसका अनुवाद उनके मुताबिक यह है कि इंसान की मौत वहीं होगी जहां किस्मत में लिखी होगी. लिहाजा उन्हें लौट जाना चाहिए.
यहां यह जानना ज़रूरी होगा कि सपा सरकार ने जनसंहार के आरोपियों (जाटों) को कथित फर्जी मुक़दमों से बचाने और जाटों और पीडि़त मुसलमानों में सद्भाव कायम करने के लिए ‘फैसला पंचायतें’ आयोजित करने का अभियान चला रखा है. जिसका मक़सद सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अखबारों में दिए गए बयानों के मुताबिक मुसलमानों को दुबारा गांव लौट जाने और आरोपियों पर से मुक़दमा उठा लेने के लिए उन्हें तैयार करना है. वहीं दूसरी ओर जिन पीडि़त मुसलमानों ने अपने गांव लौटकर बचे-खुचे सामान लाने की कोशिश की उनसे गांव के जाटों ने पुलिस के सहयोग से जबरन हलफनामे लिए कि उनके साथ कोई हिंसा नहीं हुयी और उन्हें हिंदुओं से कोई शिकायत नहीं है.
दरअसल पीडि़त मुसलमानों को दुबारा गांवों में भेजने की रणनीति ही इसलिए बनायी गयी है कि अगर ये लोग गांव नहीं गए और बाहर ही कहीं बस गए तो मुक़दमों में अपनी गवाही पर कायम रह जाएंगे. क्योंकि तब उन पर गांवों के जाटों का कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा.
दृष्य -3. कांधला ईदगाह कैम्प जहां 10 हजार के करीब मुसलमान हैं, में ‘अमन का कारवां’ लेकर लखनऊ से एक सत्ता के करीबी उलेमा पहुंचे हैं. जिनके पिछले दिन के एक ऐसे ही कैम्प में आयोजित कार्यक्रम की अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अमन का यह कारवां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कहने पर निकाला है ताकि सूबे में अमन कायम हो सके. कैम्प में मौजूद पीडि़तों के लिए यह कौतूहल का विषय है कि हिंसा के शिकार लोगों के बीच अमन का संदेश लेकर किसी के आने का क्या मतलब है? वे जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करके वे उन्हें ही अपनी स्थिति का जिम्मेदार बताना चाहते हैं?
दृष्य -4. लगभग हर कैम्प में सामुहिक शादियां कराते धार्मिक संगठन, जिनमें सपा सरकार के मंत्री और नेताओं की उपस्थिती अहम.
दृष्य -5. हिंसा पीडि़तों के लिए अपनी तंजीम की तरफ से रिहायशी कॉलोनी की बुनियाद रखते एक बड़े उलेमा संगठन के सदर (जो अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुलायम सिंह को बुलाने के लिए मशहूर हैं. पिछले 22 अक्टूबर को स्थानीय प्रशासन द्वारा तकनीकी कारणों से उनके रिहायशी कॉलोनी को रोकने की कोशिश से नाराज मौलाना ने लखनऊ में मुलायम और अखिलेश से स्थानीय प्रशासन की शिकायत की थी)
इन दृश्यों के राजनीतिक निहितार्थों पर गौर किया जाए तो इसके केंद्रक उत्तर प्रदेश के इतिहास के इस सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी संगठित हिंसा को नियती, इस्लाम से भटके मुसलमानों पर अल्लाह का कहर साबित करने की कोशिश करते दिखने के साथ ही इंसाफ की कानूनी लड़ाई लड़ने से पीडि़तों को हतोत्साहित करते दिखेंगे. इसके साथ ही दोषियों को सजा दिलाने, पीडि़तों को दुबारा उनकी मर्जी के स्थान पर बसाने जैसी संवैधानिक जिम्मेदारियों से सरकार को मुक्त कर, इन जिम्मेदारियों में खुद अपने को लाने, जिसमें सरकार भी इनकी मदद करती है, करते दिखेंगे.
इस तरह धार्मिक संगठन और स्वयं राज्य मशीनरी खुद अपने प्रयासों से मुसलमानों के अनागरिकीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देती देखी जा सकती है. जिसके परिणामस्वरूप मुसलमानों में विक्टिमहुड की मानसिकता और मज़बूत होती है, जो धीरे-धीरे पूरे समुदाय की सोच बनती जाती है.
यहां यह गौर करना ज़रूरी होगा कि राज्य द्वारा अपने ही नागरिकों को नागरिक होने की हैसियत से प्राप्त अधिकारों के प्रति उदासीन करने और उनकी नागरीकीय ज़रूरतों की पूर्ती के लिए उन्हें सरकार के बजाए गैरसरकारी तंत्र (जो विचार के स्तर पर लोकतंत्र-विरोधी होते हैं जैसे कॉर्पोरेट तंत्र जिसमें एनजीओ भी शामिल हैं और धर्मतंत्र) की ओर धकेलना मौजूदा व्यवस्था की विशेषता बनती जा रही है. लिहाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई तार्किक अड़चन नहीं होनी चाहिए कि जनता को नागरिक अधिकारों से लैस करने का दावा करने और इसी बुनियाद पर संचालित होने वाले हमारे लोकतंत्र की ज़मीनी सच्चाई यही है कि वह अपनी ही जनता के एक बड़े हिस्से के अनागरीकीकरण पर टिका है. यही उसके होने का तर्क है. वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के अमीर होने का तर्क औरों का उससे गरीब होना होता है.
इसीलिए अनागरिकीकरण की प्रक्रिया के रूकने या बाधित होने से (नागरीकीय चेतना के विकसित और मज़बूत होने से) मौजूदा लोकतांत्रिक ढांचा डरता है, कि वह टूट जाएगा. इसीलिए हम पूरी राज्य मशीनरी, दक्षिण और मध्यमार्गी पार्टियों, मीडिया सभी को अपने-अपने स्तर पर जनता के कमजोर हिस्सों के अनागरिकीकरण की इस प्रक्रिया को मज़बूत करते देख सकते हैं. मसलन, छत्तीसगढ़, उडि़सा या झारखंड में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ खनिजों की लूट नहीं है, इसको सम्भव और शासकवर्गीय हितों के पक्ष में तार्किक बनाने के लिए आदिवासीयों को जबरन नागरिक न मानने की परियोजना भी है. हजारों की तादाद में राज्य की जिम्मेदारियों को खुद निभाने की होड़ मचाने वाले एनजीओ वहां ऐसे ही नहीं सक्रीय हैं.
बहरहाल, यहां यह देखना भी ज़रूरी होगा कि अनागरिकीकरण का राजनीतिक लाभ ज्यादा आक्रामक तरीके से शासकवर्ग भले ही भूमंडलीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद से ले रहा है, लेकिन इसकी वैचारिक बुनियाद आजादी के दूसरे-तीसरे दशक में ही पड़ गई थी. जिसमें जनता की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया. शासकवर्ग ने इन समस्याओं से ग्रस्त अवाम से नागरिक होने के नाते मिले राजनीतिक चेतना और अधिकार को त्याग देने का समझौता किया कि इस शर्त को मानने के बाद ही वे उन्हें इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा.
इस तरह अपनी घोर दरिद्रता के बावजूद सौ साल तक अंग्रेजी साम्राज्यवाद और दो दशक तक अपनी ही चुनी सरकारों से राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाली अवाम को यह समझाने की कोशिश शुरू हुई कि उसकी ज़रूरत सिर्फ रोटी-कपड़ा-मकान है (रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान) जिसका राजनीतिक एजेंडा आम अवाम के जेहन से सत्ता-शासन में निर्णायक होने या उस पर काबिज़ होने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर देना था. आम लोगों को बताया गया कि वो सिर्फ अपने रोटी कपड़े की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं, जबकि राजनीतिक सत्ता संचालन खास लोगों का काम है.
इस पूरी परियोजना में शासकवर्ग ने जनता के सामने कई कृत्रिम समस्याओं को मुद्दा बना कर पेश किया और आह्वान किया कि लोग इनके खिलाफ उनके नेतृत्व में ही संघर्ष करें, जबकि इन समस्याओं के कारक वे खुद थे. शासकवर्ग की तत्कालीन सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी के ‘गरीबी हटाओ’ नारे के पीछे जुटी भीड़, अपने नागरिक होने से प्राप्त राजनैतिक चेतना को छोड़ने के समझौते की पृष्ठभूमि में हुआ शासकवर्ग का सबसे सफल और निर्णायक आयोजन था. जबकि इसके विपरीत वाम धारा की राजनीति ने गुलाम से प्रजा और प्रजा से नागरिक बनने के मनुष्यता के लम्बे और ऐतिहासिक संघर्षों से प्राप्त राजनीतिक मूल्यों को संरक्षित और मज़बूत करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी के प्रति निष्ठा दिखाते हुये व्यवस्था जनित भुखमरी-बेरोजगारी जैसी समस्याओं के खिलाफ जनता के नागरिकीय चेतना को बचाए रखते हुये विचारधारात्मक संघर्ष कायम रखा. इसीलिए उनके नारे में हिंदुस्तान सिर्फ रोटी-कपड़ा नहीं मांगता. वह उसके साथ लाल निशान भी मांगता है (रोजी रोटी लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान)
नागरिकीय चेतना के क्षरण और उससे लैस अवाम के फर्क जिसकी तुलना हम मार्क्सवादी अवधारणा में ‘क्लास इन इटसेल्फ’ (अपने आप में वर्ग) और ‘क्लास फॉर इटसेल्फ’ (अपने लिए वर्ग) के फर्क से भी कर सकते हैं, को समझने के लिए हमें कांग्रेस-भाजपा-सपा जैसी पार्टियों के प्रभाव वाले आम लोगों और वाम जनवादी धारा (संसदीय और गैरसंसदीय) प्रभाव के आम लोगों के बीच के फर्क को देखना चाहिए. जहां पहली स्थिति में वह रोटी-कपड़ा-सड़क को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत बताता है, जिसे पूरा करने का वादा हर चुनाव में पार्टियां उससे करती हैं. जिसके चलते वह हर चुनाव के बाद राजनीतिक चेतना और हैसियत को खोकर नागरिक से याचना करते लालची व्यक्ति में तब्दील होता जाता है. वहीं वाम जनवादी प्रभाव के आम लोग कहीं प्लेकार्ड तो कहीं बंदूक लिए देश की सम्प्रभुता, संसाधनों पर अपनी खुदमुख्तारी का सवाल उठाते हुये हजारों सालों के संघर्ष के बाद प्राप्त आधुनिक मनुष्य की राजनीतिक गरिमा (उसकी नागरिक हैसियत) को प्रदर्शित करता है.
दरअसल बुरे से बुरे दौर में भी नागरिकीय चेतना को बचाना और विकसित करना ही वास्तविक (जनवादी) लोकतंत्र है. जबकि पूंजीवादी लोकतंत्र जनता के समक्ष आए हर संकट (मसलन साम्प्रदायिक हिंसा) का इस्तेमाल उसके नागरिकीय चेतना को कुंद करने, उसे त्यागने के लिए मजबूर करने के लिए करता है.
इसीलिए मुज़फ्फरनगर-शामली या देश के किसी भी हिस्से में साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार मुसलमान जब कहते हैं कि उन्हें इस व्यवस्था से सिर्फ सुरक्षा की गारंटी चाहिए तब वह नागरिक होने के चलते हासिल अपनी सियासी चेतना, आकांक्षाओं और ताक़त को सरकारों और पार्टियों के सामने सुरक्षा के शर्त पर त्याग रहे होते हैं. और यही समपर्ण उनके विरूद्ध हिंसा की राजनीति करने वालों को ताक़त देती है.
बहरहाल, साम्प्रदायिक हिंसा पीडि़त मुसलमानों के नागरिकीय चेतना के क्षरण और उसके समानांतर हमलावरों (यहां जाटों) का नागरिकीय सशक्तिकरण (व्यवस्था के अंतर्गत जो सम्भव हो सके जैसे नौकरियों में आरक्षण, गिरफ्तारियों से छूट इत्यादि) एक साथ कैसे संचालित होता है, इसके कुछ उदाहरण भी इस पूरी परिघटना को समझने के लिए ज़रूरी होगा.
पहला- राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जो इस जाट लैंड के सबसे प्रभावशाली क्षत्रप माने जाते हैं, मुज़फ्फरनगर आने से पहले जाटों को नौकरियों में आरक्षण देने का शिगूफा छोड़ते हैं और आने के बाद सिर्फ जाटों के बीच ही जाते हैं. उनके नेताओं से मिलकर (जिनमें गठवाला खाप के मुखिया हरिकिशन मलिक जिन पर इस जनसंहार का मास्टर माइंड होने का आरोप और कई संगीन मुक़दमे हैं, भी शामिल हैं) किसी भी ‘बेकसूर’ की गिरफतारी नहीं होने देने का आश्वासन देते हैं. उनसे गन्ना मूल्यों, गांव में पक्की सड़क और बिजली पर बात करते हैं.
दूसरा – भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल घोषणा करता है कि वह 27 अगस्त को मारे गए गौरव और सचिन के गांव मलिकपुरा में पक्की सड़क बनवाएगा.
तीसरा – प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से गौरव और सचिन के रिश्ते की बहन (जिसकी कथित छेड़खानी के आरोप में पहले गौरव और सचिन आदि ने शाहनवाज़ नाम के मुस्लिम युवक की हत्या की और उसके तत्काल बाद मुस्लिमों द्वारा गौरव और सचिन का कत्ल कर दिया गया. हालांकि आश्चर्यजनक रूप से दोनों पक्षों की तरफ से की गयी एफआईआर में छेड़खानी जैसी घटना का कोई जिक्र नहीं है और विवाद का कारण बाईक टकराने को लेकर हुई तूतू-मैंमैं बताई गई है) ने जो मांग-पत्र सौंपा उसमें गांव में पक्की सड़क बनवाने जैसी मांग थी.
चार – सपा के मुस्लिम नेता कैम्पों में राहत कार्य करते फोटो खिचवाते हैं तो वहीं पार्टी के हिंदु नेता जाटों को ‘निर्दोषों’ का उत्पीड़न नहीं होने देने का भरोसा दिलाते फोटो खिंचवाते हैं.
पांच – हिंदी मीडिया पूरे दो-दो पेज जाट गांवों में कथित निर्दोष जाट पुरूषों के उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के हथियारबंद प्रदर्शन की बड़ी-बड़ी तस्वीरों सहित कवरेज देता है. तो वहीं पूरे एक पेज पर राहत कैम्पों में धार्मिक संगठनों द्वारा करायी जा रही शादियों, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा लगाए गए मेडिकल कैम्पों की तस्वीरें और खबरें रहती हैं. जिनके शीर्षक और खबरों की भाषा भावनात्मक और मुहावरेदार है, जिससे प्रतीत होता है कि हजारों की संख्या में मुसलमान इन कैम्पों में किसी प्राकृतिक आपदा के चलते आए हैं और ‘सदियों पुरानी भाईचारा, गंगा-जमुनी तहजीब’ को किसी अंजान ताक़त ने आग लगा दी हो. वहीं जाट महिलाओं के आंदोलन की खबर की भाषा अत्याधिक राजनीतिक है जहां उनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की जा रही है. वहीं उर्दू अखबारों में इम्दाद (मदद पहुंचाने/पुण्य कमाने) महोत्सव की तस्वीरें और खबरें कई-कई पृष्ठों तक फैली हुई हैं.
बहरहाल, नागरिकीय हैसियत के क्षरण के साथ बनते मुसलमानों के ‘विक्टिमहुड’ की मानसिकता का मुख्य स्वर ‘शिकायती’ होता है जो धीरे-धीरे एक वैचारिक अवधारणा का रूप ग्रहण करता जाता है.
यहां यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि दलितों के अस्मिता आधारित राजनीतिक उभार का मुख्य स्वर भी ‘शिकायती’ था. लेकिन हिंदु धर्म के अंदर की इकाई (बहिष्कृत ही सही) होने के चलते सत्ता में उसके समायोजन (राजनीतिक तौर पर उनके संस्कृताइजेशन) के साथ ही उसकी ‘शिकायती’ मुद्रा समाप्त होती गयी.
लेकिन हिंदु धर्म के दायरे से बाहर के ‘शिकायती’ समूह होने के कारण मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हो सकती थी. इसलिए उसकी शिकायती मुद्रा (विक्टिमहुड) एक समानांतर वैचारिक (खुले तौर पर प्रतिक्रियावादी और छुपे तौर पर इस्लामिस्ट), राजनीतिक (यथास्थितिवादी और वाम विरोधी) और आर्थिक (राजनीतिक कार्य-संस्कृति वाले संगठनों की तरह सवाल ‘हल’ करने के बजाए सवाल ‘उठाने’ के नाम पर धन संग्रह) तंत्र में विकसित होता गया. जिसमें भारतीय मुसलमानों के एक अमीर हिस्से और आस-पास के अमीर मुस्लिम देशों (जो पैन इस्लामिक विचारों के पोशक हैं) की मौजूदगी ने अहम भूमिका अदा की. जो दलितों के संदर्भ में सम्भव नहीं था.
इस पहलू पर इसलिए गौर करना ज़रूरी था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसमें मुसलमानों की स्थिति को दलितों से भी बद्तर बताया गया है, के आने के बाद से मुसलमानों और दलितों की स्थिति के बीच बहुत सपाट तरीके से तुलना करने का ट्रेंड बन गया है. हिंदु धर्म से बाहर के होने के कारण मुसलमानों के ‘शिकायतों’ को हल न कर पाने की वास्तविक और ढ़ांचागत कमजोरियों के बावजूद वोट बैंक का बड़ा हिस्सा होने के चलते उनको अपने साथ रखना और शिकायत करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर देना कथित सेक्यूलर राजनीति का ट्रेंड बनता गया. जिसमें बाबरी मस्जिद के मसले पर ढ़ुलमुल रवैये के चलते कांग्रेस को छोड़ कर आए मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति खड़ी करने वाले कई दलों को मुसलमानों की तरफ से समर्थन भी मिला. लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और अनुभवों और परिस्थितियों ने उनके जेहन को धर्मनिरपेक्षता की वैचारिक परिधि से निकाल कर धर्म की पहलू में अपने ज़ख्म चाटने को छोड़ दिया था.
इसीलिए उस ज़माने में भाजपा की साम्प्रदायिक लहर के खिलाफ खड़े दिखने की मुद्रा बनाने वाले मुलायम को उसने एक सेक्यूलर नेता के बतौर नहीं बल्कि एक ‘मौलाना’ के बतौर स्वीकार किया. जो बाबरी कांड के चलते मुसलमानों में नागरिकीय चेतना (जिसके तहत वह अपनी समस्याओं के हल के लिए देश के राजनीतिक और कानूनी इदारों पर भरोसा करता था) के क्षरण के साथ आए इस खतरनाक वैचारिक बदलाव जिसमें वह मानने लगा था कि कोई ‘मौलाना’ ही उसका रक्षक हो सकता है, को दर्शाता है.
ऐसे राजनीतिक माहौल में वह दल सबसे ज्यादा सेक्यूलर माने जाने लगे जो ज्यादा से ज्यादा संस्थागत तरीके से ‘शिकायतें’ सुन और संयोजित कर सकते थे. इस तरह मुसलमानों की शिकायतें सुनने और शिकायतों की जांच करने की मांग-जांच आयोगों का गठन, उनकी स्थितियों की समीक्षा के लिए कमीटियों का गठन, मुसलमानों में मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनता गया. तो वहीं राज्य और राजनीति के बाहर की शक्तियों के लिए भी मुस्लिमों के सशक्तिकरण के नाम पर यह एक उद्यम बनता गया.
राजनीतिक दलों और गैर राजनीतिक कतारों (एनजीओ और धार्मिक संगठन) को शिकायतें सुनने-सुनाने का खेल कितना रास आता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट (जिस पर अब तक अमल नहीं हुआ) इसका सटीक उदाहरण है. जिसको जारी करने भर से कांग्रेस को सेक्यूलर पार्टी बताते हुये कई धार्मिक-सामाजिक संगठनों ने सोनिया गांधी को बधाई दी थी. जिसका चुनावी लाभ उसे 2009 के चुनाव में हुआ था. तो वहीं कई गैर-सियासी सेक्यूलर संस्थाओं और धार्मिक संगठनों ने इस रिपोर्ट को मुसलमानों के विक्टमहुड मानसिकता को और पुख्ता करने का उपक्रम बना दिया. मसलन, भले ही इसकी सिफारिशों पर अमल के लिए मुस्लिम संगठनों की तरफ से कोई व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन नहीं चला हो लेकिन एक बड़े मुस्लिम संगठन ने मिशन 2017 नाम से (सच्चर कमीटी की रिपोर्ट 2007 में आने से दस साल बाद 2017 तक मुसलमानों के हालात पर) सर्वे का कार्यक्रम चला रखा है. जिसके लिए उसने तमाम शहरों में लोगों की नियुक्ति कर रखी है.
दरअसल, मुस्लिम विक्टमहुड की सामूहिक शिकायती चेतना अपनी तकलीफों की बढ़ती फेहरिस्त और आंकड़े देख कर ठीक उसी तरह संतुष्टी पाती है, जैसे साम्प्रदायिक हिंदुत्वादी चेतना किसी निर्दोष अफजल गुरू की फांसी से. इस विक्टमहुड तंत्र और उसकी सेफ्टीवाल्व बनी शिकायती यंत्रों को जब कोई चुनौती मिलती है या उसकी सीमाओं पर सवाल उठते हैं तब इस तंत्र के रखवाले किस तरह उसका बचाव करते हैं, इसे समझना भी अहम होगा.
मसलन, जहां सेक्यूलर संस्थाएं (एनजीओ) सभी राजनीतिक दलों के साम्प्रदायिक और मुस्लिम-विरोधी होने का सरलीकृत विश्लेषण करके इस मसले पर राजनीतिक हस्तक्षेप को व्यर्थ साबित करने की कोशिश करती हैं तो वहीं सत्ता परस्त धार्मिक संगठन सरकारी ‘टोकेनिज्म’ का बढ़चढ़ कर तारीफ कर उस पर उठने वाले सवालों की गम्भीरता कम करने की कोशिश करते हैं और जब उससे भी सरकारों को राहत नहीं पहुंचा पाते तब सवाल उठाने वालों को ही संदिग्ध बताने की कोशिश करने लगते हैं.
मसलन, बम्बई दंगों की जांच के लिए गठित श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट जब महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने विधान सभा में रखा तब उस पर अमल करने का दबाव डालने के बजाए मुस्लिम संगठनों में इतने पर ही सरकार की तारीफ करने की होड़ मच गयी और मामला वहीं शांत हो गया. इसी तरह आतंकवाद के आरोप में निर्दोष फंसाए गए तारिक़ कासमी और खालिद मुजाहिद (जिनकी हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी गई) को निर्दोष बताने वाली निमेष कमीशन की रिर्पोट को सार्वजनिक कर उस पर अमल करने की मांग के साथ चले रिहाई मंच के ऐतिहासिक धरने (121 दिन) के दौरान सरकार द्वारा जन-दबाव में कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट को स्वीकार करने या विधान सभा सत्र के पहले ही दिन उसे पटल पर रख देने के बाद भी उस पर अमल के लिए जारी रिहाई मंच के धरने को उलेमा तंत्र ने अनावश्यक और सरकार विरोधी बताकर सरकार को बचाने की कोशिश की.
इन तथ्यों की रोशनी में जाहिर है मुसलमानों को विक्टिमहुड मानसिकता से निकाले बिना मुज़फ्फरनगर जैसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं रोकी जा सकती. जो एक लम्बी और जटिल प्रक्रिया है. जो इस समाज को उसके सवालों पर संगठित तरीके से सड़क पर उतारने से शुरू होता है. दूसरे, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शवादी टोटके जो दरअसल साम्प्रदायिक ताकतों के पक्ष में यथास्थितिवाद को बनाए रखने के सबसे घातक हथियार हैं के लिए अब कोई स्पेस नहीं होना चाहिए.
मसलन, इस जनसंहार पर प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए हलफनामे जिसमे उसने मृतकों और घायलों की पहचान उनके धर्म के आधार पर की है पर सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी कि सरकार पीडि़तों की धर्म के आधार पर शिनाख्त न करे और उन्हें नागरिक सम्बोधित करे, साम्प्रदायिक हिंसा की कड़वी सच्चाईयों से भागने जैसा है. क्योंकि इसका राजनीतिक जमां हमेशा साम्प्रदायिक ताकतों के पक्ष में होता है. क्योंकि जब उनके द्वारा आयोजित हत्या कांडों में उनके शिकारों की पहचान सामने आती है तो वही सबसे पहले ऐसे टोटकों से अपनी दरिंदगी छुपाने की कोशिश करते हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसलिए अप्रांगिक है कि दंगों में लोग मारे ही इसलिए जाते हैं कि हमलावर उन्हें नागरिक मानने को तैयार ही नहीं होते. (संघ परिवार के पास तो इसका बाकायदा लिखित सिद्धांत है कि अल्पसंख्यकों को कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है)
इसलिए अगर हमारा लोकतंत्र सचमुच साम्प्रदायिकता से लड़ना चाहता है तो उसकी अदालतों को इन सच्चाईयों को स्वीकार करना ही होगा कि 1984 में सिख मारे गए, कंधमाल में इसाई मारे गए, 1993 और 2002 में मुसलमान मारे गए और हमलावर हमेशा संघ परिवार के प्रभाव वाले साम्प्रदायिक हिंदु थे, जिन्हें सहिष्णुता आधारित धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखने वाले आम हिंदुओं की खामोश हिमायत प्राप्त थी. यह स्वीकारोक्ति )डायग्नोसिस) साम्प्रदायिकता के खिलाफ ईमानदार लड़ाई के लिए सबसे निर्णायक है.
तीसरे – इस जनसंहार ने यह भी दिखा दिया है कि असमान भूमि सम्बंधों का इस्तेमाल जब साम्प्रदायिक फासीवादी शक्तियां करती हैं तब किस तरह की मध्यकालीन हिंसा मुमकिन होती है (ज्यादातर पीडि़त मुसलमान भूमिहीन हैं जो बड़ी जातों के मालिक जाटों के यहां सदियों से एक तरह की बेगारी करते हैं. जिनमें से अधिकतर के मताधिकार का इस्तेमाल जाट खुद करते हैं)
लिहाजा भूमि वितरण और मालिकाना हक के सवाल को हल किये बिना (जो इस कृषि आधारित क्षेत्र में नागरिकीय हैसियत का सबसे निर्णायक पैमाना माना जाता है) ‘मुजफ्फरनगर’ की पुनरावृति नहीं रूक सकती. लेकिन क्या ऐसी पहल क़दमियों के लिए हमारा ‘लोकतंत्र’ तैयार है?
(लेखर रिहाई मंच के प्रवक्ता हैं.)