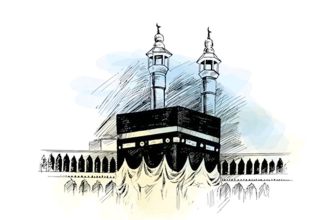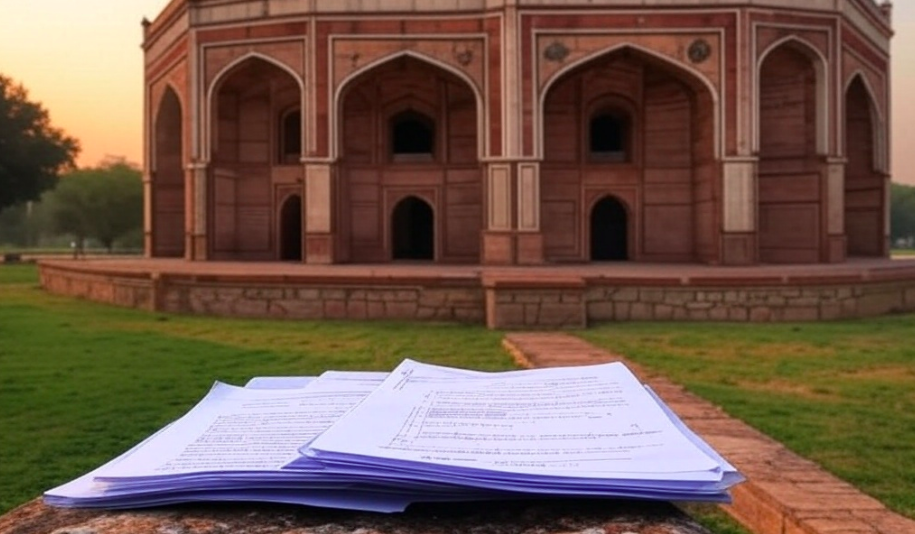By Jaya Nigam
2 फ़रवरी को नेटवर्क ऑफ़ वीमेन इन मीडिया की जामिया के अंसारी ऑडीटोरियम में हुई पब्लिक मीटिंग में जाना हुआ. एक दिन पहले से ही वहां देश भर की महिला पत्रकार, सांस्थानिक और स्वतंत्र दोनों ही, भारतीय मीडिया में महिलाओं की समस्याएं, अनुभव और काम करने के माहौल पर अपने अनुभव साझा कर रही थीं.
बैंगलौर की पत्रकार अम्मू जोसेफ़ जो सालों से इस मुद्दे पर सक्रिय हैं, उनकी पहल पर दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ.
दूसरे दिन यानी 2 फ़रवरी को सार्वजनिक सभा में एक रिपोर्ट की फाइंडिंग पेश हुईं, जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर किए गए शोध के निष्कर्ष थे. इसके बाद एक पैनल डिस्कशन रखा गया, जिसका संचालन स्क्रॉल की पत्रकार कल्पना शर्मा ने किया.
इस पैनल में वायर की एडिटर मोनोबिना गुप्ता, मीटू इंडिया पेज़ की संचालक समेत वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ और अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर भी शामिल रहे. डिस्कशन में लगातार मीटू के ज़रिए उठाए गए मुद्दों पर नई पुरानी महिला पत्रकारों के बीच की असहमतियों पर बात हुई.
ये सामने आया कि भारतीय मीडिया में मौजूद लैंगिक असमानता के जिस माहौल को पुरानी महिला पत्रकार सहज मानकर चलती थीं, उसी असमानता के मुद्दों पर नई पीढ़ी की महिला पत्रकारों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है.
ध्यान रहे कि ये मामला महज़ यौन उत्पीड़न का न होकर असमानता के उस माहौल के बारे में कहा गया जिसका चरम स्वरूप यौन उत्पीड़न या बलात्कार के रूप में महिलाओं को मीडिया संस्थानों के अंदर झेलना होता है.
इस बात को लेकर लगभग पूरे पैनल में सहमति दिखाई दी कि महिलाओं ने अब लैंगिक गैर-बराबरी के माहौल के लिए एक न्यायपूर्ण भाषा इवॉल्व कर ली है, जो जेंडर के मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए पहले ना तो मौजूद थी और ना ही चलन में थी.
नैना ने ये महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित किया कि दरअसल कार्यस्थल पर समान अवसर पाना और यौन हिंसा से दूर बेहतर माहौल पाना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है. जिसे महिलाओं ने भारत में पहचानना, रेखांकित करना और इसके लिए लड़ना बहुत पहले से शुरू किया है और मीटू आंदोलन को इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक कड़ी माना जाना चाहिए.
अमित बरुआ जो बतौर दि हिंदू के संपादक कार्यक्रम में शामिल थे, उन्होंने मीडिया संस्थानों में उच्च पदों पर बैठे लोगों के महिलाओं के प्रति व्यवहार और यौन उत्पीड़न के मामलों से निबटने में इच्छा शक्ति के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ऊपर के लोगों का व्यवहार दरअसल किसी मीडिया ऑफ़िस के अंदर के माहौल को दुरुस्त रखने के लिये सबसे ज़रूरी है. मीडिया में बतौर फ्रीलांसर काम कर रही महिलाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, वो संस्थान के अंदर काम कर रही महिला पत्रकारों के मुक़ाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण और असमान है, उन्होंने इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया.
पैनल में सबसे ज़्यादा मुखर और स्पष्ट रूप से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अपने विचार रखे, जिन्होंने ये बताया कि ये देखना ज़रूरी है कि मीटू आंदोलन के बाद अब सर्वाइवर्स के साथ सिस्टम किस तरह पेश आ रहा है.
उन्होंने बताया कि उनके ऊपर भी डिफामेशन का एक मुक़दमा यौन उत्पीड़न के आरोपी पचौरी के द्वारा लगया गया है, जिससे लगातार जूझते हुए वो बराबर ये महसूस कर रही हैं कि उन सर्वाइवर्स को बैकलैश से बचाया जाना कितना ज़रूरी है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर रख कर यौन उत्पीड़न के सालों पुराने घाव भारतीय समाज के सामने रखे हैं.
उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के सांस्थानिक हमले जो इन सर्वाइवर्स पर हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एकजुट होना मीटू आंदोलन के समर्थकों के लिए कितना ज़रूरी है, इसी बाबत उन्होंने बताया कि मैं भी बोलूंगी नाम से वो कुछ मीटू समर्थक एक लीगल कलेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए फंड जुटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है.
इस पैनल डिस्कशन को संचालित करते हुए कल्पना शर्मा ने कहा कि जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी और ईव टीजिंग जैसे शब्दों का प्रयोग कैसे मीटू जैसे अभियानों में सिमटे अन्य ख़तरों की ओर इशारा करता है कि इसे लैंगिक मुद्दों के ओवरहाइप के बहाने अराजनीतिकरण की ओर ले जाया जा सकता है इसलिए सही परिप्रेक्ष्य में इसे समझना कितना ज़रूरी है.