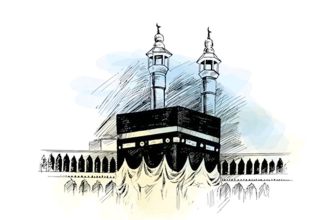Tarique Anwar Champarni for BeyondHeadlines
पूर्व आईएएस टॉपर शाह फ़ैसल ने अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद एक नई पार्टी का गठन किया है. शाह फ़ैसल के इस फ़ैसले का स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे समय में यह फ़ैसला लिया है, जब कश्मीर गर्म तवे की तरह तप रहा है. यह बेहद हिम्मत की बात है जब कश्मीर में पहले से उमर अब्दुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ़्ती की पीडीपी की मज़बूत उपस्थिती है, उसके बावजूद भी क़दम बढ़ाया है.
मैंने फ़ारूक अब्दुल्लाह की जगह उमर अब्दुल्लाह और मुफ़्ती सईद की जगह महबूबा मुफ़्ती का नाम इसलिए लिया है ताकि शाह फ़ैसल जैसे नौजवान को सामने रखकर बात किया जाए. इन दोनों पार्टियों के रहते हुए शाह फ़ैसल के द्वारा पार्टी का गठन करना कई मायनों में सोचनीय है.
ज़ाहिर है यह फ़ैसला एक दिन में तो लिया नहीं गया होगा. इस फ़ैसले तक पहुंचने से पहले वह कई तरह के विचारों से गुज़रे होंगे. कश्मीर की समस्याओं को पहचाना गया होगा. उन समस्याओं का क्रिटिकल एनालिसिस किया होगा. डेमोग्राफिक एवं भौगोलिक परिस्थिति को समझने का प्रयास किए होंगे. फिर उसी आधार पर लोगों से संपर्क किया होगा. उनके सामने उपरोक्त सभी बातों पर चर्चा हुई होगी. फिर कुछ लोगों को तैयार करके एजेंडा तय पाया होगा. एजेंडा की पूर्ति के रास्ते में आने वाली दिक़्क़तों पर मंथन के बाद उन दिक़्क़तों से निपटने के तरीक़ों पर चर्चा हुई होगी. फिर जाकर पार्टी बनाने के फ़ैसला तक पहुंचे होंगे. अब जब पार्टी बन गया है तब जाकर अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने के लिए एजेंडा के साथ ज़मीन पर काम करना शुरू करेंगे.
आज भारत की मुस्लिम राजनीति अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रही है. मैं जब मुस्लिम राजनीति की बात कर रहा हूं तो इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं मुसलमानों की अलग राजनीतिक गिरोहबंदी या राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं. मेरी असल चिंता सेकूलर दलों में लगातार कम हो रही प्रतिनिधित्व को लेकर है.
सीएसडीएस की रिपोर्ट के अनुसार लोकतान्त्रिक संस्थानों में किसी भी अन्य समुदायों से अधिक भागीदारी मुसलमानों की है, मगर उसके अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है. हम मुस्लिम राजनीति के कमज़ोर होने के जो फैक्टर हैं, उसको ढूंढने में आज भी असफल हैं. हम बड़ी चालाकी से भाजपा और आरएसएस पर आरोप मढ़कर निकल जाते हैं और बाक़ी के जो कुछ लोग बचते हैं वह मुस्लिम धर्म-गुरुओं को गाली देकर काम चला लेते हैं.
यदि बिहार के संदर्भ में देखा जाए तब एक समय था जब किशनगंज, अररिया, पुर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), सीवान, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया इत्यादि ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे, जहां से मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौक़ा मिलता था. कुछ जीतकर भी आते थे और कुछ अपनी मज़बूत उपस्थिती भी दर्ज कराते थे.
लेकिन अचानक से उम्मीदवारों की संख्या कम होने लगी. इसके पीछे कई कारण है. पहला, जो प्रभाव वाले पुराने नेता थे वह इस दुनिया से चल बसे. दूसरा पुराने प्रभाव वाले कुछ नेता जो बचे हुए हैं उनका अपने ही समुदाय में प्रभाव कम हो चुका है. तीसरा परिवारवाद या वंशवाद से निकलकर आने वाले नेता ज़मीनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं जिस कारण समाज में अधिक प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं. चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण और असल समस्या की जड़ है वह नए नेतृत्व का उभार नहीं हो पाना है.
मुसलमानों में एक लंबे समय से नई नेतृत्व का उभार नहीं हो पाया है. आज भी वही लोग नेतृत्व कर रहे हैं जो परिवारवाद से होकर राजनीति में पहुंचे है या फिर किसी राजनीतिक दल के रहमो-करम पर राजनीति कर रहे हैं.
विकल्प नहीं मिलने के कारण मुसलमान प्रतिनिधित्व के नाम पर कुछ नेताओं को मजबूरी में भी ढ़ो रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विकल्प खड़ा भी कैसे किया जाए? प्रतिनिधित्व का स्थान इतना खाली है कि मुसलमान निगाह टिकाए बैठे हैं. साथ ही कुछ नए लोग जो प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं उसको आम मुसलमान स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है. यहां पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आख़िर यह सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है?
सामंजस्य नहीं बन पाने के पीछे कई कारण हैं. पहला महत्वपूर्ण कारण है कल तक विश्वविधालय से उभरने वाले छात्र नेता, शिक्षक या एनजीओ से उभरे लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा समाज के लोगों के बीच आकर करते थे. मगर आज विश्वविधालय की राजनीति में सक्रिय नेता या एनजीओ से उभरे लोग सेमिनार रूम और शहरी एक्टिविज़्म तक सिमट कर रह गए हैं.
अख़बार की सुर्खियों में रहने के लिए समाज से लगभग रिश्ता कटा हुआ होता है. मगर विश्वविधालयों के सेमिनार रूम में बैठकर समाज की समस्याओं पर चर्चा करने के कारण आम जनमानस से जुड़ाव नहीं हो पाता है. यह जो अर्बन-सेंट्रिक राजनीति या एक्टिविज़्म है वह गांव-ग्राम के लोगों पर असर नहीं डाल पाता है.
सेमिनार रूम में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा ज़रूर होती है. अर्बन-सेंट्रिक नेताओं या एक्टिविस्टों की सबसे बड़ी समस्या है कि जब वह समाज के बीच आते हैं तब वह समाज के मूल समस्याओं पर चर्चा नहीं करके मुसलमानों के धार्मिक रीति-रिवाजों और धार्मिक नेताओं पर चोट करना शुरू करते हैं. हमारा समाज अभी इतना उदार नहीं हुआ है कि धार्मिक रीति-रिवाजों और धार्मिक नेताओं पर किए गए हमलों को बर्दाश्त कर सके.
दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो लोग प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं वो इतने अर्बन-सेंट्रिक और तथाकथित बौद्धिकता का परिचय देने लगते हैं कि आम जनता ऐसे नेताओं को प्रतिनिधित्व देने से घबराती है. ऐसी स्थिति में यही होता है कि राजनीति में क़दम रख चुके लोग अलग-अलग दलों से सांठ-गांठ करके राजनीति शुरू करते हैं. नेटवर्किंग, लॉबी या धन इत्यादि देकर राजनीतिक दल या फिर दल के मुखिया द्वारा मनोनीत होने के बाद सदन पहुंचते हैं. लॉबी, नेटवर्किंग और पैसे इत्यादि देकर जो सदन पहुंचते हैं वह अपने दल और दल के मुखिया के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं. जिस कारण आम जनता के प्रति उनका जुड़ाव कम हो रहा है.
जनता और नेता दोनों के बीच की इस दूरी को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है. उदाहरण के रूप में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का जब उभार हुआ तब मुस्लिम एक्टिविस्टों ने इनके कार्यक्रमों को भारी संख्या में आयोजित किया और मुसलमानों का भारी जनसमर्थन प्राप्त हुआ. मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने समाज से ऐसे ही कुछ लोगों को ढूंढकर और जनसमर्थन देकर प्रोमोट करे ताकि प्रतिनिधित्व का अभाव नहीं रहे. यदि मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं तब ज़ाहिर सी बात है कि जो नेटवर्किंग, लॉबी या पैसे की बल पर मनोनीत होकर आएंगे वह अपने दल और दल के मुखिया के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे.
यदि कल कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी या हार्दिक पटेल पर उनकी पार्टी किसी भी प्रकार का दबाव बनाना चाहेगी उससे पहले एक बार इन नेताओं को मिलने वाले जनसमर्थन के बारे में ज़रूर विचार करेगी. मनोनीत होकर आने वाले लोग हमेशा दल और दल के मुखिया के एहसान के नीचे दबा रहेगा, इसलिए ऐसे नेताओं से समाज हित के बारे मे सोचना आम जनता की बेवकूफ़ी होगी.
कश्मीर की राजनीति को शेष भारत की राजनीतिक वातावरण में फिट करना उचित नहीं है. मगर राजनीतिक इच्छा-शक्ति को साबित करने के लिए शाह फ़ैसल का उदाहरण पेश किया जाना भी ज़रूरी है. डॉ शाह फ़ैसल ने अपने पूरी ज़िन्दगी रिस्क ही लिया है. मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद मेडिसिन में कैरियर नहीं बनाकर सिविल सर्विस की तरफ़ बढ़ गए. सिविल सर्विस में दस वर्ष नौकरी करने के बाद त्यागपत्र देकर राजनीति की तरफ़ क़दम बढ़ाया. वह भी एक ऐसे राजनीतिक माहौल में जहां बर्फ होने के बावजूद भी माहौल हमेशा आग की तरह होता है.
विश्वविधालय की राजनीति या एनजीओ से निकलकर राजनीति शुरू करने वाले लोगों को डॉ शाह फ़ैसल की तरह समाज की जड़ों को समझकर रिस्क लेना पड़ेगा. तभी किसी प्रकार के नेतृत्व के उभार या प्रतिनिधित्व को बढ़ाए जाने की कल्पना की जा सकती है.
(लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), मुम्बई से पढ़े हैं. वर्तमान में बिहार के किसानों के साथ काम कर रहे हैं.)