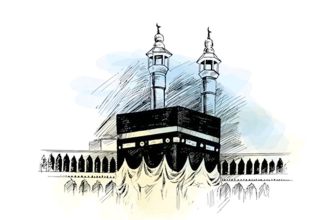By Prof. Mohammad Sajjad
“बेगूसराय (बिहार) से मुस्लिम उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करना मुसलमानों के वजूद का सवाल है!”
इस तरह की बातें दिल्ली के एक मशहूर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में कम्यूनिकेशन का एक उज्ज्वल, होनहार मुस्लिम छात्र ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में कही. इस बात ने मेरी घबराहट को बढ़ा दिया. क्या यह एक अपवाद है? या शिक्षित युवा मुसलमानों के ग़ौरतलब हिस्से की यह अंदर की आवाज़ है? यह सवाल मैंने अपने आप से पूछा.
बाद में मैंने अपने इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू कर दिया. सोशल-मीडिया ने स्पष्ट रूप से मेरी निराशा का समर्थन किया. मैं इस बात से चिंतित हो गया कि आख़िर भारतीय लोकतंत्र जा कहाँ रहा है, जहां निराशाजनक रूप से बांटने वाली पहचान की सियासत तेज़ी से हमारे राजनीति और समाज में घुस रही है? काफ़ी पढ़े-लिखे मुस्लिम युवा कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं, हालांकि इस हिस्से के बहुत सारे लोग लोकसभा में मुसलमानों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के नाम पर ऐसा कर रहे हैं.
इसके बाद मैंने उनसे पूछा —अगर आप सभी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के उम्मीदवार को ही पसंद करते हैं, तो उनके मुसलमान होने पर इतना ज़ोर क्यों दिया जाना चाहिए? उनमें से कुछ ने कन्हैया को मुसलमानों का समर्थन वापस लेने की धमकी भी देते रहे, क्योंकि गुजरात के दलित नेता, जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया के लिए प्रचार करने के बाद, राजद के मुस्लिम उम्मीदवार गैंगस्टर-विधायक (हत्याओं के लिए दोषी) की पत्नी हिना शहाब के ख़िलाफ़ सीवान में सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने गए थे.
यह और भी अजीब था. किसी गैंगस्टर की पहचान सिर्फ़ एक गैंगस्टर के रूप में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों इन मुसलमानों को एक गैंगस्टर को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह इन मुसलमानों को एक पूरे समुदाय के रूप में पेश करना चाहिए? वे ऐसे सभी सवालों से बचते हैं.
दूसरे मुस्लिम भी हैं, जो अपने तर्क को रखते हुए मानते हैं कि वामपंथी पार्टियां, मुसलमानों को सत्ता के ढांचे और प्रक्रियाओं में उचित हिस्सेदारी दिए जाने के मामले में ज़्यादा ख़तरनाक हैं. वे ममता बनर्जी से पहले पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चा शासन द्वारा मुस्लिमों को मिलने वाली सत्ता में हिस्सेदारी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल और वहां सच्चर रिपोर्ट के साथ होने वाले बरताव को लेकर सही ही तो कहते हैं.
एक तर्क तो यह भी दिया जाता है कि कन्हैया कुमार जैसे किसी भूमिहार को किसी मुसलमान की क़ीमत पर महागठबंधन की तरफ़ से तरजीह क्यों दिया जाए? ऐसा कहते हुए वे दो सच्चाई नज़रअंदाज़ कर जाते हैं :1952 के बाद ज़्यादातर भूमिहार सासंद को ही वहां से चुना गया है; केवल एक बार, 2009 में एक मुस्लिम उम्मीदवार (NDA का) निर्वाचित हुआ था.
दिलचस्प बात यह है कि ये मुसलमान यह भूल जाते हैं कि मधुबनी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर जैसी सीटों को अपेक्षाकृत अधिक मुस्लिम वोट मिले हैं, और इनमें से कुछ ने मुसलमानों को कई बार चुना भी है, इसके बावजूद महागठबंधन ने इसे ग़ैर-मुसलमान उम्मीदवारों को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है.
ये सांप्रदायिक मुसलमान इन सीटों पर मुसलमानों के वजूद पर किसी तरह का ख़तरा नहीं चाहते हैं. इन्हें अपनी संभावना से बेख़बर रहना मंज़ूर नहीं हैं. क्या होगा, अगर सभी हिंदू केवल हिंदुओं का चुनाव करने के लिए एकजुट हो जाए? पर्याप्त मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर ज़ोर देते हुए, उनमें से ज़्यादातर ने मुसलमानों के अज़लाफ़ और अरज़ाल समुदायों के और भी कम प्रतिनिधित्व की अनदेखी करते हुए ही अपने प्रतिनिधियों को चुना है.
दिलचस्प बात है कि एक बार जब राजद के मुस्लिम उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, और सीपीआई को गठबंधन में नहीं लिया गया, तो उसी नवोदित मुसलमान पत्रकार ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह इच्छा भी जताई कि कन्हैया को ध्रुवीकरण को लेकर भाजपा के आग उगलने वाले कुख्यात नेता, गिरिराज सिंह के ख़िलाफ़ भूमिहार वोटों में कटौती करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए ताकि राजद के मुस्लिम उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो सके. हालांकि, जब उन्हें और उन जैसे लोगों को यह पता चला कि कन्हैया को मुस्लिम वोट भी मिल सकता है, तो उनके पराजय और और हताशा के अहसास उनके सोशल साइट्स पर छलक आया. उन्होंने उन सभी “मामूली संख्या वाले” मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने तीख़े हमले किए, जिन्होंने कन्हैया का बढ़-चढ़कर समर्थन किया.
सोशल-मीडिया पर ये बहस हमारे समाज और राजनीति में आ रही जातीय-आधारित श्रेणीबद्ध दमनकारी पदानुक्रम, बढ़ती धार्मिक कट्टरता, बहुसंख्यक के हमले, अल्पसंख्यक उत्पीड़न, प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता, मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व आदि गड़बड़ियों को सामने लाती है.
समस्या यह है कि दबाव डालती इन समस्याओं का जवाब भारत ने पहचान-आधारित अंधराष्ट्रवादी राजनीति के दिया है. इस प्रकार, इस तरह के किसी पहचान वाले नाममात्र के प्रतिनिधित्व को उसके सशक्तिकरण के एक पर्याय के रूप में देखा जाता है. कहने की ज़रूरत नहीं कि यह सिर्फ़ एक विचित्र और भ्रम पैदा करने वाला सशक्तिकरण है. यह उन कई कारणों में से एक है कि भारत को इस तरह के भयानक बहुसंख्यकवाद से सामना करना पड़ता है.
यह निराशावाद का दौर है. 1960 और 1970 के दशक के ठीक उल्टा, इस दौर में युवाओं को आजीविका और नागरिक स्वतंत्रता के ठोस मुद्दों को लेकर सड़क पर चलने वाले आक्रामक लोकप्रिय आंदोलन के माध्यम से मुक्ति की राजनीति के लिए रोल मॉडल के रूप में कोई नेतृत्व नहीं मिला है.
यहां तक कि बिहार के कुछ हिस्सों में क्रांतिकारी वामपंथियों को छोड़कर, वामपंथी भी अपने रास्ते से भटक चुके हैं. समाजशास्त्री प्रोफ़ेसर आनंद कुमार अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय राजनीति में वामपंथ की कुछ न्यूनतम उपस्थिति ठीक वैसे ही बिलकुल आवश्यक है, जैसे खाने में नमक; इसकी कमी और अधिकता, दोनों खाने का स्वाद बिगाड़ देते हैं.
ऐसे हालात में, एक ग़रीब किसान, लेकिन ग्रामीण बेगूसराय के एक उच्च जाति के हिंदू परिवार से आने वाले कन्हैया, जेएनयू के छात्र-कार्यकर्ता के रूप में सामने आए, जो कि कट्टर देशभक्ति और दमनकारी शासन का शिकार हो रहे थे. उन्होंने इसका प्रतिकात्मक प्रतिरोध बहुत ही बहादुरी के साथ किया. उन्होंने एक तरह से कॉरपोरेट नियंत्रित शासनों के दौर में प्रतिरोध वाली छात्र और युवा राजनीति को फिर से सामने लाने में मदद की. यह उनके साथ प्रतिध्वनित हुआ और यह गूंज, जाति, धर्म और लिंग की काट के रूप में सामने आती दिखाई पड़ी.
मेरे विचार से कन्हैया से पहले, पिछले कुछ दशकों में जेएनयू के कई अन्य वामपंथी छात्र कार्यकर्ता, बहुत व्यापक बौद्धिकत, नज़रिया वाले, सफल अभिव्यक्ति और वाककुशल थे. चंद्रशेखर तो कन्हैया से बहुत आगे थे. लेकिन चंदू को मार्च 1997 में सीवान में शहाबुद्दीन के शूटरों ने कथित रूप से हत्या कर दी थी. उन व्यापक मूल्यों की तुलना में, आज जबकि राज्य अधिक दमनकारी और प्रतिरोध कमज़ोर प्रतीत होता है, तब कन्हैया का महत्व और बढ़ गया है.
युवाओं को उपभोक्तावाद की पीड़ा हरण करने वाली दवाएं परोसी जा रही हैं. कॉरपोरेट के स्वामित्व वाले टीवी समाचार चैनलों ने घोर निष्ठा से काम किया है और झूठ को प्रचारित करने में उनकी भूमिकाएं घातक रूप से ख़तरनाक हो गई हैं. दलितों, मुसलमानों और जनजातियों जैसे कमज़ोर पहचान वाले कैंपस, शिकार करने वाले शासन के निशाने पर आ गए हैं. पुलिस और जांच एजेंसियां, ख़तरनाक सत्ताधारी पार्टी की बदले की राजनीति के घातक रूप के अधीन हो गए हैं.
ऐसे भयावह परिदृश्य में कन्हैया अपनी सीमाओं के बावजूद प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सामने आया है. मुसलमान नौजवानों के कई वर्गों की नज़र भी उन पर हैं. हमारी नज़र में इसकी तुलना में राजद के मौजूदा मुसलमान उम्मीदवार की साख ज़ाहिरी तौर पर कमतर है. वह मुसलमानों की लिंचिंग और हिरासत में हो रही मौत पर ख़ामोश थे. राज्य के उच्च सदन में विधान पार्षद होने के बावजूद उनका योगदान शायद ही कुछ रहा हो. अगर वास्तव में उनका योगदान कुछ है भी तो उनके समर्थक उन योगदानों का स्पष्ट तौर पर रखने और प्रचार करने में सक्षम नहीं हैं. लेकिन, संप्रदायवादी मुसलमान तब भड़क उठते हैं, जब उनके सह-धर्मी को पहचान-आधारित चुनावी प्राथमिकताओं को उसे धता बताते हुए देखा जाता है.
वास्तव में, राजद के तेजस्वी यादव ने भी भगवा ब्रिगेड के हाथों मुसलमानों के ऐसे उत्पीड़न को लेकर बहुत देर से और बेहद अनिच्छुक तरीक़े से प्रतिक्रिया दी. समझदारी के साथ उन्होंने संस्थागत समर्थन भी नहीं दिया. बिहार में राजद-कांग्रेस के अन्य बड़े मुस्लिम नेता की सामने नहीं आए. यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती और उनके मुस्लिम नेताओं का भी है. कन्हैया के ठीक उल्टा, इनमें से कोई भी सड़क पर नहीं उतरा.
पहचान की बीन बजाने और लोगों को ठोस मुद्दों को न उठाने देने और मतदाताओं को अपने विधायकों के प्रदर्शन को लेकर किसी तरह का सवाल नहीं करने देने की दक्षिणपंथी राजनीति, हिन्दू और मुसलमान, दोनों की संगठित जातियों के बीच तेज़ी से प्रतिस्पर्धा करती दिखाई पड़ती है.
यहां तक कि सामाजिक न्याय की राजनीति अब कुछ प्रमुख जातियों के आधिपत्य तक सिमट गई है. भयावह बहुसंख्यकवाद ने इन ताक़तों को अपना पारंपरिक समर्थन का आधार दे दिया है. स्थानीय निकायों के चुने गए मावालियों जैसे प्रतिनिधि विधायक बनने के लिए इन विभाजनकारी लामबंदी का सहारा लेते रहे हैं. ग़ैर-पहचानवादी, ठोस सामाजिक-आर्थिक वाले आजीविका जैसे मुद्दों पर लोगों को लामबंद करने की तुलना में यह एक आसान रास्ता है.
इस प्रकार कन्हैया के लिए समाज के हर हिस्से की लामबंदी और समर्थन सही मायने में पहचान-आधारित घृणा से भरी हुई, सामाजिक रूप से विभाजनकारी राजनीति के ख़िलाफ़ सड़क पर हो रही आक्रामक लामबंदी वाली आज़ादी की राजनीति को फिर से परिभाषित करने और उसे मज़बूत करने की दिशा में एक कोशिश है. एक व्यक्ति या राजनेता के रूप में कन्हैया, आने वाले दिनों में लंबे समय तक क़ायम रहे या नहीं, लेकिन आज कुछ तो ऐसा है, जिसका वह प्रतीक है.
अपने प्रतिनिधियों को चुनने वालों को यह जताने की ज़रूरत है कि निराशा के इस दौर में आशा की ऐसी कई गलियों का पता मालूम किया जा सकता है, जो हमें उम्मीद से मुक्ति और सशक्तीकरण के ज़रूरी राजपथ की ओर ले जाएगी.
हर सीट इतना भाग्यशाली नहीं है कि उसे भरोसेमंद विकल्प मिल सके. बेगूसराय के हिंदुओं और मुसलमानों को पहचान की इस राजनीति के ख़िलाफ़ मुखर होकर बताने की ज़रूरत है कि नींद में सोये शहर के आस-पास और बाहर की दुनिया के लिए उम्मीद का एक बड़ा पैग़ाम है.
विगत औपनिवेशिक और प्रारंभिक स्वतंत्रता के दौर में बेगूसराय वाम-नेतृत्व वाली आक्रामक किसान राजनीति का केंद्र था. इसके बाद बेगूसराय ने अपने उस दर्जे को खुद ही खो दिया, क्योंकि अपने कल्पनाशीलता को वह आगे नहीं बढ़ा सका; धीरे-धीरे मिटता गया, क्योंकि जाति, भूमि, साथ ही वर्ग आधारित उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने के लिए इसके पास कोई संकल्पना रह नहीं गई थी. पहचान को लेकर असुरक्षित रहने वाले मुसलमानों के रूप में, इन्हें किसी जी-हुजूरी करने वाले दास और मुंह में दही जमा कर नहीं बोलने वाले प्रतिनिधि के बजाए एक मुखर और साफ़-साफ़ बोलने वाला प्रतिनिधि मिलेगा. पसंद तो उनकी होगी! चाहे ‘मुस्लिम राजनीति’ को फिर से परिभाषित किया जाए, इसे अल्पसंख्यकवाद से आगे ले जाएं. यही बहुसंख्यकवाद का विरोध को आगे ले जाने का एक तरीक़ा है. मुस्लिम और हिंदू नेताओं को यह एहसास होना चाहिए कि विभाजनकारी ध्रुवीकरण का मार्ग आसान करने के बजाए नागरिकता के मुद्दों को लेकर सड़क पर होने वाली आक्रामक लामबंदी ही उन्हें प्रतिबद्ध नेता बना सकती है.
यह संभवतः भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए तभी शुभ है, जब बेगूसराय हिन्दू और मुसलमान दोनों ही की सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी राजनीति को रौंद दे और बाक़ी बिहार और हिन्दुस्तान को ख़ुद को एक ज़रूरी अनुकरणीय रोल मॉडल बनाने के लिए प्रेरित करे.
क्या ऐसा हो पाएगा? इस सवाल के जवाब में ही संपूर्ण संस्कृति और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व वाली सभ्यता के रूप में भारत का भविष्य निहित है.
(प्रोफ़ेसर मोहम्मद सज्जाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में एडवांस स्टडी सेंटर में हैं और दो इन पुस्तकों के लेखक हैं: Muslim Politics in Bihar: Changing Contours (Routledge, 2014/2018 reprint) और Contesting Colonialism and Separatism: Muslims of Muzaffarpur since 1857.)