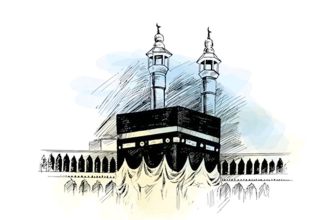Firdous Azmat Siddiqui for BeyondHeadlines
रस्म व रिवाज कभी भी किसी मज़हब का हिस्सा नहीं रहा. समाज का अटूट हिस्सा ज़रूर कह सकते हैं. और जो चीज़ समाज का हिस्सा बन जाती है उसे ख़त्म करना कभी आसान नहीं रहा. पटाख़ेबाज़ी भी उनमें से एक है. शायद ही किसी मज़हब की अहम किताबों में इसका ज़िक्र रहा हो, पर ये सदियों से होता रहा है…
अगर हम मुस्लिम क़ौम की बात करें तो शबे-बारात जो रमज़ान से पन्द्रह दिन पहले की शब (रात) में होती है, बहुत अहम रात है. पूरी रात याद-ए-इलाही में जागने की रात है. कहा जाता है कि इस रात मुर्दों की रूह घर आती है. इसलिए इस रात अच्छा खाना बनाकर फ़ातिहा करके ग़रीबों में तक़सीम करने से मुर्दे की रूह को तस्कीन होती है. साथ ही औलादें अपने बुज़ुर्गों की क़ब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़े और रोशनी करें तो उन्हें इसका सवाब मिलेगी…
इस तरीक़े से शबे-बारात एक बहुत ख़र्च वाला त्योहार बन गया. सारे दिन घर की औरतें तरह-तरह के हलवे बनाती हैं, शाम को पूरा खाना. हलवा व फल के साथ फ़ातिहा होती है. फिर घर के मर्द क़ब्रिस्तान फ़ातिहा पढ़ने जाते हैं, वहां अगरबत्ती व रोशनी का इंतेज़ाम करते हैं. और ऐसा माना जाता है (जैसा कि मुझे बचपन में बताई गई है) कि उस दिन जब कोई मुर्दे के रिश्तेदार नहीं आता तो दूसरे मुर्दे उनको तंज़ कसते हैं. हालांकि मुझे नहीं लगता कि मरने के बाद कोई किसी को तंज़ करता होगा.
लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यह रिवाज शायद इसलिए चला ताकि उनकी औलाद कभी अपने बुज़ुर्गों को भूलने न पाए. बूज़ुर्गो को याद करने में कोई गुरेज़ भी नहीं, पर परेशानी तो तब होती है जब वो किसी समाज का अटूट हिस्सा हो जाए.
ऐसी कई रस्में हैं, जो मुस्लिम समाज का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. मोहर्रम में ढ़ोल-नगाड़े, रोशनी, दरिया की इबादत, घर के ताख़ पर कुछ पत्थर या फूल वगैरह रखकर दिया व अगरबत्ती जलाना, बुज़ुर्गों की मज़ार पर अक़ीदत के फूल चढ़ाने तक बात समझ में आती है. पर वहां धागा बांधकर मन्नत मांगना, बाबा की मज़ार में सजदा करना, मुरादों की दरख्वास्त देना, कलीयर शरीफ़, रूड़की की मज़ार पर तो यह रिवायत है कि बाक़ायदा मुरादों की पूरी फ़हरिस्त के साथ बाबा के नाम पर ख़त लिखकर गूलर के पेड़ से नारों में बांध देते हैं, इस यक़ीन के साथ कि यह ख़त बाबा पढ़ेंगे और उनके मुद्दों को ख़ुदा की बारगाह में रखेंगे. पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ़ तो पंच पीरों की इबादत सदियों से चली आ रही है. शेख़ सद्दों की मज़ार पर ज़िंदा घूमते बिच्छुओं को हाथ पर चलाना और बिच्छू न काटे तो मुरादों की पूरी होने की अलामत. ख़ासतौर पर ऐसी औरतें जिनकी औलाद न हो, माना जाता है कि वहां ज़ियारत करने पर औलादमंद हो जाती हैं.
किछौछा शरीफ़ (बहराईच) और भुलई का पुरा (फुलपुर, इलाहाबाद) की मज़ार पर औरतों को हाल आना जो कि माना जाता है कि भूत का साया है और बाबा की बारगाह में ठीक हो जाएगी. ख़ासतौर पर पूरे बदन तोड़कर झूमना और मुजावरों के हाथ बाल पकड़-पकड़ कर खींचना. देखने वालों की रूह कंपकंपा दे, पर शायद ही ऐसी औरतों के सरपरस्त कभी उन्हें डॉक्टर या मनोवैज्ञानिकों को दिखाने के बारे में सोचते हों. कई बार तो ऐसे साये और बाबा से त्रस्त बच्चियों की मौत तक हो जाती है और यह ख़ौफ जड़ जमा लेता है कि देखो बाबा ने कहा था मैं इसको लेकर रहूंगा और उसकी जान लेकर रहे.
लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये सारे बाबा ज़्यादातर लड़कियों पर क्यों? भूत आसेब क्या मर्द से डरते हैं?
ज़ाफराबाद, जौनपुर जिसे कभी शिराज-ए-हिन्द (पूरब का ताज) कहा गया. सदियों से सूफियों की जमघट की जगह रहा. शेख़ सदरूद्दीन, हाजी हरमैन शाह सुहरावर्दी जिन्हें बादशाह फिरोज़ शाह ने चिराग़-ए-हिन्द का लक़ब दिया था. बावजूद इसके कि सुहरावर्दी सिलसिले में उर्स और क़व्वालियों का कोई चलन नहीं था. उनके ख़ानकाह की रिवायत के हिसाब से सिर्फ़ ईद-उल-अदहा के एक दिन पहले हज की नमाज़ पढ़ी जाती है जिसकी इमामत शाह हरमैन के खानदान के मर्द वारिस ही कर सकते हैं. पर वक़्त गुज़रने के साथ तक़रीबन पिछले बीस पचीस सालों से वहां हज की नमाज़ के दिन से तीन दिन तक सालाना उर्स की रिवायत क़ायम हो गई है, जबकि सूफ़ी सिलसिले में उर्स किसी सूफ़ी की विलादत के जश्न और उनकी तालीम को आगे ले जाने के तौर पर होता है. फिर भी शाह हरमैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ हर साल उर्स की रिवाययत और उन रिवायतों का ख़ास तवज्जो ग़ैर मुस्लिम औरतों का दरगाह से लगी नीम के पेड़ पर नाणा बांधना, थाली सजाकर आरती देना अपने आप में बड़ा रोचक मंज़र होता है. जहां एक तरफ़ दो क़ौमों के बीच विरोधभास बढ़ रहा है. ख़ासतौर से यह विरोधाभास औरतों के मेलजोल को रोकने में ज़्यादा नज़र आता है, वहां प्यार व अक़ीदत का ऐसा मंज़र कि एक तरफ़ क़व्वाली और फ़ातिहा ख्वानी चले, दूसरी तरफ़ हमारी दूसरी सह-बहने थाली और दिया की रोशनी से बाबा को अपना अक़ीदत पेश करें, ऐसा मंज़र बहुत कम ही देखने को मिलता है.
उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहर में सिकन्दरा क़स्बा, शहर या गांव का पाया जाना और वहां ग़ाज़ी मियां की मज़ार होना और हर इत्तेवार को ग़ाज़ी मियां की मज़ार पर गैर-मुस्लिम औरतों की अपने मज़हबी अक़ीदे के हिसाब से अक़ीदत पेश करना जिसमें सफ़ेद मुर्गे को चढ़ाना अहम होता है.
एक ख़ास बात यह है कि हिन्दुस्तान की ज़्यादातर रस्म व रिवाज को चलाने वाली औरतें हैं, जिनका इस्लामिक इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है. जिनका उन्नीसवीं सदी के बीच में अलग-अलग तहरीकों ने एतराज करना शुरू किया और 1857 के बाद का दौर वो दौर है कि जितना सनातनी धर्म का हिन्दूकरण होना शुरू हुआ उतने ही ज़ोर-शोर से हिन्दुस्तानी मुसलमानों का इस्लामीकरण भी. और फिर यहीं से रस्म रिवाजों पर सवाल उठने शुरू हो गए. और ये वही वक़्त था, जब हिन्दुस्तान में मुसलमानों के दो अहम फ़िरक़ों का उरूज़ भी शुरू हुआ —वहाबी व बरेलवी.
वहाबी तहरीक का हिन्दुस्तान में संगठित करने का काम सैय्यद अहमद बरेलवी ने 19वीं सदी के शुरूआती दौर में किया. पर इसे एक विकसित सोच के तौर पर अशरफ़ अली थानवी ने नई दिशा दी. ख़ासतौर पर उनकी मशहूर किताब बेहिश्त-ए-ज़ेवर जिसे 20वीं सदी के शुरूआती दौर से घर-घर में पाया जाना ज़रूरी हो गया, जिसमें वो सारी रेसिपी थी कि किस तरह मुस्लिम औरतों पर ज़िम्मेदारी है कि बदहाल होती क़ौम को एक अच्छी और तरबियत याफ़्ता औलाद बनाएं. इस किताब में उन तमाम रस्म-रिवाज़ो पर ख़ूब हमला है और ऊपर बताए गए हर रिवायत को बिद्दत कहा गया.
वहाबी तहरीक के साथ ही बरेलवी तहरीक का आग़ाज़ हुआ. दोनों का सबसे अहम फ़र्क क़ुरान और हदीस की अहमियत को लेकर है, जहां वहाबी तहरीक सिर्फ़ ख़ालिस क़ुरान के हिसाब से चलने की वक़ालत करता है तो बरेलवी सेक्ट में क़ुरान के साथ हदीस और सहाबा के रिवायत की बहुत अहमियत थी. ख़ासतौर पर ये पूरा बरेलवी सोच सूफ़ियों को बहुत अहमियत देता है. साथ ही हिन्दुस्तान के उन रिवाजों को बहुत अहमियत देता है जो सदियों से हिन्दू-मुस्लिम के मिलने से मिली जुली तहज़ीब की बात करता है. शायद यही वजह रही कि बरेलवी फ़िरक़ा का असर सेंट्रल यूपी को पार करके पूर्वी हिन्दुस्तान की तरफ़ ज़्यादा मज़बूत रहा है. जैसे जैसे पूरब की तरफ़ बढ़ेंगे यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन औरत हिन्दू है और कौन मुस्लिम?
हिन्दुस्तान की तक़रीबन डेढ़ सदी से चल रही इस फिरक़ापरस्ती और इस्लामीकरण की जद्दोज़हद ने अब जाकर रंग लाना शुरू किया. और इस क़वायद में रस्म व रिवाजों पर ख़ूब हमले हुए, जो शायद गंगा-जमुनी तहज़ीब के प्रतीक थे. इसका सबसे ज़्यादा असर मुस्लिम औरतों पर हअा. उनके कपड़ों पर, उनके रिवाजों पर, परदा, और सबसे ज़्यादा त्योहारों का ग़ैर-इस्लामी तरीक़े से मनाने को लेकर जिसमें शबे-बारात और मुहर्रम अहम रहें.
गत 10 सालों में अब शायद ही दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाक़ों में पटाखों की आवाज़ आए जबकि हमें आज भी याद है कि हमारे बचपन में इस क़दर पटाखों के शोर होते कि एक दूसरे की आवाज़ न सुनाई देती. पर अब यह बिद्दत हो गया है और इसे आम मुसलमानों ने क़बूल भी कर लिया है. जबकि दूसरी तरफ़ दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद न तो सरकार और न ही सिविल सोसाइटी पटाखों की आवाज़ पर कंट्रोल कर पाई. सच तो ये है कि आतिशबाज़ी में पहले से ज़्यादा बढ़ोत्तरी हुई है.
हिन्दुस्तान में मज़हब का हर काम में बड़ा अहम रोल होता है. शायद दिवाली के पटाखों को भी मज़हबी इदारों के फ़तवे की दरकार है, वर्ना पटाखों का चलन ही मुस्लिम के आने के साथ शुरू हुआ और दिवाली रामायण की परम्परा के हिसाब से हज़ारों साल से चली आ रही थी तो शर्तिया उसको मनाने का अंदाज़ आतिशबाज़ी नहीं रही होगी जो कि मुग़लों के साथ आई. कहने का मतलब यह है कि त्योहरों से जुड़े हुए रस्म व रिवाज दरअसल किसी धर्म का अभिन्न अंग नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही रिवाजों का एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों के मिलने जुलने और सीखने से शुरू हुई है, जो कई मायनों में अच्छी भी रही और कई मायनों में दकियानूसी भी. जिन्हें आज की तारीख़ में सवाल करना ज़रूरी है और उसके लिए हर समुदाय को खुले मन से बात करनी पड़ेगी न कि यह सोचने पर कि कोर्ट हमारे मज़हबी रिवाज में दख़ल कर रहा है. सोचने की बात ये है कि ऐसे हालात क्यों बने कि कोर्ट को दख़ल देना पड़ा.
(लेखिका जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सरोजनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ में असोसिएट प्रोफ़ेसर हैं. ये उनके अपने विचार हैं.)