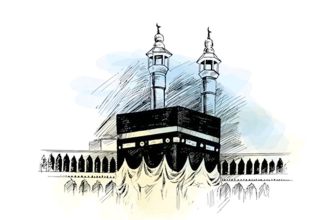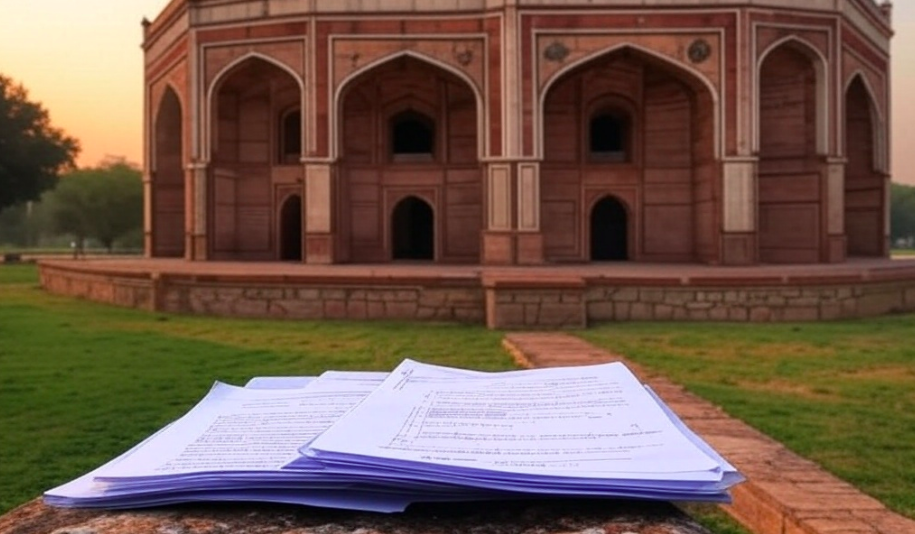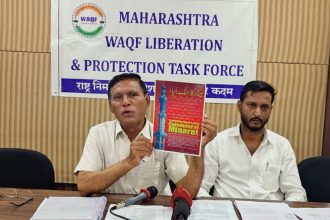यौम-ए-आशूरा के मौक़े से ये सवाल ज़ेहन में आना ज़रूरी है कि आख़िर 14 सौ साल बाद हम इस दिन को इतनी शिद्दत से याद क्यों करते हैं? वैसे तो इस दिन को लोग मातम का दिन कहते हैं, लेकिन असल में ये दिन मातम से ज़्यादा मलामत का दिन है.
यज़ीद की मलामत का दिन है. ये दिन हमें बताता है कि अपने वक़्त में अपनी ताक़त के बल पर हुकूमत चाहे जितना भी ज़ुल्म कर ले… उस समाज में, उस दौर में कुछ हक़ पसंद लोग होंगे, जो उस पहाड़ सी ताक़त से बे-सरोसामानी में भी टकरा जाएंगे. और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो इस दर्द को अपने सीने में महफूज़ रखेंगे. बल्कि यूं कहें, उनकी पीढ़ियों में… कि दिल के दाग़ को किस तरह से रखते हैं रौशन, ये हुनर भी रखने वाले होंगे.
बनू उमय्या के दूसरे शासक यज़ीद के माथे पर नवास-ए-रसूल हज़रत इमाम हुसैन के क़त्ल का दाग़ है. इस शहादत को गुज़रे 1380 साल हो गए, लेकिन हर दौर में, हर ज़माने में लोग यज़ीद को मलामत करते आ रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है.
इमाम हुसैन को शहादत क्यों देनी पड़ी?
मामला कुछ यूं है कि पैगंबर मोहम्मद (ﷺ) के इंतक़ाल के तीस साल बाद अमीर माविया शासक (असल ख़िलाफ़त का दौर जाता रहा) बने. अपने दौर में उन्होंने खूब जंगें लड़ी, ख़ूब फ़तूहात हासिल कीं. मौटे तौर पर उनकी रियासत में अमन चैन भी था… लेकिन वो उसूल नहीं थे, जो इस्लामी हुकूमत का तुर्र-ए-इम्तियाज़ होता है. अपने मुख़ालिफ़ीन को जमकर कुचला, जब चाहा जिसे चाहा मावरा-ए-अदालत (extra judicial) क़त्ल को अंजाम दिया. 15 साल तक ज़ुल्म-व-सितम की हुकूमत चला चुका तो अपनी मौत से पांच साल पहले अपने बेटे को हुकूमत देने का ऐलान किया. तब तीन महादेशों तक हुकूमत फैल चुकी थी, लेकिन सिर्फ़ 5 लोगों ने मौजूदा हुकूमत के फ़ैसले का विरोध किया.
सन् 680 में जब माविया का इंतेक़ाल हुआ तो बेटे यज़ीद को ताज पहनाई गई. ऐलान से ताजपोशी के दौरान पांच साल में मुख़ालिफ़ीन पांच में से एक शख़्स का इंतेक़ाल हो चुका था. चार बचे. चार में से अब दो की ये राय हुई कि जब यज़ीद ने हुकूमत ले ली है तो बग़ावत न की जाए. बाक़ी बचे दो… इन दोनों की दो राय थी. एक की राय थी कि हिजाज़ (मक्के-मदीने) में रहकर विरोध किया जाए. जबकि इमाम हुसैन ने कूफा (इराक़) जाने का फैसला किया. कूफा गए और करबला में शहादत का जाम पीया.
इस पूरे घटनाक्रम से साफ़ है कि हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले हमेशा कम लोग होते हैं.
मायूस न हों
करबला की घटना के 40 साल बाद… उसी उम्मया शासक में एक खलीफ़ा हुए— उमर बिन अब्दुल अज़ीज़. सिर्फ़ दो साल तक ख़लीफ़ा रहे. लेकिन इस इंसाफ़पसंदी से हुकूमत की कि शिया और सुन्नी दोनों उन्हें पहला मुजद्दि-ए-इस्लाम क़रार देते हैं.
हमें क्या करना चाहिए?
अगर इमाम हुसैन के सच्चे पैरोकार हैं तो हालात कैसे भी हों, सच के साथ रहिए. ग़लत के ख़िलाफ़ अलम उठाएं. दूसरे हालात से मायूस नहीं होना चाहिए. आख़िर आज़र के यहां भी इब्राहीम पैदा होते हैं.
सबक क्या है?
हाकिम वक़्त का हुकमरां होता है, जो चाहे सो कर ले… लेकिन इतिहास कभी माफ़ नहीं करता. मरने के बाद भी मलामत जारी रहती है. यज़ीद सबसे बड़ी मिसाल है. लानत है यज़ीद पर…
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. ये लेख उनके फेसबुक टाइमलाईन से लिया गया है.)