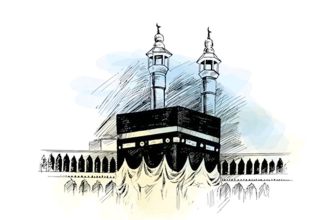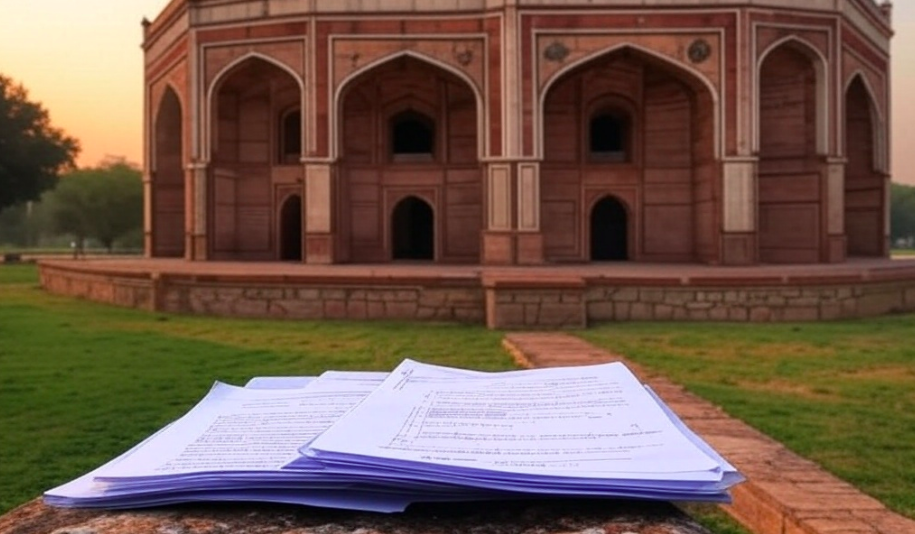By Tarique Anwar Champarni
पटना का मौर्यालोक मार्केट राजनीतिक प्राणियों का चारागाह है. प्रतिदिन शाम में लेखक, पत्रकार, छात्र-नेता, राजनेता, शिक्षक, समाजसेवी, डॉक्टर, व्यापारी, ब्यूरोक्रेट इत्यादि का लगने वाला जमावड़ा बिहार की राजनीति को समझने के लिए पर्याप्त है. उस जमावड़े में शामिल कुछ लोग केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनाने की बात करते हैं साथ में कन्हैया कुमार की जीत की भी कामना करते हैं.
आप जब उन लोगों की जाति जानने का प्रयास करेंगे तब आप बखूबी समझ जाएंगे कि वह किस जाति समूह के लोग हैं.
एक दिन पटना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिस में बेगूसराय मंडल भाजपा के महामंत्री से भेंट हुई. वह भी जाति से भूमिहार थे. बातचीत में ऐसा लगा कि उनकी भी इच्छा थी कि कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़े. आप निजि जीवन में भाजपा से सहानुभूति रखने वाले कुछ भूमिहार जाति के लोगों से बात करें. बात करने के दौरान एक बात सभी में कॉमन होगा वह यह कि सब कुछ के बावजूद कन्हैया भाषण अच्छा करता है.
मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया है ताकि यह समझा जा सके कि कन्हैया कुमार के भूमिहार जाति से होने और बेगूसराय से चुनाव लड़ने के बीच का सम्बन्ध समझ सके. वह भले ही आवेदन देकर भूमिहार जाति में जन्म नहीं लिए हो, मगर बेगूसराय में उनकी जाति उनकी पहचान बनती जा रही है.
बीबीसी के एक कार्यक्रम में कन्हैया जाति के प्रश्न पर जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या वह अपने माता-पिता बदल लें. मेरा मानना यह है कि जातीय श्रेष्ठता के प्रश्न पर इतना घुमाकर जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है. बल्कि यह स्थापित सत्य है कि सवर्ण जाति में जन्म लेने पर लॉबी, नेटवर्किंग, मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता इत्यादि स्वयं से विकसित होता जाता है.
इसी 15 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में बीबीसी हिंदी के द्वारा “बोले बिहार” नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. उस कार्यक्रम के एक हिस्सा में कन्हैया कुमार को बतौर वक्ता बुलाया गया. कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार रूपा झा मॉडरेट कर रही थी. इस पूरे कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने जिस तरह से जाति के प्रश्न का उत्तर दिया वह बिल्कुल ठहलाने जैसा था.
वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर ने जब जातिय पहचान के संदर्भ में प्रश्न किया तब कन्हैया कुमार रूस के लेनिन का उदाहरण देकर और रूस के विघटन की बात करके प्रश्न को टाल गए. जबकि सच्चाई यही है कि रूस के भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. भूगोल एवं समाज का राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप होता है.
रूस के विघटन में रूस की भौगोलिक संरचना सबसे बड़ी वजह थी. भारत के संदर्भ में उसी रूस की थ्योरी को फिट करके नहीं देखा जा सकता है. बल्कि रूस की सामाजिक संरचना में जाति जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मगर वहां की जो सामाजिक संरचना थी उसको कम्युनिस्ट सही से एड्रेस नहीं कर सकी जिसका परिणाम हुआ कि रूस से कम्युनिस्ट की सरकार चली गई. इसलिए भारत के राजनीतिक बदलाव को रूस के सन्दर्भों में जस्टिफाई करना एक प्रबुद्ध स्कॉलर का काम नहीं है.
वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जो जाति के मुद्दें पर बहस नहीं करना चाहता है वही असल जातिवादी है. इस पूरे एपिसोड में कन्हैया कुमार ने जाति वाले सवाल को टाल दिया. रूपा झा के सवाल को भी कन्हैया ने टालने का प्रयास किया. वह मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक विशेष जाति वर्ग के होने के कारण बेगूसराय में उनको लाभ मिल रहा है. बल्कि जाति के सवाल को रात में सड़कों पर निकलने वाली महिलाओं की छेड़खानी से तुलना करके जवाब दिया.
महिला तो स्वयं में एक शोषित वर्ग है और उसी वर्ग को उदाहरण मान लेना तर्कपूर्ण नहीं है. देश भर के दर्जनों प्रतिष्ठित संस्थानों में सैकड़ों रिसर्च से साबित हो चुका है कि महिला स्वयं में शोषित वर्ग है और यदि महिला दलित समुदाय से है तब दोहरा शोषण झेलती है. फिर कन्हैया जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जाति जैसे संवेदनशील मुद्दें को इतने हल्के में लेकर कैसे चल सकते है? ग़ज़ब तो तब लगा जब हॉल में बैठें लोग कन्हैया के जवाब के बाद ताली पीट रहे थे.
जहां तक सवाल भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के कमज़ोर होने का है, तब कन्हैया ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकारा कि कम्युनिस्ट पार्टी समाज के बदलते स्वरूप को समझकर आंदोलन का रूप नहीं बदल सकी है. मैं कन्हैया की इस बात से भी सहमत नहीं हूं. भारत कल भी जातिवादी समाज था और आज भी जातिवादी समाज है. भारत की राजनीतिक सच्चाई को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक जातियों की आंतरिक राजनीति को नहीं समझ लिया जाए.
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा वर्ग-विभेद को मुद्दा बनाकर राजनीति किया है. जबकि होना यह चाहिए था कि कार्ल मार्क्स की उस थ्योरी को भारत में जाति में फिट करके देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बाबा साहब अम्बेडकर मार्क्स और हेगेल की थ्योरी को जाति की संरचना पर फिट करके देखना चाहते थे. क्योंकि उच्च जाति में जन्म लेना एक एडवांटेज रहा है.
कम्युनिस्ट आंदोलन में सबसे अधिक सहभागिता दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की रही है. लेकिन प्रतिनिधित्व हमेशा सवर्ण एवं ब्राह्मणों के हाथ में रहा. उदाहरण के रूप में बेगूसराय, चम्पारण, जहानाबाद, गया, आरा इत्यादि ज़िलों में भूमिहार जाति का दबदबा रहा है. बिहार में भूमिहार ही सबसे अधिक ज़मीन के मालिक हैं. दलितों का सबसे अधिक शोषण यही जाति वर्ग के लोग भी किए हैं. लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यही है कि कम्युनिस्ट आंदोलनों के अग्रणी नेता भी शोषक समुदाय के लोग हैं.
समाजवादी आंदोलन के बाद लालू, मुलायम, नीतीश, पासवान जैसे नेताओं का जब उभार हुआ तब दलितों, पिछड़ों एवं मुसलमानों में प्रतिनिधित्व को लेकर एक चेतना का विकास हुआ. यहीं से दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कम्युनिस्ट आंदोलन से निकलकर समाजवादी राजनीति की तरफ़ शिफ़्ट हुए और नेतृत्व परिवर्तन का यही दौर था जिसे कम्युनिस्ट लोग जंगलराज से पुकारते हैं.
कम्युनिस्ट पार्टी में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर कन्हैया ने रामावतार शास्त्री को बड़ी चालाकी से एक यादव नेता के प्रतीक के रूप में पेश कर दिया. आज भी दूरस्थ भारत की एक बड़ी आबादी कन्हैया कुमार और रवीश कुमार को दलित समझती है. भला उस आबादी को 1967 में चुने गए सांसद राम अवतार शास्त्री की जाति कैसे मालूम होगी? हां, मगर 1967 के समय के लोगों को मालूम था कि राम अवतार शास्त्री यादव समुदाय से आते थे.
इन सब मुद्दों पर बहस करने से पूर्व कन्हैया कुमार को थोड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political Representation) और राजनीतिक सहभागिता (Political Participation) के बीच के अंतर को समझना चाहिए. यह तो स्थापित सत्य है कि कम्युनिस्ट आंदोलन में शोषितों के नाम पर सबसे अधिक सहभागिता पिछड़ी जाति, दलित, अल्पसंख्यकों की रही है.
मगर क्या सहभागिता के अनुपात में दलित, पिछड़े एवं अल्पसंखयकों को प्रतिनिधित्व मिला? कन्हैया ने दबे लफ़्ज़ों में यह मैसेज देने का प्रयास किया कि कम्युनिस्ट पार्टी यादव जाति के लोगों को सांसद बनाती रही है. इसलिए महागठबंधन के अगुआ तेजस्वी यादव को चाहिए कि बेगूसराय से भूमिहार कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार करें.
एक युवा ने कन्हैया कुमार से पूर्व छात्र-नेता चंद्रशेखर उर्फ़ चंदू और बाबहुली नेता मो. शहाबुद्दीन के संदर्भ में प्रश्न किया. कन्हैया ने एक अप्रत्याशित उत्तर दिया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था.
कन्हैया बार-बार यह बताने का प्रयास करते रहे कि चन्द्रशेखर सीपीआई के नहीं थे बल्कि सीपीआई (एमएल) के नेता थे. अब जब चारों तरफ़ से वाम एकता की बात हो रही है उस समय चंदू के प्रश्न पर चंदू को सीपीआई (एमएल) से जोड़कर स्वयं को चंदू से अलग कर लेना कितना न्यायसंगत है? जब सीपीआई और सीपीआई (एमएल) आपस में मिलने को तैयार नहीं है फिर कन्हैया किस तरह के महागठबंधन में शामिल होने की कल्पना कर रहे हैं?
क्या वह सिर्फ़ इसलिए चंदू के सवाल को टाल गए कि महागठबंधन के प्रत्याशी बनने के रूप में उन्हें मो. शहाबुद्दीन के परिवार का अनैतिक समर्थन करना पड़ेगा?
चन्द्रशेखर उर्फ चंदू 1990 में एम.फिल के लिए जेएनयू गए. वह जेएनयू जाने से पूर्व पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे. वह पटना यूनिवर्सिटी में सीपीआई की छात्र विंग AISF के सक्रिय सदस्य थे. वह जब जेएनयू गए तब सीपीआई (एमएल) की छात्र विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) के ढाँचा को अपनी परिश्रम से खड़ा किए थे. कन्हैया कुमार भी सीपीआई की विंग AISF के नेता हैं. इसलिए कन्हैया द्वारा चंदू को सीपीआई से सिरे से खारिज़ कर देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है.
भक्त का विरोध करते-करते लोग कब अंधसमर्थक की फ़ौज खड़ी कर लेते है पता भी नहीं चलता है. जब जेएनयू घटना के बाद कन्हैया कुमार जेल से छूटकर कैंपस पहुंचे तब एक ज़ोरदार भाषण दिया. कन्हैया का कहना था कि संयोग से जेल में उनको खाना लाल और नीलें रंग के कटोरे में परोसा गया. मालूम नहीं उनकी यह बात कितनी सत्य पर आधारित है, वही जाने.
दरअसल, वह यह बताना चाहते थे कि भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा. मगर भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है? जबकि भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों में नार्थ पोल और साउथ पोल का फ़र्क़ है.
उदाहरण के रूप में भगत सिंह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे. जबकि अम्बेडकर पूरा एक ड्राफ़्ट लेकर साइमन कमीशन से दलितों की हिस्सेदारी मांगने चले गए. अम्बेडकर हमेशा डेमोक्रेटिक तऱीके से क़लम को हथियार बनाकर लड़ाई लड़ने की बात करते थे. जबकि भगत सिंह सेंट्रल हॉल पर बम फेंक रहे थे. शूद्रों पर हो रहे अत्याचार के लिए अम्बेडकर ने सवर्णों एवं ब्राह्मणों को दोषी ठहराते थे इसलिए उनका मत था कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय ब्राह्मण भारत से अधिक मिलने की संभावना है. लेकिन भगत सिंह इस बात को नकारते थे.
ऐसे अनेकों वैचारिक विरोधभास हैं, जिससे साबित होता है कि कन्हैया कुमार के सामाजिक रूप से विशेष सुविधा प्राप्त सवर्णों के नेता है. यदि ऐसा नहीं होता तब वह सामाजिक न्याय को मज़बूती प्रदान करने के लिए बेगूसराय से मुहिम छेड़ते और कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर ही किसी दलित या पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज के किसी नेता को मज़बूती से समर्थन देकर चुनाव लड़ाते. इससे सहभागिता के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी बढ़ता और सामाजिक न्याय की विचारधारा भी मज़बूत होती. साथ में कम्युनिस्ट पार्टी की विश्वसनीयता भी वापस लौटती…
(लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), मुम्बई से पढ़े हैं. वर्तमान में बिहार के किसानों के साथ काम कर रहे हैं.)