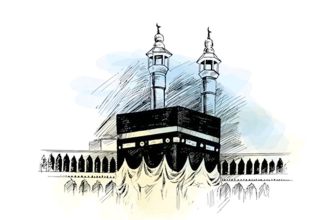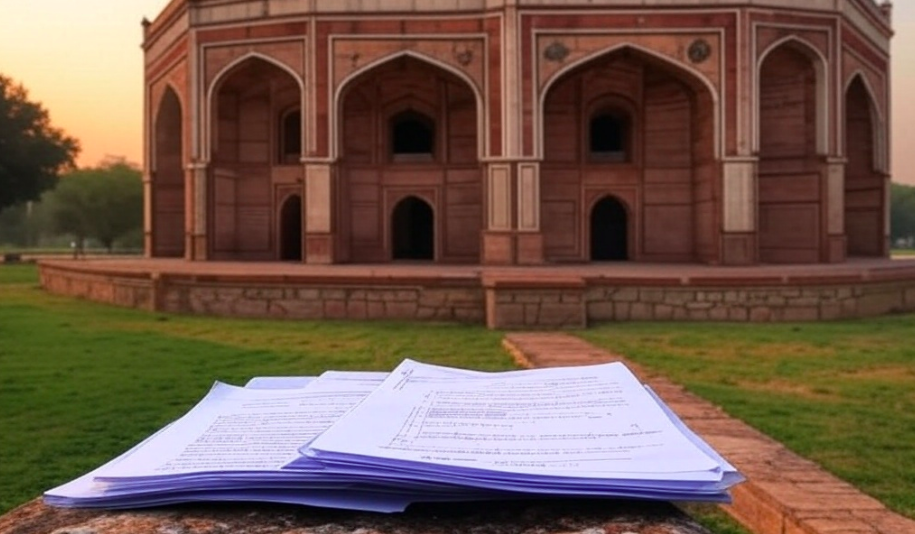Zubair Alam for BeyondHeadlines
देश भर में भाजपा के अत्याधिक उभार से सबसे दुखदायक स्थिति बहुजनों की राजनीति करने वाले दलों की है. आप लोग कहेंगे कि यह कहना किस तरह उचित है. इसका जवाब बड़ा रोचक है.
इन दलों के नेताओं का समान रूप से मानना है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने के लिए भाजपा का डर बना रहना चाहिए. इस कोशिश में ही यह दल सत्तासीन रहते हुए भी ठोस सामाजिक बदलाव से भागते रहे हैं. इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की जगह सत्तासीन होने में सारा ज़ोर लगाया है.
क्या विभिन्न धार्मिक समूहों और जातियों का हुजूम रखने वाले ओबीसी वर्ग में नेतृत्व के स्तर पर विविधता का अभाव कोई और कहानी नहीं बताता है? मंडल कमीशन की आधी अधूरी सिफ़ारिशों के लागू होने के बाद यह बदलाव ज़रूर नज़र आया कि पिछड़ी जातियों के नेताओं को मुख्यधारा में आने का अवसर मिला. परंतु यह सवाल आज भी बना हुआ है कि ओबीसी के स्थापित नेताओं में तमाम पिछड़ी जातियों का समावेश है?
क्या आज का ओबीसी नेतृत्व पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि उसके अंदर तमाम ओबीसी जातियों का प्रतिनिधित्व है? अति पिछड़ा वर्ग और अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के नुमाइन्दे कहां हैं?
मंडल कमीशन ने लगभग चार हज़ार ओबीसी जातियों को चिन्हित किया था. इस कमीशन के एक सदस्य एल.आर. नायक ने इन जातियों में मौजूद असमानता पर भी प्रकाश डाला था और उनका मत था कि ओबीसी में वर्गीकरण तर्क संगत है.
मंडल कमीशन ने सेकूलर-कम्यूनल के दायरे से निकल कर पहली बार स्पष्टता से कहा कि मुस्लिमों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी में आता है. अनुमान के आधार पर इसे कुल मुस्लिम जनसंख्या का लगभग पचासी प्रतिशत कहा जाता है. इनमें अधिकतर की हालत दयनीय है.
इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में हुकुम सिंह के नेतृत्व में ओबीसी वर्गीकरण के लिए बनी “सामाजिक न्याय समिति” ने मुस्लिम ओबीसी को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में रखने की सिफ़ारिश की थी. “सच्चर कमेटी” ने भी मुसलमानों को तीन वर्ग में विभाजित किया. इस प्रकार मुस्लिमों को एक इकाई समझने वालों का दावा खारिज हो गया.
बहुजन/ओबीसी नेतृत्व और मुस्लिम ओबीसी
उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश भर में बहुजन एवं ओबीसी जातियों पर आधारित दलों के उभार के बाद नेतृत्वकर्ता के रूप में जो लोग सामने आए उनसे निम्नलिखित सवाल किया जाना चाहिए.
1. क्या यह लोग ओबीसी में सिर्फ़ हिन्दुओं की जातियो को मानते हैं?
2. क्या उनके अनुसार मंडल कमीशन ने मुस्लिमों को ग़लत तरीक़े से ओबीसी में जोड़ दिया है?
3. अगर मुस्लिमों के एक हिस्से को उनके पिछड़ेपन के आधार पर इस वर्ग में शामिल किया जाना न्याय संगत है तो क्यों अभी तक यह वर्ग पहचान से वंचित है?
4. आख़िर एक ही समय में ओबीसी वर्ग में चिन्हित किए गए दो समूहों में नेतृत्व के स्तर पर एक पक्ष का नेतृत्व नगण्य क्यों है?
5. क्या मुस्लिम ओबीसी को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर हाशिए पर नहीं रखा गया है?
6. क्या राम मनोहर लोहिया के “संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ” और कांशीराम के “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” जैसे नारों के दायरे में मुस्लिम ओबीसी नहीं आता है?
इन दलों में मुस्लिमों को टिकट दिया जाता है लेकिन नेतृत्वकर्ता इस बात को कभी सामने नहीं लाते कि उनका प्रत्याशी मुस्लिमों के कौन से वर्ग से आता है. नेतृत्वकर्ता यह नहीं कहते कि बनारस कैंट विधानसभा का प्रत्याशी मुस्लिम ओबीसी है और बनारस उत्तरी विधानसभा का प्रत्याशी मुस्लिमों के स्वर्ण वर्ग से है.
इसका दिलचस्प उदाहरण यूपी विधानसभा का पिछला चुनाव है. बसपा नेताओं ने 100 मुस्लिमों को टिकट देने की बात को कई बार दोहराया लेकिन यह नहीं बताया कि उनके चुने गए प्रत्याशियों में कितने मुस्लिम ओबीसी हैं और कितने स्वर्ण मुस्लिम. इन दलों के इस रवैये के पीछे आख़िर कौन सा डर काम कर रहा है?
यह आश्चर्यजनक स्थिति है. ओबीसी नेतृत्व में आपको हिन्दू नेता मिल जाएंगे, लेकिन आपको ठीक से चार मुस्लिम नेता भी नहीं मिलेंगे जिनकी पहचान ओबीसी नेता की हो. ओबीसी के स्थापित नेतागण लगभग तीस साल के इस सफ़र में आख़िर क्यों मुस्लिम समुदाय से ओबीसी नेतृत्व सामने नहीं ला पाए?
इस सवाल पर विचार करते समय एक और सवाल उभरता है. बहुजनों या ओबीसी के नाम पर सत्ता में रहे इन दलों ने अभी तक अपनी सरकारों का गठन किस प्रकार के समीकरण के तहत किया है?
बहुजन/ओबीसी नेताओं का समीकरण
उत्तर प्रदेश और बिहार इस समीकरण को समझने में सहायक हैं. उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद की राजनीति का केन्द्र ओबीसी और दलित बने. मुलायम सिंह यादव को ओबीसी नेता और मायावती को दलित नेता के तौर पर पहचान मिली. इन दोनों नेताओं को प्रदेश में सरकार चलाने का अवसर कई बार मिला. यह सामन्यत: माना जाता है कि इस दौर में पिछड़ों और दलितों का इक़बाल बढ़ा था.
इसी संदर्भ को पिछड़े मुस्लिमों पर लागू किया जाए और पूछा जाए कि इनके अधिकारों में और मान सम्मान में क्या वृद्धि हुई थी? यह सवाल इसलिए भी जायज़ है कि इन्हीं मुस्लिमों के एकतरफ़ा समर्थन की वजह से मुलायम सिंह यादव “मुल्ला मुलायम” कहे गए. इसी आधार पर मायावती की भी आलोचना की गई. यूपी के पिछले विधान सभा चुनाव में उन्होंने ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट देकर मुलायम सिंह यादव को मात देने की कोशिश भी की थी.
तमाम प्रयासों के बाद भी ओबीसी में शामिल अलग-अलग जातियों विशेषकर मुस्लिम ओबीसी नेतृत्व का नहीं उभरना इस बात का संकेत है कि इन दलों की नियत में खोट है. “पिछड़ा-पिछड़ा एक समान, हिन्दू हो या मुसलमान” जैसे नारों से साफ़ था कि भविष्य का समीकरण यही हो सकता है क्योंकि इसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं अधिकारों के प्रति चेतना थी.
“जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” का नारा देने वाले कांशीराम की बसपा का सफ़र रोचक है. कभी “तिलक तराजू और तलवार” कहने वाला दल “हाथी नहीं गणेश है, विष्णु ब्रह्मा महेश” तक आ गया. इस सफ़र में बसपा ने स्वर्णों का साथ लिया और सत्ता के लिए जिताऊ फार्मूले के तहत मुस्लिमों को एक इकाई के रूप मे देखा.
यह फार्मूला भय और आशंका से पीड़ित मुस्लिमों की मजबूरी का दोहन है. इस सियासी समीकरण की वजह से इन दलों के लिए ज़रूरी था कि भाजपा के लिए जगह बनी रही अन्यथा मुसलमान हाथ से निकल जाएंगे.
समाजवादी पार्टी ने यह फार्मूला ज़्यादा तत्परता के साथ अपनाया. यही कारण है कि इस पार्टी के शासनकाल में मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा के ज़्यादा मामले सामने आते रहे हैं. सत्ता के लिए सपा ने भी स्वर्णों को जोड़ा और इसी जिताऊ फार्मूले पर अमल करते हुए मुस्लिमों को एक इकाई के तौर पर संगठित किया. यह अलग बात है कि इस क्रम में दोनों दल अपनी स्थापना के उद्देश्य से बहुत दूर चले गए.
ओबीसी मुस्लिमों का भविष्य
यूपी और बिहार सहित देश भर में कितने ऐसे नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनकी धार्मिक पहचान मुस्लिम है एवं सामाजिक व्यवस्था में उन्हें ओबीसी वर्ग में गिना जाता है? चार या पांच नाम भी किसी को याद नहीं होगा. इसलिए यह बात पूर्णत: सच है कि बहुजनों एवं ओबीसी की राजनीति मुस्लिमों विशेष रूप से ओबीसी मुस्लिमों के हितों के विपरीत रही है. इसका कारण सामाजिक व्यवस्था नहीं है. इसका कारण बहुजन एवं ओबीसी दलों का पछपाती और दिशाहीन नेतृत्व है. यह नेतृत्व कभी सत्ता के लिए विपरीत सोच वाले दलों के साथ गठजोड़ करता है तो कभी एक विशेष धार्मिक पहचान को अपनाता है.
आज भी यह पार्टियां इसी फार्मूले पर चल रही हैं. इसका जीता जागता उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव है. सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन में किसी भी दल के पास एक भी ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जिसकी पहचान ओबीसी नेता की हो. इसी तरह बिहार में भी बताना मुश्किल है कि राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के गठबंधन में कितने ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनकी पहचान ओबीसी नेता की है. मुस्लिमों के अंदर मौजूद सभी वर्गों की नुमाइन्दगी करने वाले नेताओं की कमी यह दर्शाती है कि मुसलमान आज भी इन दलों के लिए एक इकाई के रूप में सिर्फ़ वोट बैंक हैं. इनकी मदद से चुनाव जीतना इन दलों का एकमात्र उद्देश्य है.
इस बहस के संदर्भ में कुछ सवाल उठते हैं. इन दलों के जातीय विशेष से आने वाले नेताओं ने जिस तरह अपना नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश की है क्या वह इसी प्रकार अपने स्वभाविक घटक अर्थात ओबीसी मुस्लिमों में भी नेतृत्व तैयार करने में सहायक बनेगें?
कम्यूनल वातावरण में ओबीसी मुस्लिमों के अधिकारों पर जो संकट मौजूद है उससे उबरने में इन दलों की क्या भूमिका होगी? इन्हीं सवालों पर बहुजन एवं ओबीसी राजनीति निर्भर है. भविष्य में बहुजन एवं ओबीसी दलों के नेताओं का रवैया अपने समान लोगों के साथ किस प्रकार का होगा इसी से वंचितों अर्थात ओबीसी तथा अन्य बहुजनों की दिशा और दशा निर्धारित होगी.
(लेखक जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं. इनसे zubair2amu@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है.)