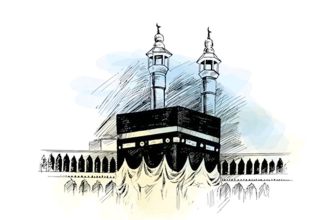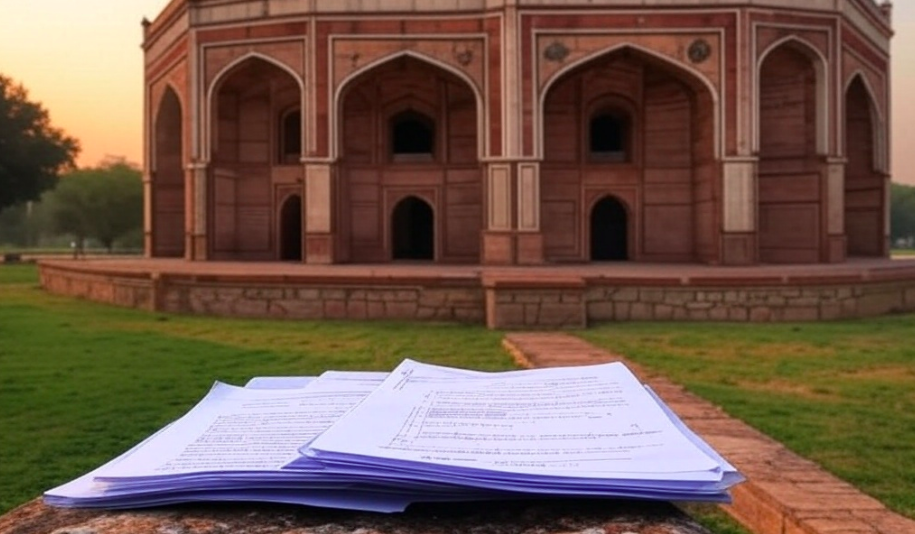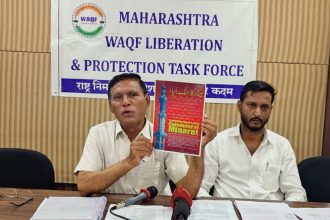By Lochan & Istikhar for BeyondHeadlines
विश्व स्तर पर महामारी की स्थिति उत्पन्न होने के साथ, प्रत्येक व्यक्ति खुद को कोरोना वायरस (COVID-19) से असुरक्षित महसूस कर रहा और चिंतित भी है.
महामारी के रूप में घोषित होने से पहले किसी बीमारी के फैलने के तीन चरण होते हैं. पहला —दूसरे देश से आने वाले संक्रमित लोगों से फैलना, दूसरा —स्थानीयकृत लोगों से फैलना और तीसरा —सामुदायिक स्तर पर गतिविधि से फैलना.
भारत में तीसरे स्तर का प्रभाव धीरे-धीरे दिखने लगा हैं. भारत में वायरस की धीमी प्रगति का कारण अल्प-मात्रा में हुए जांच को भी माना जाता है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कहा कि उचित सुविधाओं की कमी के कारण, भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था को अभी भी कोरोना के उचित परीक्षण करने के लिए 7.7 मिलियन किट की आवश्यकता है.
विशेषज्ञों ने बताया कि कम से कम 2-14 दिनों के लिए स्वयं-संगरोध (अलग-थलग) और ‘सामाजिक दूरी’ करने जैसे व्यवहारों से इस घातक संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है. विशाल सांस्कृतिक विविधता वाले समाज के लिए सामाजिक दूरी की तकनीकी प्रयोग करना और व्यवहार में लाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है.
इस लेख द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या है? इसका अभ्यास कैसे किया जा सकता है? मिथकों का प्रभाव ख़त्म करना, तथ्यों का पता लगाना और सही शब्दावली का उपयोग करना सामाजिक पूर्व आवश्यकता है.
धारणा यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी पीड़ित को पहचान नहीं किया जा सकता है, जो आपके अगल-बग़ल में हो सकता है. इससे वायरस के संपर्क में रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की संभावनाओं को सीमित करता है.
इसलिए कोई भी व्यक्ति जो लक्षणग्रस्त या संक्रमित हो, उसे ख़ासतौर पर सबसे कमज़ोर आबादी, बुज़ुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों से दूर रखना पड़ता है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस दूरी को 1 मीटर के रूप में पहचानता है. सीडीसी (CDC) 2 मीटर कहता है, जिससे सामाजिक दूरी का न्यूनतम माप निर्धारित होता है. परिवार कल्याण और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (MoHFW), गैर-दवा संक्रमण की रोकथाम और उसी के ख़िलाफ़ नियंत्रण हस्तक्षेप के रूप में सामाजिक दूरी को संदर्भित करता है.
‘सामाजिक दूरी’ शब्द का प्रयोग अक्सर आत्म-संगति या अलगाव के रूप मे भी किया जाता है, लेकिन ये तकनीकी और व्यावहारिक रूप से भिन्न है. जो केवल उन लोगों के गतिविधि को प्रतिबंधित करता है जो लक्षणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति की पुष्टि के लिए संक्रामक वातावरण से अवगत है.
दूसरी तरफ़ अलगाव के मामले में, संदिग्ध व्यक्तियों को परिवार के बाक़ी सदस्यों से दूर रखा जाता है. यह एक साथ कितने प्रक्रिया में होता है, लेकिन संदर्भ बिंदु भिन्न होता है. अलगाव के साथ सामाजिक दूरी, एक धीमी प्रक्रिया है, और ज़ाहिर तौर पर लक्षण दिखने में कुछ सप्ताह लगते हैं. तत्काल नाटकीय प्रभाव की अपेक्षा करना निश्चित रूप से एक ग़लत आशंका है. कुछ ही समय में इसका दुस्प्रभाव तीव्र गति से बढ़ जाएगा अगर सामुदायिक रूप से सुरक्षित व्यवहार नहीं किया. जैसे- शारीरिक दूरी, साफ़-सफ़ाई, डॉक्टरों के निर्देशों का पालन, मास्क का उपयोग, स्वयं को साफ़ करना आदि.
यह देखते हुए कि सामाजिक दूरी के तहत मानव अंतःक्रिया का पूर्ण समाप्ति उपयुक्त नहीं है, सामान्य अभ्यास शारीरिक रूप से स्वयं को दूर करना चाहिए. पूरी तरह से 100% दूरी बनाना अवांछनीय है. शारीरिक दूरी को भावनात्मक पृथक्करण से अलग माना जाता है. जबकि ये पूर्णत: सही नहीं है.
स्वयं अलग-थलग की लंबी अवधि में सभी से दूरी बनाए रखने में, संदिग्ध व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक भलाई पर दुष्परिणाम पड़ता है. इसलिए समायोजन तदनुसार किया जाना चाहिए. ज़ाहिर तौर पर इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है. लेकिन संक्रमित या संदिग्ध बुज़ुर्गों को घर में ही अलग-थलग कमरों मे रखना, दूर से उनको सुविधाओं के अभाव और मृत्युशय्या पर देखना, दिल टूटने से अधिक बुरा कुछ और भी नहीं हो सकता है.
बीबीसी समाचार चैनल ने बताया कि वर्तमान में कोई प्रभावी टीका, दवा या चिकित्सा उपलब्ध नहीं है. इस प्रकार पीड़ित व्यक्ति को सामाजिक दूरी ‘कम से कम आधे साल’ के लिए अभ्यास करना पड़ेगा. वैश्विक स्तर पर सामाजिक समारोहों जैसे सार्वजनिक परिवहन, विश्वविद्यालय सभा (सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला आदि), खेल आयोजन और अन्य स्थगित कर दिया गया. वहीं निम्न वर्गों की जीविका, स्वस्थ्य और भलाई अनदेखा कर दिया गया जिस पर चर्चा होना भी महत्वपूर्ण है.
जैसा कि देखा गया है, महामारी की स्थिति हमें अपनी नियमित व्यवस्थाओं में सुधार करने का एक अच्छा अवसर भी मिलता है. जैसे- स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, शारीरिक और व्यावहारिक शिक्षा में सुधार. इस महामारी की स्थिति से निपटने के लिए रणनीति प्रत्येक स्तर से गुज़र रही है, इसलिए मिथकों की फैलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है.
एक उचित संदर्भ नियमवाली का पालन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और दुविधाओं का शिकार नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया के बजाए सरकारी सूचनाओं का पालन करना उचित है.
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च, 2020 को ‘जनता कर्फ्यू’ की घोषणा की गई थी, जो वैश्विक स्तर पर प्रचलित बड़ी सभाओं पर स्थगित और प्रतिबंधित के समानांतर में लाई गई थी. लेकिन जनता में इसको मिथक रूप मे फैलाया गया. जैसे —थाली बजने के साथ ‘गो कोरोना गो’ कहने से कोरोना चला जाएगा, गाय-मूत्र पीने से कोरोना संक्रमण कम हो जाएगा, कर्फ्यू 14 घंटे का है जबकि संक्रमण 9-12 घंटे बाद निष्क्रिय हो जाता है. इसके नतीजे में लोग सड़कों पर झुंड बनाकर इकठ्ठा हो गए, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना बढ़ गया, जिसका परिणाम भारत मे तेज़ी से बढ़े संदिग्धों के आकड़ों से लगाया जा सकता. जबकि जनता कर्फ्यू जनता में थाली और ताली बजाने की मिथक फैलाने में कोई पीछे नहीं रहा चाहे प्रशासन, मीडिया या बॉलीवुड स्टार हो.
इस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, पूरी तरह से व्यवस्थित और संघटित प्रयास की ज़रूरत है. साथ ही शारीरिक दूरी का अभ्यास करते हुए, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित जा सकता है. इस महामारी का समाधान सरकार और जनता एक साथ मिलकर करना होगा. हमें जीवन के साथ संघर्ष कर रहे लोगों के लिए सम्मानजनक व्यवहार के रूप में शारीरिक दूरी और सामाजिक एकजुटता का अभ्यास करना होगा. यह पीढ़ी एक इतिहास देख रही है और हमें इसे बेहतर बनाने के लिए तत्पर रूप से सुरक्षित व्यवहार करना होगा.
(लोचन शर्मा और इस्तिख़ार अली जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर हैं.)