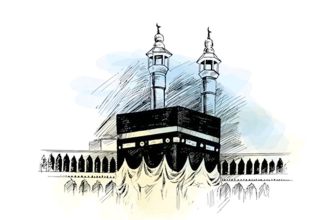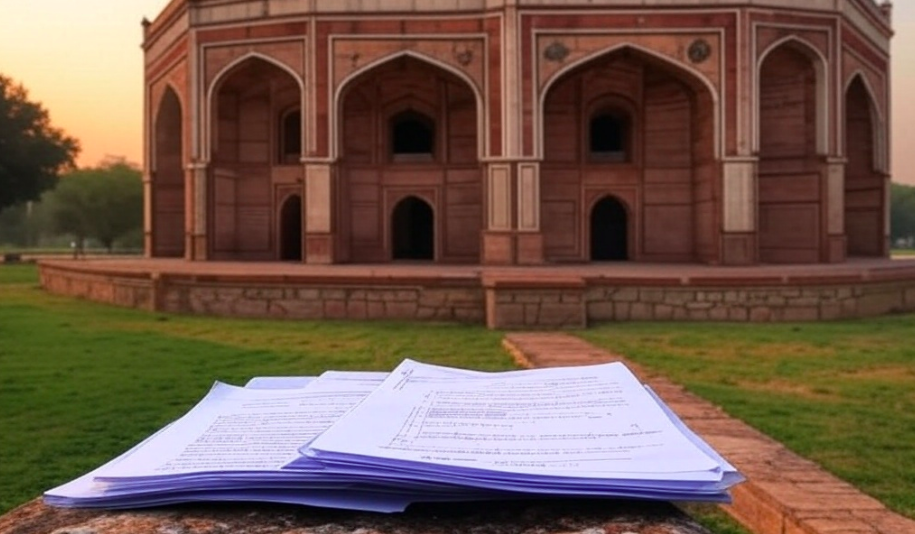Sharjeel Imam for BeyondHeadlines
इस बार आम चुनाव में ‘फ़ासीवाद विरोधी मुहिम’ के कुछ विचित्र परिणाम सामने आए हैं. बेगूसराय में ‘फ़ासीवाद विरोधी’ बुद्धिजीवियों की लाॅबी ने अपनी पूरी शक्ति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उभरते हुए सितारे कन्हैया कुमार के पीछे लगा दी है. चूंकि राजद ने भाकपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है, इसलिए अब इन उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुक़ाबला होगा :
• राजद के सवर्ण मुस्लिम उम्मीदवार तनवीर हसन
• भाजपा के सवर्ण (भुमिहार) हिंदू उम्मीदवार गिरिराज सिंह
• भाकपा के सवर्ण (भुमिहार) हिंदू उम्मीदवार कन्हैया कुमार
सत्ताधारी भाजपा को लगभग सभी हिन्दू जातियों से काफ़ी वोट शेयर मिला है, इसलिए उसे हराने की पूरी ज़िम्मेदारी मुस्लिम मतदाताओं पर डाल दी गई है. बेगूसराय में भाकपा और राजद दोनों मुस्लिम वोटों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं.
भाकपा के बिना यह एक सीधी लड़ाई होती. मुसलमान राजद को वोट देते और फ़ासीवादी ताक़तों के प्रतिनिधि गिरिराज सिंह हारते. पिछले चुनाव के दौरान, तनवीर हसन ने 3.5 लाख वोट हासिल किए और तक़रीबन एक लाख वोटों के अंतर से हारे. भाकपा+जेडीयू ने लगभग दो लाख वोट पाए. इस साल मुसलमान तथा राजद के साथ जुड़े अन्य समुदाय तनवीर हसन के चुने जाने के लिए एक बार फिर प्रयासरत होंगे.
लेकिन फ़ासीवाद के ख़िलाफ़ एकता की दुहाई देते हुए 2014 की तरह ही इस बार भी भाकपा फिर से काम बिगाड़ने में लगी है. यहां तक कि ‘क्रांतिकारी कन्हैया’ की जादुई उपस्थिति ने कई मुसलमानों को भी भ्रमित कर दिया है.
एक आकस्मिक नायक
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापक मुहम्मद सज्जाद ने एक लेख में लिखते हैं कि कन्हैया ना सिर्फ़ व्यावहारिक बल्कि बेहतर उम्मीदवार है. उन्होंने तनवीर के लिए प्रचार करने वाले मुसलमानों को उनकी ‘सांप्रदायिक’ मानसिकता के लिए लताड़ा, और मुस्लिम प्रतिनिधित्व की जायज़ मांग को मात्र ‘पहचान की राजनीति’ तक सीमित कर दिया. वे हमें एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करने के लिए कहते हैं, जहां हिन्दू केवल हिन्दुओं को ही वोट देंगे (जैसे कि इसके लिए किसी भी कल्पना की आवश्यकता हो!).
उन्होंने मुसलमानों के बीच जाति-द्वेष के मुद्दे को भी उठाया, और कहा कि राजद ने उच्च-जाति के मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कोई भी पिछड़े मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा है. उनकी राय में कन्हैया आशा और परिवर्तन की एक किरण हैं और मुसलमानों को अपने संकीर्ण दायरे से बाहर निकल कर उन्हें वोट देना चाहिए.
कन्हैया के समर्थन में लिखे गये लिए तुलनात्मक रूप से ग़ैर-जानकारी से भरे एक दूसरे लेख में उमर ख़ालिद ने भी कमोबेश यही नज़रिया सामने रखा है. वे कहते हैं कि ‘फ़ासीवाद’ के ख़तरे के सामने हमें अपनी ‘पहचानों’ से ऊपर उठ कर कन्हैया को ही वोट डालना चाहिए.
मामला गंभीर है और गुत्थी उलझी हुई है. हम अपनी बात संयोगवश हीरो बने कन्हैया कुमार से शुरू करेंगे, जिनकी आरंभिक प्रसिद्धि ही ग़लत समय पर ग़लत जगह पर ग़लत मुद्दे पर बोलते हुए पाए जाने के कारण हुई.
एआईएसएफ़ के उम्मीदवार के रूप में उनके एक ज़ोरदार भाषण की बदौलत वे 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए. फ़रवरी 2016 में अफ़ज़ल गुरु की फांसी और कश्मीरियों पर अत्याचार के विरुद्ध कैंपस में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ जिसके बाद भाजपा सरकार का जेएनयू पर दमनचक्र आरंभ हुआ. कन्हैया, उमर और अनीरबान गिरफ़्तार हुए. कुछ कश्मीरियों समेत कई छात्रों के ख़िलाफ़ मुक़दमे चलाए गए. इस सब में कन्हैया आकस्मिक रूप से हीरो की तरह उभरे क्यूंकि उनका और उनकी पार्टी का कश्मीर पर नज़रिया इससे मिलता-जुलता नहीं है.
पटियाला अदालत में वकीलों की भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद, कन्हैया फौरन जेएनयू और फासीवाद-विरोधी ब्रिगेड के हीरो बन गए. कैंपस लौटने के बाद उन्होंने कश्मीरी नारे ‘इंडिया से आज़ादी’ को ‘इंडिया में आज़ादी’ में बदलकर अपने अवसरवाद का एक और नमूना पेश किया.
ध्यान रखना चाहिए है कि राजद्रोह के मामले की गंभीरता उन लोगों के लिए वास्तविक थी, जिन्होंने वाक़ई इस तरह के नारे लगाने की हिम्मत की, फिर भी अधिकतर कवरेज भाकपा के सवर्ण हिंदू छात्र नेता कन्हैया को ही मिली.
साक़िब सलीम ने नेताओं की हवा बांधने की इस प्रक्रिया में उदारवादी मीडिया की भूमिका की चर्चा की है. उन्होंने इसकी तुलना लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ पिछड़े छात्रों के मामले के साथ की है जिन्हें प्रधानमंत्री को काला झण्डा दिखाने के कारण ऐसे ही आरोपों का सामना करना पड़ा. उन्हें पकड़ कर जेल में डाला गया और पीटा गया फिर भी कोई उनका नाम तक नहीं जानता.
कथानक भाजपा ने चुना और संघी मीडिया ने जिन्हें ‘खलनायक’ बताया, उदारवादी मीडिया ने उनका महिमामण्डन किया. कन्हैया की पूरी महानता केवल मार्क्सवाद और वर्ग-संघर्ष के उनके अधकचरे ज्ञान और अनायास गिरफ़्तार होने और वकीलों से पिटने मात्र से ही है. कुछ लोग कहते हैं कि वे बढ़िया वक्ता हैं लेकिन ऐसे तो सैकड़ों छात्र-नेता अकेले बेगूसराय में ही मौजूद हैं. सांसद बनने के लिए ये तो कोई पर्याप्त योग्यता नहीं है.
यदि वे वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो उन्हें बेगूसराय में एक मुसलमान प्रत्याशी की हार सुनिश्चित करने की बजाए केजरीवाल की तरह किसी प्रतीकात्मक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था.
मुसलमानों के मुद्दे और भाकपा
जहां तक भाकपा का सवाल है, उसे पश्चिम बंगाल में माकपा के साथ दशकों तक मुस्लिम वोट मिले, फिर भी वहां मुसलमानों की परिस्थिति वंचितों की ही रही. यह तथ्य सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी नोट किया गया है, जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के विकास के सूचकांक भारत के सभी राज्यों में सबसे कम में से हैं. वाम-मोर्चे ने लगभग सभी मुसलमानों को सामान्य श्रेणी में रखा हालांकि अधिकतर मुसलमान पिछड़े वर्गों में हैं. पिछले दशक में ममता बनर्जी ने ही मुसलमानो की बहुलांश जातियों को आख़िरकार पिछड़ों की सूची में सम्मिलित किया.
भाकपा की एक और विशेषता रही है कि मार्क्सवाद पर शानदार भाषण देने वाले उसके नेता उच्च-जातियों में ही पाए जाते रहे हैं. कन्हैया तो बस भाकपा में सफल होने वाले सवर्ण नेताओं की सूची में सबसे ताज़ा उदाहरण मात्र हैं. मज़ेदार तो यह है कि भाजपा भी उसी जाति से सबसे ज़्यादा वोट पाने की आशा में है जिस जाति से कन्हैया आते हैं. ये आगामी प्रतियोगिता की ‘क्रांतिकारी’ प्रकृति के बारे में अपने आप में बहुत कुछ कहता है.
दूसरी ओर, तनवीर हसन एक एमएलसी रहे हैं और एक अनुभवी नेता हैं, जो 1970 के दशक से समाजवादी आंदोलनों में शामिल हैं. वे भाजपा को हराने के लिए पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं.
विकल्प स्पष्ट होना चाहिए था
एक तरफ़ हैं कन्हैया जो कि एक सोशल मीडिया परिघटना है, जो एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो भाजपा का समर्थन करता है और एक ऐसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो गंभीर रूप से मुस्लिम विरोधी रही है.
दूसरी तरफ़ हैं तनवीर, जो बिहार को सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त और पिछड़े मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए जानी जाने वाली पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं.
फिर भी उदार लॉबी ने कन्हैया के लिए मुस्लिम वोटों को लुभाने में और तनवीर हसन के विरुद्ध उम्मीदवार मैदान में उतारने के भाकपा के नासमझी भरे क़दम का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.
पहचान की राजनीति और मुस्लिम सांप्रदायिकता
उनका पहला तर्क होता है कि यदि हिंदू सिर्फ़ हिंदुओं को ही वोट दें तो सोचो मुसलमानों का क्या होगा? लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें इसके लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भारतीय राजनीति की सच्चाई ही है. मौलाना आज़ाद को भी 1952 में रामपुर से चुनाव लड़ना पड़ा था क्यूंकि यूपी में वही एकमात्र सीट थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे.
मुहम्मद सज्जाद ने स्वयं ऐसा एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है: 1962 के चुनाव में जब मग़फ़ूर एजाज़ी मुज़फ़्फ़रपुर से कांग्रेस के विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए.
“इंदिरा गांधी को कांग्रेस के लिए मुज़फ़्फ़रपुर में विशेष प्रचार-अभियान चलाने पड़े जिनके भाषणों द्वारा वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया. फलस्वरूप 58,000 वोट पाने में कामयाब रहने के बावजूद एजाज़ी की हार हुई”
बिहार में पिछले तीन दशकों में जो बदलाव आया वह यह है कि जातिगत संघर्षों के फलस्वरूप मुस्लिम और पिछड़े समुदायों के बीच गठबंधन बन पाया, जिससे मुस्लिम उम्मीदवार हिन्दू उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ हिन्दू वोट हासिल कर सके. अब केवल 2019 के चुनाव में बिहार में हिन्दुओं के वोट सिर्फ़ हिन्दुओं को जाने की दलील देकर डराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा.
दूसरा आरोप आता है मुस्लिम-सांप्रदायिकता का और इसे सबसे अधिक दोहराया जाता है. विद्वानों और शोधकर्ताओं ने इस कांग्रेसी शब्द-युग्म का उपयोग इस हद तक किया है कि मुसलमान भी अपना प्रतिनिधित्व मांगने में शर्मिंदा होने लगे हैं. इसके बाद, वामपंथी वाक्यांश ‘पहचान की राजनीति’ को लपेट दिया जाता है. दरअसल मुसलमान एक अल्पसंख्यक समुदाय हैं और दलितों की ही तरह संगठित होने के लिए अपनी धार्मिक पहचान का उपयोग करना हमारा अधिकार है. जब दलित अपनी जातिगत पहचान के आधार पर रैली करते हैं, तो हमारे उदारवादी अचानक ‘जातिविहीन’ हो जाते हैं; इसी तरह, जब मुसलमान पुनर्वितरण चाहते हैं, तो हमारे उदारवादी यकायक ‘धर्मनिरपेक्ष’ हो जाते हैं और ‘पहचान की राजनीति’ का आरोप लगाने लगते हैं.
अंत में, बिहार की राजनीति में निम्न जाति के मुसलमानों का मुद्दा. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च-जाति के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में अधिक हिस्सा मिलता रहा है. लेकिन पिछले तीन दशकों में यह धीरे-धीरे बदला है. इसका कारण है कि लालू – और कुछ हद तक नितीश – ने निम्न जाति मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयास किए.
इस साल, राजद 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, जिनमें से चार मुस्लिम हैं. उनमें से दो शेख़ समुदाय के हैं, एक सैय्यद है और एक कुल्हय्या (पसमांदा) है. 1931 की जाति की जनगणना के अनुसार, बिहार में लगभग एक-तिहाई मुसलमान खुद को ‘शेख़’ कहते थे; मुसलमानों में यह सबसे बड़ा ब्लॉक है.
यह सच है कि एक और पिछड़े मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाना चाहिए था, लेकिन बस भाकपा का बचाव मात्र करने के लिए राजद की आलोचना नहीं की जा सकती है. ये हस्यास्पद है कि मुसलमानों को कहा जाए कि मुस्लिम उम्मीदवार के ख़िलाफ़ भुमिहार को वोट करो, सिर्फ़ इसलिए कि पहला वाला सैय्यद है. फिर भी, उदारवादी मुसलमान सांप्रदायिक कहलाए जाने के डर से बचने के लिये इस हद तक जा सकते हैं.
(शरजील इमाम आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं और वर्तमान में जेएनयू से आधुनिक इतिहास पर पीएचडी कर रहे हैं. वे विभाजन और मुस्लिम राजनीति पर काम कर रहे हैं.)