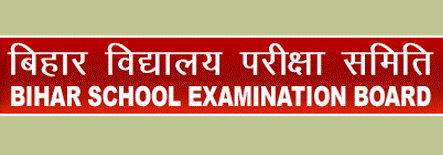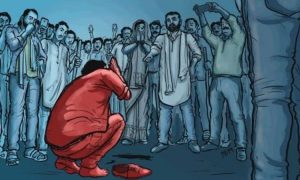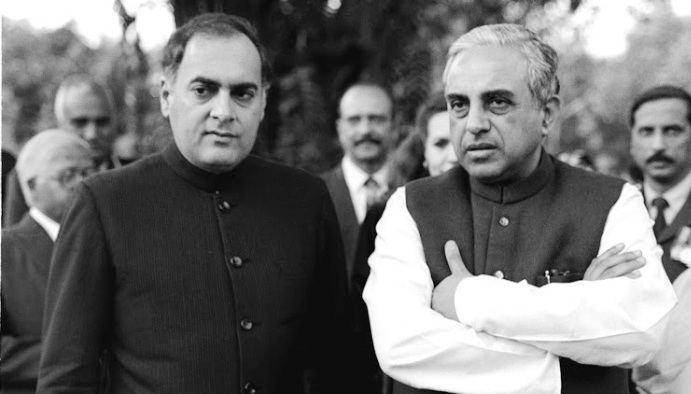Hare Ram Mishra for BeyondHeadlines
अभी कुछ दिन पहले ही, ‘आध्यात्मिक गुरू और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को लोकसभा चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए.
इसके पीछे उनका तर्क था कि क्षेत्रीय पार्टियों के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण ही केन्द्र में मिली-जुली सरकारें बनती है और जिसके लिए उन्होंने ’खिचड़ी’ शब्द इस्तेमाल किया. उनका मानना था कि खिचड़ी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, तथा रुपए के अवमूल्यन के लिए जिम्मेदार होती हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर केन्द्र में अगली सरकार मिली-जुली बनती है, तो भारतीय रुपए की कीमत काफी नीचे चली जाएगी. उनका विचार था कि मुल्क में अमरीकी समाज जैसा राजनैतिक सिस्टम लागू होना चाहिए, जहां केवल दो ही दल हैं.
उन्होंने अपने अनुयायियों से भी अपील की कि वोट देने से पहले वे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में ज़रूर रखें.
गौरतलब है कि श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के अंर्तराष्ट्रीय महासचिव महेश गिरि पूर्वी दिल्ली से भाजपा के टिकट पर लोकसभा के प्रत्याशी हैं. यहां तक कि राजनीतिक जगत में श्री श्री रविशंकर की छवि भी संघ के एक वैचारिक समर्थक की मानी जाती है.
यही नहीं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं. ऐसे में, यह बात साफ है कि उनकी यह अभिव्यक्ति भी संघ के राजनैतिक दर्शन का एक छोटा सा प्रतिबिंब है, और इस लिहाज से इसका विश्लेषण होना चाहिए कि छोटे दलों को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की इस विचारधारा के पीछे का राजनैतिक और सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? आखिर इस विचार के प्रचार के पीछे संघ की कौन सी राजनैतिक रणनीति काम कर रही है?
क्या यह सच है कि क्षेत्रीय दल ही वर्तमान समय में देश की सुरक्षा तथा अर्थव्यस्था की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं? और क्या उनके लोकसभा चुनाव से हटते ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जहां तक इस देश में क्षेत्रीय दलों के उदय का सवाल है, यह बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि इनका राजनीति में उदय अचानक घटी कोई परिघटना नहीं थी.
आजादी के समय तक देश के अंदर कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों के अलावा गिनती के कुछ ही ऐसे दल थे जो राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर नहीं थे. ज्यादातर जनता का नेतृत्व कांग्रेस और अन्य इन्हीं दलों में कार्यरत देश के सवर्ण और एलीट तबकों द्वारा किया जाता था.
देश के सामाजिक और राजनैतिक विकास की प्रक्रिया में जब जब किसी खास वर्ग को ऐसा महसूस हुआ कि उसके लाजिमी सवाल अब वर्तमान नेतृत्व हल नहीं कर सकता या फिर करने का इच्छुक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसी वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा उस वर्ग को राजनैतिक रूप से संगठित करने की कोशिश शुरू हुई. इसे हम उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी के उदय के रूप में देख सकते हैं.
वर्तमान बसपा का दलित मतदाता, जो कभी कांग्रेस का ही वोट बैंक था, आज उसके अलग हटकर अपने सवालों पर गोलबंद होकर एक राजनैतिक ताकत बन चुका है. इसी तरह तकरीबन हर राज्य में क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति राज्य विशेष के सामाजिक आर्थिक सवाल और जातिगत अस्मिता को लेकर हुआ है.
यही वजह है कि दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार उत्तर में नहीं है और उत्तर की राजनैतिक पार्टियां दक्षिण में अपना कोई जनाधार नहीं रखती हैं. कुल मिलाकर यह मानना कि इनकी वजह से ही राजनीति और अर्थव्यवस्था की सारी समस्याएं हैं, कोई मज़बूत तर्क नहीं लगता.
एक बात और, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां हर राज्य के आदमी की राजनैतिक आकांक्षाएं और सवाल अलग-अलग हैं, किसी सामान्य मुद्दे पर एक राय नहीं हो सकता. क्योंकि, आज तक इस मुल्क की राजनीति ने कोई ऐसा सामान्य सवाल पैदा ही नहीं किया जिसे देश के सभी राज्यों के नागरिक लाजिमी समझें और एक राष्ट्रीय विचारधारा के तहत एक सूत्र में बंध सकें। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसे सामान्य मुद्दे राष्ट्रवाद के आधार स्तंभ हो सकते थे, लेकिन आज की राजनीति इन सवालों पर बात करना जरूरी नहीं समझती.
शायद यही वजह है कि यह देश आज तक एक राष्ट्र का रूप धारण नहीं कर पाया है. अब अगर हम श्री श्री रविशंकर की यह मांग मान भी लें और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए केवल राष्ट्रीय दलों को ही आगे लाया जाए, तो और भी गंभीर समस्याएं इस मुल्क की राजनीति के सामने आ जाएंगी.
वे लोग जो अब क्षेत्रीय दलों को वोट करते हैं, अपना मत किसे देंगे? फिर उन लोगों को जबरिया किसी ऐसे दल को जिसे वे नहीं चाहते, वोट देने के लिए बाध्य करना भी एक तरह की तानाशाही ही होगी. इन मतदाताओं के विकल्पों का खात्मा नहीं किया जा सकता.
हम यह भी जानते हैं कि मुख्यधारा के ज्यादातर राजनैतिक दलों के बीच संघ की गहरी घुसपैठ है और यह भी सच है कि क्षेत्रीय दलों को वही जातियां ज्यादा समर्थन करती हैं, जो लंबे समय तक सामाजिक और राजनैतिक तिरस्कार तथा अन्याय सहते हुए देश के विकास क्रम में पिछड़ गई थीं. या फिर, वे सब देश की सवर्ण पोषित मनुवादी व्यवस्था के उत्पीड़न की शिकार रही हैं. फिर यह भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरह से देश के एक बड़े वर्ग की राजनैतिक सहभागिता का खात्मा करके इस लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखा जा सकेगा?
गौरतलब है कि संघ का पूरा राजनैतिक दर्शन ही मनुस्मिृति आधारित तानाशाही युक्त कुलीनतंत्रीय है जहां एक खास वर्ग ही सत्ता संचालन करता है. उसकी इस व्यवस्था में लोकतंत्र और सामाजिक न्याय जैसे शब्द केवल एक भ्रम से ज्यादा कुछ नही हैं.
दरअसल, आज इस देश का लोकतंत्र जिस जगह पर खड़ा है वह एक एक लंबे विकास का परिणाम है. क्षेत्रीय पार्टियों का विकास भी उसी क्रम में हुआ है. उन्हें अब इस परिदृश्य से अचानक गायब नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें देश की समस्याओं की जड़ ही कहा जा सकता है.
कुल मिलाकर, श्री श्री रविशंकर का यह बयान संघ के उस फासीवादी राजनैतिक दर्शन को समर्थन देता है, जहां पर देश की पिछड़ी, शोषित और दलित, अल्पसंख्यक जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है.
अगर यह बात मान ली जाए तो एक बड़ी आबादी के राजनैतिक अधिकार का खात्मा हो जाएगा और केवल कुछ ही दलों के पास वास्तविक सत्ता केन्द्रित हो जाएगी. यह क़दम धीरे धीरे लोकतांत्रिक रास्ते से मुल्क को फासीवाद की ओर अग्रसर कर देगा.
क्या हम लोकतंत्र के रास्ते इस मुल्क में फासीवाद को अपनी पकड़ बनाने का मौका देना चाहेंगे? जाहिर है बिल्कुल नहीं क्योंकि उस अवस्था में एक नागरिक के मूल अधिकार भी अलग-अलग होंगे जो कि बेहद खतरनाक होगा.
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार हैं.)