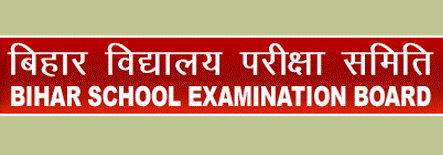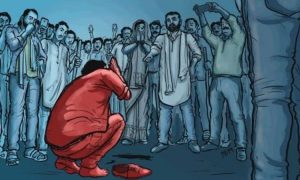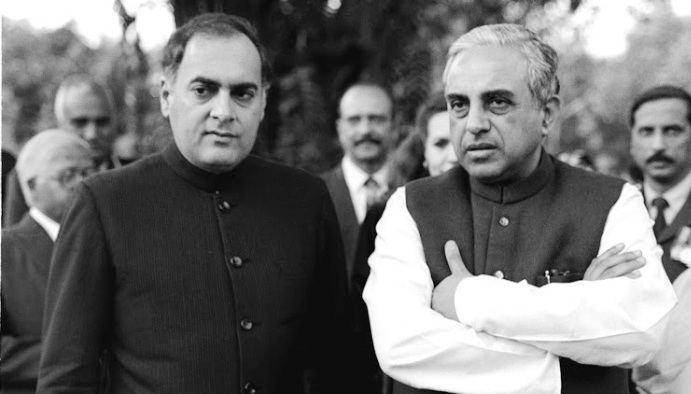बात 1896 की है. महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ था. अनाज की दुकानें लूटी जा रही थीं. इस पूरे मामले में बाल गंगाधर तिलक ने 17 नवम्बर, 1896 के ‘केसरी’ के लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार को याद दिलाया कि लोगों की जान की हिफ़ाज़त करना उनकी ज़िम्मेदारी है. लेख में अकाल-ग्रस्त ग्रामीणों के हालात के हवाले से चेतावनी दी कि सरकार ने अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो किसान बग़ावत कर देंगे. साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ‘स्पेशल रिलीफ़ फंड’ जो खज़ाने में पड़ा है, उसका सही इस्तेमाल किया जाए…
तिलक के इस मैगज़ीन में कई महीने तक अकाल की चर्चा होती रही. दरअसल इस ‘केसरी’ मैगज़ीन का संपादन, प्रकाशन और मुद्रण तीनों की ज़िम्मेदारी बाल गंगाधर तिलक पर थी. तिलक ने यहां तक लिखा कि किसी ज़िला और गांव में किसान कम से कम इस साल ‘लैंड टैक्स’ अदा न करें.
इंग्लैंड की महारानी ने अपनी स्पीच में कहा था कि अकाल पीड़ितों को बचाने के लिए वो बहुत चिन्तित हैं. उसका हवाला देते हुए तिलक ने अपने पाठकों से पूछा कि ‘क्वीन चाहती हैं कि कोई न मरे, जब गवर्नर घोषणा करता है कि सब जीवित रहें और सेकेट्री ऑफ़ स्टेट, ज़रूरी हो तो खर्च करने को तैयार है तब आप कायरतावश भूखों मरेंगे? सरकार का शुल्क देने के लिए यदि आपके पास रुपया है तो ज़रूर दीजिए. किन्तु नहीं हो तो अधीनस्थ सरकारी अफ़सरों के तथाकथित क्रोध से बचने के लिए क्या सब कुछ बेच देंगे? मौत के चंगुल में भी आप दिलेर नहीं हो सकते? इंग्लैंड में यदि ऐसा अकाल पड़ता और वहां का प्राइम मिनिस्टर इतना उदासीन होता तो सरकार स्किट्ल्स की तरह लुढ़क जाती. बाज़ार क्यों लूटते हो? कलेक्टर के पास जाओ और काम और अनाज देने को कहो. यह उसका कर्तव्य है.’
1897 के शुरू में देश ब्यूबॉनिक प्लेग महामारी का शिकार हो गया. बम्बई में चार सप्ताह के अन्दर चार सौ व्यक्ति प्लेग (गिल्टी वाला) का शिकार हो गए. वायसराय ने परिस्थिति की गंभीरता के तहत 4 फ़रवरी 1897 को ‘एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897’ लागू कर दिया. गवर्नरों को विशेष अधिकार मिल गए. बता दें कि आज भी यही 123 साल पुराना एक्ट कुछ संशोधनों के साथ हमारे देश में लागू है.
बहरहाल, तिलक ने सरकार का हर तरह से साथ दिया. रोगियों को शेष आबादी से अलग रखे जाने में अधिकारियों की सहायता की. किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो अपने मकान में रहकर खुद को ईश्वर की दया पर निर्भर रहने के पक्ष में थे.
इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने रैण्ड नामक अफ़सर पूना में नियुक्त किया जो सतारा में सहायक कलेक्टर रह चुका था और अपनी ताक़त आज़माने के काम के लिए मशहूर था. उसे ‘प्लेग कमिश्नर’ बना दिया गया और ‘एपिडेमिक डिजीज एक्ट’ के अन्तर्गत विशेष अधिकार दे दिए गए.
रैण्ड ने ब्रिटिश सेना को मकानों का निरीक्षण करने के लिए भेजा. निरीक्षण करने के बाद उसने उन घरों में सामाग्री नष्ट कर दी जिन पर प्लेग का संदेह था. यही नहीं आरोप ये भी है कि उसने औरतों के साथ छेड़खानी की और वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार किया. कई स्वस्थ लोगों को भी महामारी वाले अस्पताल में पहुंचा दिया.
तिलक ने ‘केसरी’ के लेख में इस अमानुषिक व्यवहार को ‘ए वास्ट एजिन ऑफ़ ऑपरेशन’ कहा. साथ ही वे कुछ लोगों के साथ रैण्ड से मिलने गए और समझाया कि इतना सख़्त व्यवहार न करें. लेकिन रैण्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ.
22 जून, क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली का दिन था. रात के डिनर के बाद जब गवर्मेंट हाउस के मेहमान अपनी-अपनी बग्घियों में जा रहे थे. तभी रैण्ड और एयर्स्ट की हत्या कर दी गई.
इस हत्या के बाद पूना में कर्फ्यू लगा दिया गया. बीस हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित हुआ. सरकार का अंदाज़ा था कि रैण्ड और एयर्स्ट की हत्या तिलक का षड्यंत्र है. तिलक ने सख़्त भाषा में दो लेख लिखे और पुलिस द्वारा उत्पीड़न एवं सरकारी अफ़सर के पूना-वासियों पर अत्याचार की सख़्त आलोचना की.
तिलक के इस लेख के बाद उनके कुछ क़रीबी दोस्तों ने माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़ाने का मश्विरा दिया था. लेकिन इसके जवाब में तिलक का साफ़ तौर पर कहना था, ‘मैं ऐसा नहीं कर सकता. मैं इनका मुक़ाबला करने के लिए तैयार हूं. अगर मुझे सज़ा होगी तो मेरे देश-वासियों की हमदर्दी तकलीफ़ के मौक़े पर मेरी ढारस बंधाएगी.’
कहा जाता है कि तिलक के इस लेख के बाद एंग्लो-इंडियन समाचार पत्रों ने भी अपनी साज़िश शुरू कर दी. तिलक ने ‘केसरी’ के लेखों के द्वारा एंग्लो-इंडियन समाचार पत्रों पर प्रहार किया.
चार सप्ताह भी नहीं बीते थे कि इन लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगा. गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट ने तिलक को क़ैद करने का हुक्म जारी कर दिया. 27 जुलाई की रात तिलक को बम्बई के गिरगांव से हिरासत में ले लिया गया. ये सबकुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इन दिनों देश के कई पत्रकारों के साथ हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है.
अगले दिन सुबह तिलक के वकील डी.डी. दावर ने चीफ़ प्रेजिडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में कहा कि तिलक की रिहाई के लिए ज़मानत देनी चाहिए. लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनके आवेदन को ये कहते हुए रद्द कर किया कि जिन अंग्रेज़ विशेषज्ञों का हवाला दिया गया है वह भारत में लागू नहीं है.
उसके बाद जस्टिस पारसन और जस्टिस रानाडे के सामने हाईकोर्ट में ज़मानत की दरख़्वास्त दी गई. उन्होंने भी यह कह कर टाल दिया कि पुलिस का केस है इसलिए जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. पुलिस कार्यवाही ख़त्म होने पर जब मुक़दमा शुरू नहीं हुआ तो दावर ने दूसरा आवेदन-पत्र दिया जो दुर्भाग्य से पारसन और बचाव पक्ष के रानाडे के कोर्ट में ही आया. उन्होंने मैजिस्ट्रेट के फ़ैसले में दख़ल देना नहीं चाहा किन्तु डिफेंस को ‘आवेदन पत्र दुबारा देने की स्वीकृति दे दी.’
इस बार सिटिंग जज जस्टिस तैयब जी के चैम्बर में आवेदन-पत्र पेश हुआ. जस्टिस तैयब जी ने यह कहते हुए तिलक को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया कि यदि ज़मानत स्वीकार न की गई तो तिलक एक महीने तक जेल में रहेंगे. यदि वे केस के अंत में बेगुनाह साबित कर दिए गए तो बड़ा अन्याय होगा. इसलिए ज़मानत मंज़ूर कर ली है.
123 साल पहले हिंदी में जासूसी लेखन के जनक गोपाल राम गहमरी, लोकमान्य तिलक पर दर्ज इस मुक़दमे पर सुनवाई की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार लिखते हैं. —अदालत के बाहर ज्यों ही यह ख़बर पहुंची, वहां उपस्थित पचास हज़ार से अधिक व्यक्तियों ने एक स्वर में जो तुमुलनाद किया, उसे कोई अब भी नहीं भूल सकता है.
वो आगे लिखते हैं, न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैयब जी अदालत के आसन से उठकर जब अपनी घोड़ागाड़ी पर सवार हुए तब उन पर इतनी पुष्प-मालाओं की वर्षा हुई कि एलिफिंस्टन रोड स्थित अपने घर पहुंचते ही उनकी गाड़ी पूरी तरह फूलों से ढक गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय अपने ताज के साथ न्यायमूर्ति का मात्र सिर लोगों को दिखाई दे रहा था. उस दिन पूरे मुंबई में इस चर्चा का ज़ोर रहा कि जहां तिलक महाराज को उनके जातिभाई ने ज़मानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया था, वहीं एक विधर्मी मुसलमान न्यायमूर्ति के हाथों उन्हें अपेक्षित मुक्ति मिल गई. यही नहीं एडवोकेट जनरल की अड़ंगेबाज़ी पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया.
उसके बाद 8 सितम्बर को बम्बई हाई कोर्ट में जस्टिस स्ट्रैचे के सामने तिलक का मुक़दमा शुरू हुआ. और एक लंबी बहस के बाद उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के तहत बम्बई प्रिजीडेंसी जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बड़ौदा जेल भेज दिया गया.
कौन थे जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी?
बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर और फिर चीफ़ जस्टिस बनने वाले पहले भारतीय थे. उन्होंने 1867 में बम्बई हाई कोर्ट में वकालत बतौर बैरिस्टर शुरूआत की और 1902 में बम्बई हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बने.
10 अक्टूबर, 1844 में पैदा होने वाले बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई के मशहूर बिज़नेसमैन तैयब अली भाई मियां के बेटे थे. वो पहले मुसलमान थे जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया. 1887 में कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने. 1873 में इनकी लीडरशिप में उस वक़्त के मुसलमानों की बम्बई में ‘अंजुमन-ए-इस्लाम’ तंज़ीम बनी थी जिसका मक़सद मुसलमानों के शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक हालात को बेहतर बनाना था.
इनके पोते बदरुद्दीन फ़ैज़ तैयब जी ने आज़ादी के वक़्त राष्ट्रीय तिरंगा झंडे की डिज़ाईन को बनाया था. इसमें सम्राट अशोक के धर्म चक्र को बीच में रखा था. इसके बाद इनकी बेगम सुरैया तैयब जी ने इसकी पहली कॉपी तैयार की जिसे भारत की आज़ादी की ऐतिहासिक रात को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर लहराया गया.
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ.ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी के साथ शामिल रहे. गांधी जी इन्हें कांग्रेस की स्थापना की सबसे अहम कड़ी मानते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग शायद ही इस महान नेता को याद रख पाए हैं.