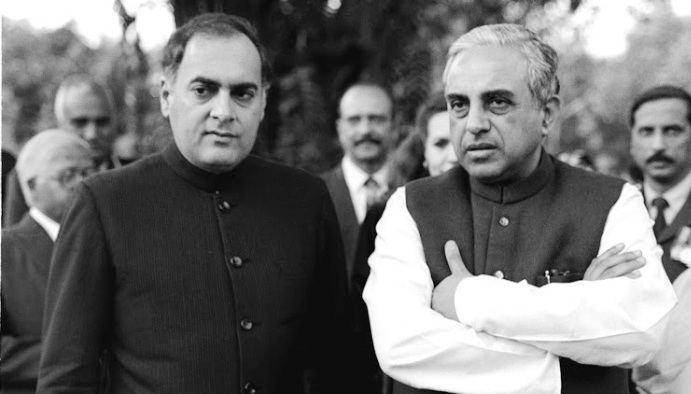Zulaikha Jabeen for BeyondHeadlines
एक प्रश्न, जो मुझे हर वक़्त परेशान करता है. वो यह है कि नमाज़, रोज़े का पाबंद, या हज पर जाने की इच्छा रखने वाला/वाली, क़ुरआन की बात करने वाला/वाली मुसलमान प्रोग्रेसिव या सेक्युलर क्यों नहीं हो सकता/सकती?
आखिर क्यों हिन्दुस्तानी मुसलमान तब तक सच्चा कम्युनिस्ट और सेक्यूलर (स्वीकार्य) नहीं हो सकता/सकती, जब तक वह खुद के अंतिम संस्कार की विधि भारतीय बहुसंख्यक वर्ग के रिवाज के मुताबिक करने की वसीयत न कर दे?
माफी के साथ यहां ये जोड़ना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि नवरात्र और दुर्गापूजा बंगाल के कामरेडों से, पोंगल, ओणम दक्षिण के कामरेडों से, होली, दीवाली बाक़ी के कामरेडों से कभी नहीं छूटती. मगर रमज़ान, मोहर्रम, हज से परहेज़ करता हुआ मुसलमान कामरेड गाहे बगाहे, हर जगह ज़रूर दिखाई दे जाता है. (जबकि ईद में सेंवईयां और बक़रीद में बिरयानी की दावतें स्वतःस्फूर्त तरीके से इनके यहां वाजिब मान ली जाती हैं.)
एक बहुत ही सक्रिय कम्युनिस्ट खुर्शीद अनवर का जिक्र यहां लाज़मी है. उनकी अ स्वाभाविक मौत के बाद उनके मातृ परिवार की उन्हें आखिरी बार देखने/दुलारने और दफ़नाने की इच्छा के बावजूद खुर्शीद की ‘डेडबाडी’ इलाहाबाद नहीं ले जाने दी जाती है. और उनका बेजान जिस्म उनके पत्नी, बेटे (जो उनके साथ रहा नहीं करते थे) के कहने पर दिल्ली के ही एक इलेक्ट्रिक श्मशानगृह में ‘राख’ कर दिया जाता है.
ऐसा ही एक नज़ारा कुछ बरस पहले मशहूर रंगकर्मी, फिल्म व नाट्य कलाकार हबीब तनवीर की स्वाभाविक मौत के बाद भोपाल में देखने को मिलता है, जब लेफ्ट फ्रंट का एक घड़ा उनके जिस्म को जलाने पे उतारू था. मगर हबीब साहब की बेटी की जि़द के आगे उन्हें न सिर्फ़ झुकना पड़ा, बल्कि बड़े बेमन से आलोचना करते हुए उन्हें भोपाल के क़ब्रिस्तान में दफनाना पड़ा.
बहुसंख्यक धर्म के प्रगतिशील कामरेडों के तर्क देखिए- “हबीब साहब ने कभी मुस्लिम परंपरा का निर्वाहन नहीं किया. तो ऐसे में दफनाकर उनका अंतिम संस्कार करना गलत होगा.” (जबकि इन्हीं हबीब साहब की पत्नी जो मुस्लिम समुदाय से नहीं थीं, के अपने शव को दफ़नाने की आखिरी ‘इच्छा’ पर इन्हीं कामरेडों ने उन्हें दफनाए जाने की वकालत करते हुए कई तर्क ढूंढ़ निकाले और एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर उन्हें दफनवा कर ही दम लिया था.
इस विरोधाभासी चरित्र को क्या कहिएगा? ऐसे कामरेडों से यह सवाल लाज़मी हो जाता है कि माना मरने वाले ने मुस्लिम रिवाजों की परवाह या पैरवी नहीं की, तो क्या इतने भर से ही उसके बेजान जिस्म को जलाया जाना लाज़मी हो जाता है? मरने वाले के साथ उसके परिवार के सभी हक़ ज़बरदस्ती छीन लिए जा सकते हैं? (मार्क्स के ‘द केपिटल’ में ऐसा कोई रिवाज हमें तो दिखाई नहीं पड़ा.)
ये बड़ा दिलचस्प है कि हबीब तनवीर जी को जलाने की वकालत करने वाले ज्यादातर कामरेडों ने अपनी और अपने बच्चों की फेरों वाली शादी करवाई हैं. अपने घर के सदस्यों की मौत पे आत्मा की शांति के नाम पर वे आज भी मृत्यु भोज का तामझाम करते हैं. सर भी मुंडवाते हैं. संगम में अस्थियां विसर्जन भी करते हैं. (इन सबसे मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी और को भी नहीं होनी चाहिए.) अपनी बीवियों को मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी से सजाया है. अपनी बेटियों का कन्यादान भी किया है. ज्यादातर के लिए उनकी बीवियां करवा चौथ भी रखती हैं. और तो और राखी, दीवाली, होली आज भी उनसे नहीं छूटती… मगर एक मुस्लिम कामरेड की मौत पर बहुसंख्यक संस्कृति-पोषक कामरेडों की दबंगई देखते ही बनती है.
मेरा सवाल उन तमाम मुस्लिम प्रगतिशील कम्युनिस्टों/जमातों से भी है कि जिस मुस्लिम समुदायिक संस्कृति में पैदा होकर उसे कोसने, बुरा साबित करने में पुरी जिंदगी लगा देते हो. सर्वहारा वर्ग के मानवाधिकारों के लिए ‘पिछला’(मातृ) परिवार भी छोड़ देते हो. अपनी मर्जी से अपना परिवार बनाते, निभाते हो.
पर क्या मुस्लिम समाज, मुस्लिम युवा, मुस्लिम आबादी तुम्हारे सर्वहारा वर्ग की परिभाषा से बाहर है? साम्यवादी समाज के निर्माण में मुसलमानों को भी साथ लेने के लिए मार्क्स, लेनिन, माओ ने क्या तुम्हें मना कर रखा है? मुसलमानों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चेतना को जगाने, बढ़ाने, नए समाज निर्माण में उनको शामिल करना तुम्हें अवैध काम जैसा क्यों लगता है? अछूत की तरह मुस्लिम समाज को राजनीतिक दलालों के बाड़े में जान-बूझ कर छोड़ देने के बाद उन्हें परंपरावादी, कट्टरपंथी, जाहिल समझते/कहते हुए मज़ाक बनाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
लेफ्ट फ्रंट की दोनों बड़ी पार्टियों में किसी नरेश, अमरनाथ, प्रकाश का दाढ़ी रखना भले पुण्य न माना जाता हो, मगर किसी शौकत, तनवीर, नदीम की दाढ़ी इनकी आंखों में गुनाह की तरह क्यों चुभती है.?
बहुसंख्यक संस्कृति की औरतें, मां, बीवी, बेटियों को सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र, बिंदी, चूडियों के साथ चौबीसों घंटे देखने में तो इन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती. मगर मुस्लिम औरतें बुर्के या हिजाब में दिखते ही इन सबकी निगाहें टेढ़ी क्यों होने लगती हैं.?
इस सचाई से कौन मुंह फेर सकता है कि यूपी, बिहार में जब तक मुसलमान कम्युनिस्ट पार्टियों के करीब रहा, इन पार्टियों का सितारा उरूज पर था. हिन्दुस्तान की दोनों बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियां क्या कभी ये सोच पाएंगी कि मुस्लिम समुदाय आखिर क्यों उनसे दूर छिटकता चला जा रहा है? कम्युनिस्ट पार्टियां अपने ज़वाल (पतन) की वजहों पर कब ग़ौर फ़रमाएगी?
तहरीक-ए-आज़ादी के सिपाही, मौलाना हसरत मोहानी ‘पानीपती’ एक बड़े इंक़लाबी शायर होने के साथ ही सूफ़ी, कम्युनिस्ट और इस्लामी स्कॉलर भी रहे हैं. वे सीपीआई की फाउंडेशन के सदर भी रहे हैं. मौलाना इसहाक़ संभली एक तरफ जहां जमियतुल उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी थे, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडरों में भी शामिल रहे हैं. वे संभल सीट से कम्युनिस्ट पार्टी से लोकसभा मेम्बर भी रहे हैं. पुराने कम्युनिस्टों की ज़बान से ये चर्चा अक्सर सुनी है कि कामरेड राजेश्वर राव और इंद्रजीत गुप्ता के रहते तक दिल्ली के अजय भवन स्थित पार्टी ऑफिस में होने वाली बैठकों में अज़ान की आवाज़ आने पर मीटिंग रोक कर मौलाना इसहाक़ से कहते कि आप पहले नमाज़ पढ़ लें फिर मीटिंग आगे जारी रखेंगे.
दरअसल, ये दूसरी धार्मिक संस्कृतियों के एहतराम (आदर) का जज़्बा ही था. शायद जिससे मुसलमान विचारधारा की पुख्तगी के बग़ैर भी कम्युनिस्ट पार्टियों से खुद को जोड़े रखने में फख़्र महसूस करते थे. ये क्या कम अफसोसजनक पहलू है कि आज़़ादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों में लीडर ही नहीं कैडर में भी मुसलमानों की तादात लगातार कम होती जा रही है. मुस्लिम औरतें तो इनके यहां नहीं के बराबर हैं. नेतृत्वकर्ती के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं. न पार्टी में और न ही शिक्षार्थी/महिला फेडरेशनों में.
तथाकथित शिक्षित व प्रगतिशील मुसलमान, जो ये समझते हैं कि अछूत की तरह मुस्लिम समाज के साथ व्यवहार बरत के उन्हें जाहिल, परंपरावादी और कटटरपंथी कहकर ग़ैर मुस्लिम लड़कियों, लड़कों से खुद की शादी रचाकर/लिव इन रिलेशनशिप को अपनाकर,(अपनी बहन या भाई के लिए ऐसे रास्ते नहीं निकालते) अपना आखिरी सफर (अंतिम संस्कार) अंगारों (श्मशान घाट) के सुपुर्द करके, मुस्लिम समाज में चेतना, जागरूकता ले आएंगे तो इसे बेवकूफ़़ी ही कहा जा सकता है.
माफ़ी के साथ, बग़ैर किसी संकोच के ये कहना ज़रूरी है कि जनाब, आप या आपकी पैदा की हुई पीढ़ी को मुस्लिम समाज नाकारा समझता है. मरने के बाद खुद को जलवाने की वसीयत मुस्लिम समाज की एक पूरी पीढ़ी को आपसे ही नहीं साम्यवादी, सेक्युलर समझ और विचारधारा से दूर ले जाती है. जो नए समाज निर्माण के रास्ते धुंधले कर देता है.
इससे सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का तो कुछ भला नहीं होता. अलबत्ता शिक्षित और सेक्यूलर समाज बनाने के रास्ते रोकने में बड़े पहाड़ जैसे रोड़े ज़रूर सामने आ जाते हैं. आप जैसों की बेतुकी वसीयतों से ये समाज हर बार सिर्फ आप जैसों से ही नहीं, उन तमाम सेक्यूलर, अमनपसंद, साम्यवादी एक्टीविस्टों से भी किनारा-कशी करता चला जाता है, जो इस मुहिम के झंडा बरदार हैं या सिपाही हैं.
आपके घटिया दर्जे की निजता और झूठा गै़र इंसानी दंभ (गुरूर) समाज परिर्वतन करने वाले पूरे एक्टीविस्ट समाज के प्रति उपेक्षा, नफ़रत और अविश्वसनीयता भर देती है.
पिछले 68 बरसों में चंद ऐसे मुस्लिम लीडरों, नेतृत्वकर्ताओं के नाम क्या कोई बता सकता है, जिन्हें तथाकथित प्रगतिशील, छद्म मुस्लिम नामधारी कम्युनिस्टों ने पैदा किया हो? या उनकी परवरिश का कोई मुस्लिम युवा आज लेफ्ट समझ की बुलंदी पर हो. ज़ाहिर है एक भी नहीं है.